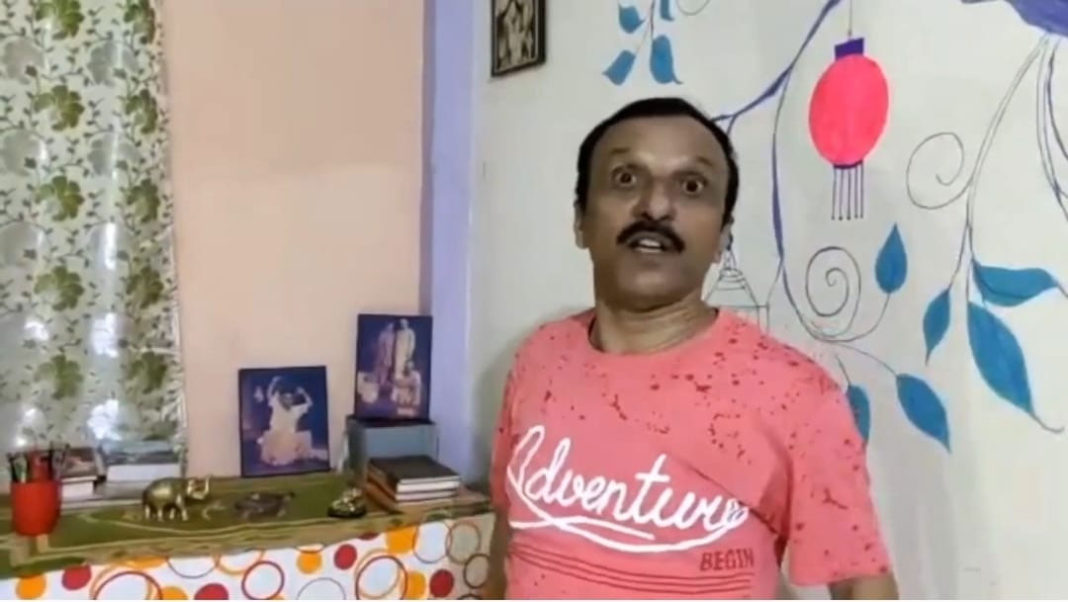सत्यदेव त्रिपाठी ।
सत्यदेव त्रिपाठी ।
सन् 2020 को कोरोना वर्ष’ के नाम से जाना जायेगा। ऐसा बीता है यह साल कि पूरा विश्व इसे एक भयावह दु:स्वप्न की तरह भूल जाना चाहेगा, लेकिन भुला कदापि नहीं पायेगा। इस पूरे साल में जो ‘जीवन चलने का नाम’ था, ‘रुके रहने’ का नाम हो गया।
2020 की ऐतिहासिक देन
वैसे तो सब कुछ में सक्रियता ही जीवन है, लेकिन रंगकर्म को तो सक्रियता के नाम से ही जाना जाता है। रंग यानी नाटक…तो रंग ही कर्म है- रंग है तो कर्म है। और ऐक्टिंग में ऐक्शन (सक्रियता- कर्म) ही तो है। रंगकर्मी सिर्फ़ मंच पर ही रंग-कर्म नहीं करता- प्रदर्शन (शो) हो, न हो- पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) रोज़ शामों या फिर नियत समयों पर पूरे नाट्यसमूह के साथ सामूहिक कर्म के रूप में जारी रहता है। इसके अलावा तो सुबह उठते ही से हर ज़हीन रंगकर्मी तरह-तरह के व्यायाम (एक्सरसाइज़), जिसमें गला व आवाज भी शामिल होती है, के साथ योग-प्राणायाम आदि में सक्रिय रहता है। लेकिन कोरोना से अखिल विश्व में जब सबकुछ ठप हो गया, तो दो-चार दिनों में ही रंगकर्मी का शरीर कसमसाने लगा। शरीर के जोड़ों को तो अकेले में भी सुबह-शाम के निजी व्यायामों से रवां कर भी लेते, लेकिन चूँकि रंगकर्म तन-मन-मस्तिष्क का समुच्चय है, सो दिमांग की नसें तड़कने लगीं, हृत्तत्रियां झनझनाने लगीं। देश के विभिन्न हिस्सों से रोज़ दो-चार फोन आ जाते- कभी मुम्बई-गोवा से, तो कभी जबलपुर-रायगढ़ से, और कभी बनारस-आज़मगढ से- ‘दादा, क्या करें…रहा नहीं जा रहा…बिना कुछ किये जिया जा नहीं रहा! कोरोना काल में रंगकर्मी की यह बेचैनी और तड़प ही डिजिटल थिएटर जैसी नयी प्रवृत्ति की शुरुआत का कारण व कारक बनी। इस अर्थ में कोरोना-काल के इस साल की देन ऐतिहासिक है। लेकिन ध्यान रहे- यह न कोई नया नाट्यरूप (थिएटर फॉर्म) है, न कोई ईजाद (आविष्कार), बल्कि एक चले आते तकनीकी विकास को रवाँ कर देने का वैकल्पिक प्रयास है।
गाँवों में जब खेती हो रही थी, तो नाटक भी होता
इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई नाटक करना चाहे और करने का अवसर न मिले। कुछ नहीं, तो घरू थियेटर (थियेटर इन होम) भी हुए- लोकल गाड़ियों में नाटक हुए… यानी पैसे वाले और अच्छे सभागार में थियेटर करने की समस्या भले होती रही हो, करने की समस्या नहीं होती थी। बनारस में हमारी ही छत पर ‘रंगशीर्ष’ चलता रहा, लेकिन जब पड़ोसी के घर भी जाने के लाले पड़ गये, तो किसी के घर-छत तक भी कैसे पहुँचे कोई? फिर दूरी बनाके रहने की मजबूरी भी… सन् 2020 ऐसा बेहाल लेके आया! उन दिनों मैं गाँव में अटक गया था। गाँवों से थियेटर के उजह जाने का दुख यों तो हमेशा चिंता व ग्लानि का सबब रहा है- ख़ासकर थियेटर से महरूम हो गये गाँवों की जानिब से, लेकिन बच्चों के उक्त फोनों के बीच उस वक़्त रंगकर्मी यानी थियेटर की जानिब से भारतीय रंगकर्म के टोटल शहरी हो जाने का दुख जितना सालता रहा कि ख़ुदा झूठ न बोलवाये, तो इस बात को लेकर उतना दंश पहले कभी न हुआ था। क्योंकि गाँव में रहते हुए देख पा रहा था कि यदि रंगकर्म यानी रंगकर्मी ने एकदम से गाँव न त्यागा होता, तो इस महामारी-काल में भी इतना मजबूर न हुआ होता! और कहना होगा कि सत्ता व व्यवस्था द्वारा गाँवों की अपार वंचनाओं, शहरी व्यामोहों में फँसी सुविधाभोगी शिक्षितों-बुद्धिजीवियों की जमातों के गाँवों से इकतरफा पलायनों तथा पाश्चात्य संस्कृति के दिखावटी जलजलों में लिप्त नयी पीढ़ी की गाँवों के प्रति अफाट हिकारतों से बदहाल होने के बावजूद आज भी भारतीय गाँवों में बहुत कुछ ऐसा बचा है, जो ऐसी किसी भी आफत-विपत में जीवन को बचा सकता है। इसे प्रमाणित किया है- कोरोना-काल में शहरों से हजारों मील पैदल चले आये मजदूरों तथा छोटी-मोटी नौकरियों-धन्धे वालों ने तथा उन्हें अनायास आश्रय देकर स्वयं हमारे गाँवों ने। जब खेती हो रही थी, तो नाटक भी होता- चौपालों-चौराहों पर ही सही। और कोरोना के समय में अपने गाँव के मन्दिर वाले चौराहे पर हमने किया भी ‘हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं ’ का एक शो- जब ‘मंच’ (पटना व मुम्बई) के सरनाम रंगकर्मी एवं सुपरिचित टी.वी.-फिल्म अभिनेता विजयकुमार संयोगन बनारस के शूट से छुट्टी पाकर दो दिनों के लिए मेरे गाँव वाले घर आ गये थे। लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि इतने के बावजूद गाँव की इस नेमत को कोई नहीं समझ पा रहा और ख़ुद थियेटर वालों के न समझने का अफसोस सर्वाधिक होगा।
घर पर ही अकेले के प्रयत्न से एकल नाटक
ऐसे में एक दिन बेहद लगनशील रंगकर्मी प्रियवर नन्द पंत के रू-ब-रू (फेसबुक) पर एक डाक (पोस्ट) मिली, जिसमें ख़बर थी कि तालेबन्दी के खाली समय का सदुपयोग करते हुए वे घर पर ही अकेले के प्रयत्न से एकल नाटक तैयार कर रहे हैं, जिसका प्रदर्शन तालाबन्दी खुलने पर करेंगे। साथ ही अभ्यास करते का वीडियो भी संलग्न था। आज हम ‘अंकीय समय’ (डिजिटल युग) में जी रहे हैं। कहना होगा कि जितना दुखद-चिंताजनक है गाँव से सारे ज्ञान-विज्ञान का पलायन और शिक्षा-संस्कृति का लोप, उतना ही सुखद व सराहनीय है आज का यह डिजिटल विकास, जो कोरोना-काल में जीवन की प्राणवायु बनकर मनुष्य का रहबर बना। इसके बिना पूरे कोरोना-काल के एकदम ठहरे समय में जीवन कैसा होता, अकल्पनीय है। इसी के सहारे सामने आया नन्दजी का वीडियो-प्रयास सबको बहुत अच्छा लगा। उनकी डाक को ढेरों पसन्द (लाइक) मिले। तभी मुझे यह भी विचार आया कि यदि नाट्याभ्यास के वीडियो-चित्र खींचकर भेजे जा सकते हैं, तो नाट्य-प्रस्तुति भी वीडियो पर हो सकती है। मंच पर होते नाटकों का वीडियोकरण तो पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में ही शुरू हो गया था, पर न वह पसन्द किया गया, न चला। इसके रंगमंचीय (थिएट्रिकल) कारण भी हैं, जो प्रसंगत: आगे आयेंगे। इसी पद्धति पर टाटा ने नाटक का चैनल शुरू किया है, पर लोकप्रिय वह भी नहीं हो रहा, जिसके लिए उसका कंजूस विधान भी जिम्मेदार है। लेकिन उस अफाट बन्दी-काल में यह सोचकर बड़ा मज़ा आया कि अपने घर में बैठके कोई नाटक खेलेगा और जीवंत (लाइव) प्रसारण में लोग अपने घरों में बैठे उसे जीवंत (लाइव) देख सकेंगे।
कोई क्यों आयेगा करने और देखने

इस विचार पर मित्रों से फोन-संवाद में चर्चा होने लगी, जो धीरे-धीरे फिर ‘रू-ब-रू’ व ‘हालचाल’ (व्हाट्सप्प) माध्यमों पर फैलने लगी। फिर उस पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं और विमर्श चल पड़े। इसमें पक्के रंगकर्मियों की तरफ से विचार सामने आया कि नाटक जीवंत विधा है- अभिनेता-दर्शक के आमने-सामने करने-देखने की। यही इस विधा की मूल प्रकृति है। फिल्म व दूरदर्शन-शृंखलाओं के समक्ष यह जीवंतता ही रंगकर्म की ताकत है- ख़ासियत है। इसी का तो अलग मज़ा है, आनन्द है, जिसके लिए लोग-बाग घर-बैठे मुफ्त के मनोरंजन को छोड़कर नाटक देखने के लिए दूर-दराज़ तक आते हैं। पैसे खर्चते हैं, समय लगाते हैं। यदि यही नहीं रहा, तो फिर कोई क्यों आयेगा करने और देखने? नाटक में क्या ख़ास रह जायेगा! या क्या रह जायेगा नाटक? यही तो इसकी पहचान है। करने वालों का यही अलग सुख है। इसी कलात्मक तृप्ति व सुखानुभूति के लिए करोड़-पति हो जाने के बाद भी फिल्म-टीवी के कलाकार बरबस मंच पर आते हैं। इसे डिजिटल कर देना तो रंगकर्म का खात्मा होगा, उसकी हत्या होगी। चित्र-माध्यम में उसका विलयन हो जायेगा। फिर तमाम तैयारियों और साधन-सर्ंजामों के साथ काट-छाँट, सम्पादन आदि से बने बहुत बेहतर कोटि के धारावाहिक व फिल्मों के समक्ष इसे कोई क्यों देखेगा? इस तरह यह रंग-कला की आत्महत्या होगी, जिसकी जिम्मेदारी आज के रंग-कर्त्ताओं के सर होगी- उनके नाम नाट्येतिहास में काले अक्षरों से लिखे जायेंगे- आदि-आदि।
कुछ न होने से तो बेहतर है कि कुछ हो
बात सही थी। जायज़ थी। खाँटी थी। सभी प्रभावित हुए। और लगा कि घर पे ‘बैठे ठाले’ की तरह ‘कुछ न करने का कुछ’ के रूप में ही सही, नाटक होने की सम्भावना की भ्रूण-हत्या हो जायेगी.। करने के लिए तैयार युवा उत्सुकों के उत्साह पस्त होने लगे, उमंगों पर पानी फिरने जैसा लगने लगा। कठिन स्थिति थी। लेकिन सबकुछ के बावजूद कुछ था, जो चूक (मिस हो) रहा था। इसीलिए वह चुभ रहा था, कुरेद रहा था। और हारकर ही सही, यह ख़ास मित्रों के बीच आपसी फोन-संवादों में फूटने लगा। रंगकला की सजीवता के नाम पर पूरे थिएटर-संसार की निष्क्रियता का पक्ष प्रमुख बनकर उभरने लगा। इसके लिए कुछ न कुछ करने की बात सर्वोपरि लगने लगी। हारकर ही सही, बुद्धिजीवी वर्ग के तमाम लोगों की धीरे-धीरे इस बात पर सहमति होने या तटस्थ स्वीकृति मिलने लगी कि कुछ न होने से तो बेहतर यही है कि कुछ हो। उधर बनारस के ‘दशरूपक’ एवं उसके सहयोगी नाट्यसमूहों के युवा रंगकर्मी ‘वाराणसी थिएटर’ के मंच से डिजिटल प्रस्तुतियों के लिए बिल्कुल सन्नद्ध… गोया उनके दिये में तेल से भींगी हुई बाती तो थी, बस जरूरत थी एक चिनगारी की।

परिस्थिति के मुताबिक सबकुछ बदलता है
इसी की खोज में आपसी बातचीत से बीच का रास्ता निकाला गया और ‘थिएटर बनाम डिजिटल थिएटर’ पर एक खुली परिचर्चा आयोजित कर दी गयी। कोशिश यह थी कि दोनो पक्षों के मतावलम्बियों का प्रतिनिधित्त्व हो। पहले दिन के प्रास्ताविक या बीज वक्तव्य का दायित्त्व मुझे ही दिया गया, जो मुझे लेना पड़ा। वह एक अद्भुत दिन था। विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए ऑन लाइन भाषण तो काफी दिये थे, पर गाँव में बैठकर मोबाइल से बोलना पहली बार हो रहा था- इस्तक़बाल कोरोना का इस नयी पहल को अंजाम देने के लिए भी! गाँव में नेट सही न था, तो आबादी से सटे खेत में खड़े होकर मैंने उस शाम अपनी बात कही थी। बात का सार उस प्राकृतिक सत्य से बावस्ता था कि परिस्थिति के मुताबिक जीवन-जगत में सबकुछ बदलता है- साहित्य-कला, दर्शन-चिंतन, सोच-विचार, सभ्यता-संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान-तकनीक आदि। जो नहीं बदलेगा ऐसे समय में नष्ट हो जायेगा। त्रिकाल में विश्रुत है कि युद्ध में योद्धा के सामने पीठ दिखाने, सर झुकाने के बदले सर कटा देना ही वीर-धर्म है, लेकिन परिस्थिति को समझते हुए कृष्ण ने पीठ दिखायी- सेना सहित पलायन कर गये और तभी नये राज्य-समाज का निर्माण कर सके- भगवान बने। उस रूप को भी देश के पश्चिमी प्रांतर में ‘रणछोड़ राया’ नाम से पूजा जाता है। और युद्ध के क्षत्रिय-धर्म को निभाने में- किसी भी हाल में उससे नहीं डिगने में ही राजपूतों को षडयंत्रकारी मुग़लों से पराजित होना पड़ा। देश गुलाम हो गया और उसके जलजले अब तक भायनक से बदतर होते जा रहे हैं। भरतमुनि के काल की रंग-परम्पराएं भी समय-प्रवाह में कितनी बदली हैं! आपात्काल में रंगमंच ने खुले विरोध के लिए ‘नुक्कड़ नाटक’ नामक नया नाट्यरूप ईजाद किया, जिसे शास्त्रज्ञ मानें, न मानें, उस वक़्त वह प्रभावी रहा- खुले विरोध का कारग़र साधन बना। समय-समय पर आज भी होता है। एक रंग-विधा के रूप में स्वीकृत है। आज कोरोना की तालेबन्दी में एक विकट परिस्थिति ने फिर चुनौती दी है। महामारी के इस प्रकोप में जब संहिता-अनुमोदित नाट्यकर्म करना जीवन के लिए घातक हो रहा है, तो विकल्प के रूप में पारम्परिक पद्धति से अलग ही सही, नाट्यकर्म में लगाकर ही नाट्यकर्मी को बचाया जा सकता है। तभी नाटक भी बचा रहेगा। यह नया रूप यदि कारगर सिद्ध हुआ, तो इसे समय-समय पर एक नाट्यरूप की तरह जारी भी रखा जा सकेगा, वरना कोरोना जाने के बाद पूर्ववत नाटक होंगे ही आदि-आदि।
डिजिटल माध्यम से नाटक करने का समर्थन
आगे के वक्ताओं में भी अधिकतर ने अपने-अपने ढंग से डिजिटल माध्यम से नाटक करने की बात का समर्थन किया। गौतम चटर्जी ने शास्त्रीय मान्यताओं के तहत नये नाट्यरूप का मार्ग प्रशस्त करने का अनुमोदन किया। संजय उपाध्याय ने कहा कि किसी भी नये प्रयोग की सम्भावना रंगकर्म की मूल प्रकृति में ही निहित है- नाटक करने को ही प्रयोग कहा जाता है। बस, सुरेश शर्मा ने ही प्रकारांतर से रंगमंच के यान्त्रिक माध्यम बन जाने पर नाट्य न रह जाने के खतरों के संकेत दिये। उनका यह कहना ‘राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय’ के कार्यकारी निदेशक की हैसियत का दायित्त्व भी था। बाद की चर्चाओं में यांत्रिकता के तोड़ का भी विचार सामने आया- जब हर प्रदर्शन के बाद उस वीडियो को नष्ट या ज़ब्त कर दिया जायेगा और हर शो के लिए पुन:-पुन: नाटक उसी तरह खेला जायेगा- जैसे नाट्यगृह में खेला जाता है। इस तरह यंत्र से संचालित होकर भी यांत्रिकता (मैकेनिज़्म) से बचा जा सकेगा।

‘डिजिटल थियेटर’ का पहला रंगोत्सव
कुल मिलाकर इस परिचर्चा ने इस विधा की शुरुआत का मार्ग-प्रशस्त कर दिया और बनारस के ‘दशरूपक’ व मुम्बई के ‘9 लिम्ब’ रंगसमूहों की युति में और इनके संचालक क्रमश: सुमित श्रीवास्तव एवं अमन जेटली के नेतृत्व में ‘वाराणसी थिएटर’ के डिजिटल मंच से ‘डिजिटल थियेटर’ का पहला रंगोत्सव सम्पन्न हुआ, जिसमें पाँच नाटक प्रस्तुत हुए- नादिरा ज़हीर बब्बर निर्देशित व सुहाना पटनी अभिनीत ‘जी जैसी आपकी मर्ज़ी’ (एकजुट’, मुम्बई), विभा रानी निर्देशित-अभिनीत ‘आज मैं ऊपर’ (अवितेको, मुम्बई), हरिशंकर परसाई की व्यंग्यकथा पर आधारित एवं मनोहर तेली निर्देशित-अभिनीत ‘आत्मस्तुति परनिन्दा’ (ड्रीमबाज़, जबलपुर), प्रेमचन्द की कहानी ‘बड़े भाई साहब’ की उमेश भाटिया निर्देशित-अभिनीत प्रस्तुति (दशरूपक, वाराणसी) और निर्मल वर्मा की कहानी ‘डेढ़ इंच ऊपर’ की इसी नाम से आलोक चटर्ज़ी द्वारा निर्देशित-अभिनीत नाट्यप्रस्तुति (दोस्त, भोपाल)। इसके साथ ही एक शाम बनारस के ‘रंगूर’ समूह की तरफ से काशी के प्रतिष्ठित नाट्यकर्मी नीलकमल चटर्ज़ी द्वारा हिन्दी-अंग्रेजी एवं बंगला की एक-एक कविताओं का नाट्यमय पाठ भी हुआ। इस तरह डेढ़-दो महीने की कश्मकश से बनता भविष्य-दर्शन साकार हो उठा- गोया ख़्वाबों की तामीर हो। इन प्रदर्शनों से पूरी सम्भावना सामने आयी कि डिजिटल के रूप में एक नये तरह का थिएटर सम्भव है। लेकिन उसे नये रूप में ढालने के लिए बहुत कुछ करना होगा। सबसे पहली बात कि डिज़िटल के मुताबिक नाटक तैयार करने होंगे- लिखने से लेकर मंचित करने की जगह व तदनुरूप नाट्य-विधान रचने तक में। ऐसा इस बार नहीं हो पाया, क्योंकि सारे नाटक पहले से तैयार थे, जिन्हें डिजिटल माध्यम में पेश भर कर दिया गया। सभी नाटकों का एकपात्री होना स्वत: इस बात का परिचायक है कि इस विधा में पात्र कम से कम होने चाहिए। उमेश भाटिया ने दो ही पात्र वाले ‘बड़े भाई साहब’ को भी एक पात्र में साधकर इसका अच्छा उदाहरण पेश किया। वैसे इस बार तो कोरोना के कारण दूरी रखने का दबाव था, वरना पात्र-संख्या सीमित तो होगी, लेकिन एकाधिक हो सकेगी। विभा रानी के नाटक के अलावा सभी में डिजिटल के हिसाब से दृश्यों स्थल व परिवर्तन भी कम से कम रहे। सारी गतियां व फैलाव उस सीमित स्थल व वहाँ लगे कैमरे में समाने जितने होंगे, तो ही यह विधा जमेगी-चलेगी। परिधान आदि के परिवर्तन भी यथासम्भव कम हों… यानी विधान की सीमाएं काफी हैं और उसी में करने की चुनौती है। नाटक की लम्बाई आधे से पौने घण्टे की ही हो, तो उत्तम- जैसे इस बार सभी शोज़ आधे घण्टे के ही रहे, जिसके लिए ‘जी, जैसी आपकी मर्ज़ी’ जैसे पूर्ण नाटक का दो-तिहाई हिस्सा कम करना पड़ा, जिसकी अच्छी सम्भावना उसमें थी।
सारा दारोमदार अभिनय पर
बेशक़, नाटक अभिनेता का ही माध्यम है। परंतु इस विधा का लगभग सारा दारोमदार अभिनय पर होगा- ख़ासकर अभिनेता की आवाज व बोलने के अन्दाज़ पर- इस विधा में इसके लिए ही पूरा आकाश है। और कम से कम गति में अधिकाधिक की प्रस्तुति के गुर को आलोक चटर्ज़ी ने बख़ूबी व एक हद तक मनोहर तेली तथा उमेश ने सिद्ध किया। लेकिन सबसे अहम होगी तेज नेट की सुविधा और सबकुछ को प्रक्षेपित करने वाले मोबाइल की गुणवत्ता, जिसकी कमतरी के चलते यह उत्सव इस बार काफी औसत दर्ज़े का होकर रह गया। ये आवश्यकताएं पूरी हो जायें और निरन्तर करने के अवसर से अभ्यास पाकर ऐसी आदत बन जाये, तो एक स्वतंत्र नाट्य रूप बनकर नाट्य-जग को समृद्ध कर सकेगा।

प्रयोग की सफलता… और बड़ा नाट्योत्सव
और ऐसा हुआ। इस प्रयोग की सफलता से हुलसा हुआ काशी रंगमंच का यह युवा दल एक और बड़ा नाट्योत्सव लेकर आया- लोकनाट्योत्सव, जिसमें देश के नौ प्रतिनिधि रंगसमूहों ने अपने-अपने इलाके के लोकरूप पर बने अपने अग्रणी नाटकों के मंचन किये- उ.प्र. की नौटंकी- अष्टभुजा मिश्र, छतीसगढ़ की पण्डवानी- सीमा घोष, बिहार का बिदेसिया- संजय उपाध्याय, हरियाणवी के डॉ महिपाल पठानिया, महाराष्ट्र का पोवाड़ा- सुधीर यशवंत जाधव, म.प्र. का बुन्देली लोक नाट्य- बालेन्द्र सिंह, राजस्थानी का- मुकेश वर्मा, जम्मू-कश्मीर से मुश्ताक़ कॉक, दिल्ली से भूमिकेश्वर सिंह। नाटक तो ये भी डिजिटल के लिए नहीं बने थे, लेकिन डिजिटल पर सही तकनीक व प्रबंधन के साथ से प्रस्तुत किये जा सके, तो डिजिटल नाट्य-प्रदर्शन की सारी सम्भावनाएं साकार हो उठीं। पहले वाले प्रयोग का यह शीर्ष जैसा आयोजन हुआ। ख़ूब चर्चा हुई- शोहरत का इंतहा नहीं। इसी मुकाम पर देश के बहु मानिन्द रंगकर्मी पद्मश्री से विभूषित श्री बंसी कौलजी भी इन काशी वालों के साथ जुड़ गये। अब ‘दशरूपक’ एवं ‘9 लिम्ब’ के साथ बंसीजी के ‘विदूषक’ की संयुक्ति में ‘कथागायकी’ समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें वसंत निरगुने ने अपने विचार एवं पद्मश्री मालिनी अवस्थी, अंजना पुरी, संजय उपाध्याय, तनरेजा सोढ़ा और वी जयरंजन ने विचार के साथ अपनी गायकी भी प्रस्तुत की।
बड़े-बड़े रंगकर्मियों के फोन आने लगे- हमें बुलाओ, हमें बुलाओ
अब यह आयोजन इतना मशहूर हो गया कि बड़े-बड़े रंगकर्मियों के फोन आने लगे। अपने प्रदर्शन के लिए लोग प्रस्ताव करने लगे। हमें बुलाओ, हमें बुलाओ…, की झड़ी लगने लगी। लेकिन वही- कि अपनी तरफ से करने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरे देखे-लेखे तो किसी दूसरे द्वारा आयोजित कोई नाट्य-प्रदर्शन नहीं हुआ और यह ताज्जुब समझ से परे रहा। सारी सफलता व सराहना के बावजूद इसका आगे न चलना भी बहुत कुछ कहता है!
डिजिटल आयोजनों का रेला
हाँ, काशी की अपनी परिचर्चा और नाट्योत्सव का असर यह जरूर हुआ कि रंगकर्म को लेकर तमाम शहरों में विचार-विमर्श यूँ शुरू हुए कि गोया आयोजनों का ज्वार ही आ गया हो। उपलब्धि यह भी रही कि डिजिटल आयोजन उस रानावि में भी हुए, जो इस पहल को लेकर सबसे अधिक असहमति का केन्द्र रहा। उस मत पर अडिग रहने वाले पुंजप्रकाशजी जैसे ज़हीन व प्रतिबद्ध रंग कलाकारों ने भी युवा रंगकर्मियों के कामों-सोचों को उन्हीं की ज़ुबानी सामने लाने के डिजिटल आयोजन की लम्बी शृंखला चलायी, जिसे अच्छा प्रतिसाद भी मिला। कुछ वरिष्ठ व सरनाम रंगकर्मियों ने निजी स्तर पर अपनी रंग-यात्राओं पर वीडियो तैयार करके मुहय्या कराये, जो काफी मक़बूल भी हुए। तमाम रंगसमूहों द्वारा थिएटर के विविध पक्षों व मुद्दों को लेकर लम्बी-लम्बी व्याख्यान-मालाएं आयोजित हुईं और उनमें देश के शीर्ष विद्वानों ने शिरकतें कीं। जीवंत सवाल-जवाब हुए। विद्वानों में विशेषज्ञ कलाकार भी रहे, जो बात करते-करते प्रदर्शन करके दिखाते भी थे, अपने सहायक कलाकरों के साथ दृश्य भी करते-कराते रहे। इस तरह उन्हें लोगों के सामने जीवंत करने का भी आनन्द मिला और सामने वालों को सुनने-देखने-समझने का भी। फिर इसमें नाट्य-संगीत के आयोजन भी हुए, जिनमें गा-गाके और गाते हुए कर-करके दर्शन-प्रदर्शन की युति साकार हुई- डिजिटल आयोजनों का रेला-सा आ गया।
कहना होगा कि इन आयोजनों में भी बंसी कौल की युति के साथ काशी का यही मंच अग्रणी रहा। सबने मिलकर ऐसे यादगार आयोजन किये, जिन्हें कार्यक्रमों का क्लासिक कहा जा सकता है। इसमें ‘कलाओं में लोकतत्त्व’ की 21 व्याख्यानों की शृंखला अपनी ज्ञान-गरिमा और कलात्मकता की दृष्टि से बेजोड़ रही। इसमें नाट्य के अलावा साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला एवं सिनेमा कला आदि पर भी प्रदर्शनपरक विमर्श हुए। रंगालोचन पर छह दिनों का आयोजन हुआ, जिसमें मौजूदा समय के छह प्रतिनिधि रंग-आलोचकों ने शिरकत की। जाहिर हुआ कि समूचा रंगालोचन खानापूर्त्ति भर ही है। न कोई आलोचनात्मक पहचान है, न कलात्मक इयत्ता। अधिकांश आलोचक अपने विषय पर कुछ ठोस बोल न पाये और कुछेक तो बोल ही नहीं पाये- एक घण्टे के लिए आये और 20 मिनट आँव-बाँव करते-करते ढेर हो गये। इस दृष्टि से यह आयोजन सबसे महत्त्वपूर्ण रहा कि कलई खुल गयी।
चुनौतियों को स्वीकारने वाली जिन्दगी व कला की पहचान
और अंत में बता दें कि जिस पंतजी के काम ने इस सबकुछ का प्राथमिक विचार दिया, उनका वह नाटक ‘सुदामा के चावल’ भी तैयार होकर आज तक प्रदर्शन की राह देख रहा है। अभी तक डिजिटल माध्यम पर नाटक तैयार किये जाने की कोई ख़बर नहीं है। ऐसे में जिस तरह इस पहल का सूत्रधार बना काशी, तो वहीं से ऐसी पहल की भी उम्मीद की जानी चाहिए कि डिजिटल माध्यम के दो-एक नाटक तैयार करके उनका प्रदर्शन कराये। लेकिन अब तो कोरोना के बावजूद बहुत कुछ खुल गया है। अब छिट-फुट नाट्योत्सव होने की ख़बरें आ रही हैं। ऐसे में नाटक न कर पाने की वह त्रासदी शायद खत्म हो, तो यह नयी विधा पुन: अनंत काल तक के लिए टल सकती है। उधर डॉक्टरों, मेडिकल शोधकर्त्ताओं-विशेषज्ञों की तरफ से कोरोना के दूसरे दौर के ज्यादा घातक होने के विचार आ रहे हैं और इधर जीवन की तमाम गतिविधियां कमोबेस चलने लगी हैं। तो नाट्य-संसार में भी गतिविधियां शुरू हो रही हैं। यह भी रोचक है और प्रकृति व काल की चुनौतियों को स्वीकारने वाली जिन्दगी व कला की तो पहचान ही यही है कि ‘बाढ़ की सम्भावनाएं सामने हैं, और नदियों के किनारे घर बने हैं’!