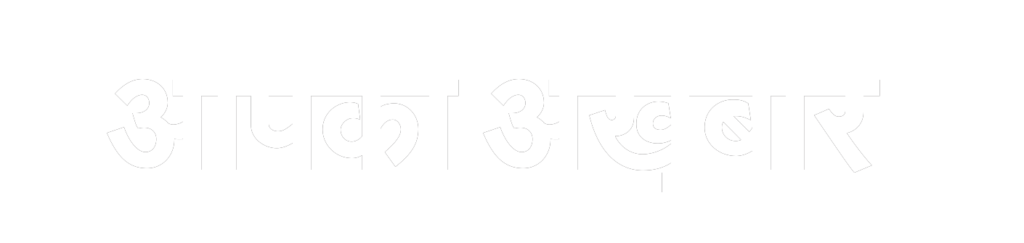सत्यदेव त्रिपाठी ।
सत्यदेव त्रिपाठी ।
आज 15-16 साल के बच्चे ‘पंगति’ शब्द जानते भी न होंगे, जबकि इसके पहले यह शब्द सबकी ज़ुबान पर होता था- बल्कि कहें कि कभी यही ‘पंगति’ या ‘पंगत’ हमारी संस्कृति का बीज शब्द हुआ करता था।
‘तेरहवीं की पंगति खाने’ का मुहावरा हास्य भी था, और झगड़े में ताना भी। आज बोला ही नहीं जाता, वरना समझा जा सकता है आज भी। लेकिन जो शब्द आज बच्चे से बूढ़े तक सभी जानते हैं, वह है- ‘बफर सिस्टम’ (‘व्यवस्था’ नहीं)। जबकि 15-20 सालों पहले भारतीय जीवन में ‘बफर’ शब्द का अता-पता भी न था। दोनो का मतलब है– विवाह-मरण… आदि सामाजिक समारोहों में सामूहिक खान-पान की पद्धति।
‘बूफे’ गाँवों में ‘बफर’ हो गया
अंग्रेजी का शब्द ‘बूफे’ हमारे पूर्वी उत्तर भारत के गाँवों में आकर ‘बफर’ हो गया है और विनोद में ‘बफैलो डिनर’ भी। ‘बूफे’ से ‘बफर’ कैसे बना, को बताना तो इस शब्द की ध्वनि-परिवर्तन-प्रक्रिया का द्रविड-प्राणायाम हो जायेगा; लेकिन पंगति का मतलब सीधा है- ‘पंक्ति’। संस्कृत शब्द ‘काक’ का जैसे बोलचाल में ‘काग’ और फिर ‘कागा’ हो जाता है, वैसे ही ‘पंक्ति’ के बीच का आधा क भी पूरा ग होकर पंगति बन गया है, जिसे बोलना कागा की तरह ही आसान हो जाता है। इसे भाषा-विज्ञान में ‘मुख-सुख’ कहते हैं। सामूहिक आयोजनों में सभी के एक पंक्ति में साथ बैठकर खाने की यह ‘पंगति-प्रथा’ ऐसी भारतीय पद्धति थी, जो ‘सत्यनारायण ब्रत-कथा’ की भाँति पूरे देश में प्रचलित थी – चाहे भले रहन-सहन, खाने-पहनने व भाषा आदि की ढेरों भिन्नताएं मौजूद हों।

पंक्तियों के कई दायरे हुआ करते थे। सबसे बड़ा व मशहूर दायरा जाति की पंक्ति का होता था। इसी से बना बहु प्रचलित शब्द ‘जाति-पाँति’ (जाति की पंक्ति) आज भी एकदम मरा नहीं है। आस-पास के चारों तरफ 5-6 किमी. की सीमा में बसे दसों गाँवों में सजातीय लोगों की पंगति हुआ करती थी। वहाँ तक रातों को खाने जाया जाता था। ऐसी पंगतों में मेरा बचपन शरीक रहा है। हम सब एक दूसरे के पूरे परिवारों को प्राय: नाम सहित जानते थे। दूसरी बड़ी पंगति होती थी – गाँव की। गाँव में किसी के घर आयोजन हो, पूरा गाँव खाता था। इन पंगतों में खाना प्रतिष्ठा का मानक हुआ करता था। जब महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, समाज-सुधारक कर्वे साहब ने घर से निकाल दी गयी चार विधवाओं को पढ़ाना शुरू किया, तो बिरादरी की पंगति से बाहर कर दिये गये थे। लेकिन गाँव की पंगति में रहने के लिए सविनय आग्रह किया था। यह खान-पान ही नहीं, एक सहकारिता सम्बन्ध भी हुआ करता था। गाँव की पंक्ति-शुद्धता पर ही परिवार की इज्जत मुनहसर होती थी। और इस प्रतिष्ठा का दर्ज़ा यह कि इसी डर से लोग शराब पीने, जाति से बाहर शादी करने… आदि कई उस समय के लिए घोर निषिद्ध समाज-विरोधी कार्य नहीं करते थे। फिर भी यदि किसी से समाज के बनाये ऐसे नियमों का उल्लंघन हो जाता, तो उसे पंक्ति से बाहर कर दिया जाना ही सबसे बड़ा दण्ड होता, जिसे कोई बर्दाश्त न कर पाता– ऐसी थी सामाजिकता। ‘पंक्ति-बाहर’ का सीधा मतलब होता ‘जाति-बाहर’। लेकिन इस दण्ड के लिए रूढ़ शब्द है ‘बिरादरी बाहर’। आम बातचीत में यही चलता है। इसी नाम से राजेन्द्र यादव की एक कहानी है। बिरादरी-बाहर होने वाले की अरदास (अनुनय) पर पूरी जाति की पंचायत बैठती थी। उससे ‘डाँड़ (दण्ड) देकर पुन: पंक्ति में लेने का विधान था। दण्ड में कोई सामूहिक उपयोग की वस्तु ली जाती थी – गाँव भर के बैठने लायक बिछौना या भोजन पकाने का बड़ा हंडा…आदि। ‘पंगति’ शब्द तो खान-पान से आगे बढ़कर जाति या एक समुदाय का भी बोध कराता, लेकिन सिर्फ़ खान-पान के लिए बोलचाल का चलता शब्द ‘भात-भोज’ ज्यादा प्रचलित रहा है।
बफर में सब कुछ पैसे का खेल
तब शादी-वादी में सबसे पहले यही देखा जाता था कि वह परिवार जाति व गाँव की पंगति में है या नहीं – पंक्ति-शुद्ध है या नहीं। प्रसंगानुसार इसमें निहित एक संकीर्णता का उल्लेख भी कर दूँ… पवित्रता के नाम पर ब्राह्मणों में इस पंक्ति-शुद्धता का सबसे छोटा दायरा एक ख़ास कुल तक सिमट गया। इसमें गाँव क्या, उसी जाति के अन्य कुल-परिवार का व्यक्ति भी उनकी पंक्ति में नहीं आ सकता। इस शुद्धता के कथित रूप से सर्वोच्च, पर वस्तुत: सबसे निकृष्ट उदाहरण आज भी मौजूद हैं- कहीं ‘पंक्ति-पावन’, तो कहीं सारस्वत आदि नाम-रूपों में। वस्तुत: कुल-श्रेष्ठता की स्पर्धा में चलती चूहा-दौड़ का यह सबसे विगर्हणीय रूप है।
लंच-डिनर पार्टियां जब चल रही हों, तो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं – ‘बूफे इज़ ऑन’, वैसे ही हम कहते थे – ‘पंगति बैठी है’। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि पंगति में खाया जाता है बैठकर। जबकि बफर (बूफे) में खड़े-खड़े खाना तो उजागर ही है, जो वहाँ की भयंकर ठण्डी और उसके लिए कोट-पैण्ट के पहनावे के हिसाब से उपयुक्त भी है। लेकिन मई-जून की तेज गर्मी में होने वाली अधिकांश शादियों में हमारे यहाँ ऐसा होना भोंड़ी नकल के सिवा क्या हो सकता है?
आज के बफर में सब कुछ पैसे का खेल है। बनाने-खिलाने वाले हलवाई (कैटरर) को ठीका दे दिया जाता है। आदमियों की संख्या के मुताबिक वह सामान लिख देता है, जिसे बाज़ार में बनिए को दे आते हैं। वह सब कुछ बाँध के घर पहुँचा देता है। फिर आयोजन के दिन सुबह हलवाई की टीम आके बनाने में जुट जाती है और शाम को खाने के समय 7-8 मेजों पर शफ़्फ़ाक़ कपड़े बिछाकर उसी पर सारे भोज्य पदार्थ रख दिये जाते हैं। एक तरफ खाने के लिए प्लास्टिक के प्लेट-चमच और दूसरी तरफ पीने का पानी व हाथ धोने की व्यवस्था। लोग आते रहेंगे, प्लेट लेके खाते रहेंगे, हलवाई के लोग सामान भरते रहेंगे… और सब सम्पन्न। लेकिन पंगति-प्रथा सिर्फ़ आके खाने तक सीमित न थी। उसमें गाँव के सारे स्त्री-पुरुष समान भाव से शरीक होते थे। बनाने से लेकर खाने-खिलाने तक सब कुछ सब लोग मिल-जुल कर करते थे। पूरे गाँव के अपने निजी काम उस दिन बन्द होते थे। सुबह से ही लोग उस आयोजन वाले घर के काम में लग जाते थे। हमेशा करते-करते सबको पता होता कि किसे क्या करने अच्छा आता है। उसी के अनुसार सभी अपने-अपने काम में जुट जाते।
कुछ लोग जमीन खोदके, फिर ईंटे जोड़ के चूल्हें बना रहे हैं; कुछ लकड़ियां ला रहे हैं- चीर रहे हैं। कुछ कड़ाही-हण्डे ला रहे– साफ कर रहे हैं। औरतें घर में आँटा-चावल-दाल-भाजी आदि सारे सामान व बर्तन आदि निकाल रही हैं। बुज़ुर्ग लोग बैठ के सबको काम सहेज रहे हैं। कुछ लोग आँटा गूँथ रहे हैं, कुछ चावल-दाल धो रहे हैं, कुछ भाजी काट रहे हैं। फिर औरतें रोटी-पूड़ी बेल रही हैं। कोई कड़ाही के खौलते घी में पूड़ियां डाल रहा, कोई छान रहा है। उधर रोटियां सेंकी जा रही है। अलग-अलग चूल्हों पर भात-दाल-भाजियां बन रही हैं। खीर-हलवे पक रहे हैं। तैयार भोजन घर में रखने के लिए औरतें कपड़े बिछा रही हैं, तो युवा लोग बड़े-बड़े बर्तनों में भरे भोजन टेका के वहाँ रख रहे हैं। गरज़ ये कि आयोजन भले एक घर का होता, लेकिन उस प्रयोजन से जुड़ जाता पूरा गाँव।
‘पंगति बैठी है’
लंच-डिनर पार्टियां जब चल रही हों, तो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं – ‘बूफे इज़ ऑन’, वैसे ही हम कहते थे – ‘पंगति बैठी है’। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि पंगति में खाया जाता है बैठकर। जबकि बफर (बूफे) में खड़े-खड़े खाना तो उजागर ही है, जो वहाँ की भयंकर ठण्डी और उसके लिए कोट-पैण्ट के पहनावे के हिसाब से उपयुक्त भी है। लेकिन मई-जून की तेज गर्मी में होने वाली अधिकांश शादियों में हमारे यहाँ ऐसा होना भोंड़ी नकल के सिवा क्या हो सकता है? फिर खड़े-खड़े व बात करते हुए चलते-फिरते खाने के मुकाबले बैठ के आराम से खाने की सहूलियत और उसका स्वास्थ्यप्रद होना तो कहने की बात नहीं। शायद इसीलिए यहाँ चलते-चलते खाना वर्जित था– ‘खादन्न गच्छामि’। लेकिन बूफे में तो प्राय: लोग चल-चल कर एक दूसरे के पास आ-जाकर खड़े-चलते, बात करते हुए खाते हैं। फिर जब मोड़कर बिछाये गये टाट या बिछावनों पर पाल्थी मारके इत्मीनान से पंक्ति में बैठा जाता, तो एक-एक खाद्य-पदार्थ लेकर लोग आते और बैठे अभ्यागतों के पत्तलों (पत्तों की बनी प्लेटों) पे रखते। इसे ‘परसना’ (सर्व करना) कहते। और ऐसा करते हुए परसने वाले का खाने वाले के सामने अपने आप ही झुक जाने में आमंत्रित के समक्ष विनम्रता की और भोज्य सामग्री लिए हुए लगातार पंगति में घूम-घूम कर इसरार कर-करके खिलाने में ‘अतिथि-सत्कार’ की भारतीय संस्कृति चरितार्थ होती। लेकिन अब तो बफर में परसने का रवाज नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इसने सबको अकेला और स्वच्छन्द कर दिया है। हाल यह है कि गाँवों में ‘बफर’ के ढक्कन खुले नहीं कि हाथों में प्लास्टिक के प्लेट लिये खाने वालों का गड्डलिका प्रवाह उमड़ पड़ता है। ‘कितनी जल्दी खाये और भागे’, की होड़ मच जाती है। उस धकापेल में बड़े-छोटे का कोई लिहाज नहीं। खाना ले पाये, तो बैठने की कुर्सी न मिली। शहरों में यह सब काफी व्यवस्थित है। लेकिन वहाँ क़तार लगती है, जिसमें प्लेट लिये खड़े होने पर शुरू-शुरू में मुझे कटोरा हाथ में लिये भिखारी की याद हो आती!

पंगति में तो परसने वालों के अलावा बड़े-बुज़ुर्ग़ भी टहलते हुए किसके पत्तल में क्या घट रहा है, का बराबर ख्याल रखते। उनकी नज़र इस बात पे भी रहती कि गाँव से लेकर बाहर तक के आमंत्रितों में, कोई बच्चा भी छूटने न पाये – बिना खाये न रह जाये। धुर बचपन में मुझे सोते से जगाके खिलाये जाने की अपनी याद है। आज ‘बफर’ का हाल यह है कि कौन क्या खा रहा है, की क्या कहें, अपनी पोती की शादी में मैंने ही नहीं खाया और किसी को पता न चला! आयोजक को नहीं पता कि किसने खाया, किसने नहीं; और न इसकी किसी को पड़ी है। यह निरपेक्षता या बेग़ानापन बफर व्यवस्था की मूल संकल्पना में निहित है। बंगला कथाकार शंकर द्वारा विदेश-भ्रमण पर लिखित सरनाम पुस्तक ‘ए पार बांगला, ओ पार बांगला’ में मैंने पढ़ा कि पाश्चात्य देशों में घर आये मेहमान को भी पानी के लिए नहीं पूछते। पूछने से उसका अपमान माना जाता है। उसे पीना है, तो जाकर फ्रिज से लेकर स्वयं पी लेगा। इतना स्वतंत्र व वैयक्तिक समाज है वह। जबकि हमारे यहाँ पूछ के, बल्कि आग्रह करके खिलाने-पिलाने की समृद्ध संस्कृति रही है। आज भी है, लेकिन अब इसी नकल में नष्ट होती जा रही है।
पंगति-प्रथा में परिष्कार
पंगति की सबसे उल्लेखनीय सामाजिकता इस विशेषता में थी कि पूरी पाँति सबके खा चुकने का इंतज़ार करती और फिर सब साथ उठते। तब तक उधर दर्जन भर बच्चे पानी का जग लिये हाथ धुलाने को तैयार रहते। सब लोग एक दूसरे को पहले हाथ धोने का मौका देते। लेकिन बफर की गँवईं धक्काधुक्की या शहर की भिक्षुकी क़तार में यदि जैसे-तैसे आप खा भी चुके, तो शामियाने के दूसरे सिरे पर रखे पानी के पास पहुँच के जिस गिलास की तरफ हाथ बढ़ाने चलते हैं, सहसा उसे कोई और हाथ उचक लेता है। और आप इस बफर ‘तहज़ीब के पेशेनज़र’ उसे नज़रअंदाज़ करने पर बाध्य होते हैं।
बूफे आने के पहले पंगति-प्रथा में एक परिष्कार हुआ था। टाट या बिछावन बिछाके पलत्थी मार (पाँव मोड़कर और एक पर एक रख) कर बैठ के खाने के बदले कुर्सी-मेज का चलन चला था, जिसमें परसने-खिलाने की शेष सारी प्रथाएं वैसी ही होतीं। महाराष्ट्र में भी कुर्सी-मेज वाली परिष्कृत पंगति में खाने के अवसर मिले। वहाँ तो मुख्य आयोजक सपत्नी (व सपरिवार भी) हर खाने वाले के सामने से हाथ जोड़े गुज़रता और ‘सावकाश जेंवाँ’ (आराम से खाइये) कहते हुए आतिथेय (होस्ट) का धर्म निभाता। यह पद्धति भी उतनी ही सामाजिक थी, सिर्फ़ मेज-कुर्सी भाड़े पर आती, जिसके लिए नक़द पैसा देना होता। वरना पंगति-प्रथा पूर्णत: आपसी सहयोग-सहकार पर निर्भर होती। घी-मसाला ही खरीदना होता– बाकी सब घर-गाँव से ही जुट जाता।
पंगतों की सर्वाधिक मज़ेदार रवायत इस बात में निहित होती कि परसने और खाने वाले सभी एक दूसरे से इतने घुले-मिले होते कि सब सबकी रुचियों-आदतों को भी जानते। जैसे हमें इतना ही नहीं पता होता कि पूड़ी हो, तो पारस भइया भात नहीं खायेंगे और पूड़ियां भी 50 से कम नहीं खायेंगे, बल्कि यह भी पता होता कि यदि पहली बार में दस-पाँच पूड़ी ही रख दिया, तो मारे गुस्से के खाना छोड़कर चले जायेंगे। इसलिए उनके पत्तल पर 25-30 पूड़ी इकट्ठे रखना है। फिर इसके आगे का खेल यह कि उनका कोई हमजोली हुआ, तो चिढ़ाने के लिए ही पाँच पूड़ी रख देता। फिर गुस्साए पारस भइया को मनाते और उन्हें मनाये जाने के सौ उपायों का भी सबको पता होता। इसी तरह खाते हुए पल्टू भैया से पूछ दें– ‘और क्या दूँ’?, तो बस लेने के देने। इसलिए जब तक वे आपको देख के पत्तल के आगे हाथ करके रोक न दें, तब तक बिना पूछे परसते रहिए। ऐसी किसी ख़ासियत से नितांत दूर बफर में सब लोग बस खाने की फर्ज़-अदाई करके चलते बनते हैं। फर्क़ यह भी है कि तब पूड़ियां गिन-गिन के खिलाने का आनंद था, अब नज़र इस पर रहती है कि खाना (डिशेज़) कितने तरह का बना है, जिसमें कार्यरत होती है हैसियत की स्पर्धा, ईर्ष्या, जो बफर की ही नहीं, इस युग की प्रवृत्ति है।
जरा देर से गये, तो…
और आप बफर में जरा देर से गये, तो शामियाने (टेण्ट कहते हैं आजकल) वाला अपनी समस्त ऊब व उतावली के साथ डेरे-डम्बर उतारते दिखता है। बिजली-उत्पादक (जनरेटर) अपने खत्म होते तेल के साथ अंतिम साँसें ले रहा होता है। यह सब देखकर आप बिना खाये चले आने जैसा महसूसते हुए भी उपरफट्टू मज़बूर की तरह खा भी लेते हैं। और ऐसी बातों का बफर में कोई मतलब ही नहीं है। उधर पंगति का अन्तिम सोपान सबसे यादगार होता, जब सबके खा चुकने के बाद सबसे अंत में परसने और अन्य प्रबन्ध करने वाले तथा आयोजक के घर के सबलोग एक दूसरे को सहेज कर साथ खाने बैठते। उस वक़्त कोई खाना खत्म हो चुका होता, तो कुछ ज्यादा बचा होता। खत्म हो रहे मिष्ठान्न आदि किसी अच्छे खाने को कोई बच्चा बड़ी चालाकी से बचा या छिपा के रखे होता… और सब कुछ को मिल-बाँट के सधाया जाता। लेकिन खाने से ज्यादा मज़ा आता पूरे भोज के दौरान हुई बातों की चर्चा व समीक्षा में– सोचकर आज भी तबियत लरज जाती है। उन दिनों सेमिनारों के बाद भी चाय पीते हुए ऐसी ही चर्चाएँ होतीं, जो आज की भगदड़ में बिल्कुल गायब हैं। उन चर्चाओं में कुछ भूल-गलतियों को अगले आयोजन में सुधारने और अच्छाइयों को आगे बढ़ाने के तमाम मंसूबे बँधते… और अगले भोज के अरमानों के सपने लेकर हम सोने जाते और नींद में परसने-खाने के सपने देखते।
कुल मिलाकर यह पंगति-प्रथा भोज के बहाने एक समूची समरस संस्कृति होती, जिसमें तमाम फौरी भेद-भावों को भुलाकर आपसी सौहार्द्र का भाव बनता। उसमें व्यक्ति-स्वातंत्र्य का एक हद तक हनन तो था, लेकिन उन मर्यादाओं में बँधकर सामाजिक नैतिकताएं काफी दृढ़ हो जातीं और तमाम आपसी कलहें और भ्रष्टताएं दब जातीं। इधर बफर का मामला ही एकदम कामपटाऊ हो गया है- ‘काम पटा, छुट्टी मिली’ की राहत और भव्यता के दिखावे के सिवा कुछ रह नहीं गया है। बफर की इस प्रथा में हमारी सामाजिकता ही नहीं, अनौपचारिकता के नाम पर आज की मनुष्यता ही बदल गयी है। लेकिन तब पंगति के बाद हमारा आपसी अपनत्त्व बढ़ गया होता, ममत्त्व कुछ गहरा गया होता। उसमें होती चुहलों के मंसायन से एक नयी ताज़ग़ी का अहसास दिलाते हुए आती सुबह हमें कुछ ज्यादा सामाजिक हो जाने का बोध कराती और पूरा गाँव कुछ अधिक मानवीय नज़र आने लगता। पंगति का सहभोज सचमुच का प्रीतिभोज होता!
ये भी पढ़ें
डीह बाबा का जाना संस्कृति के एक युग का अवसान