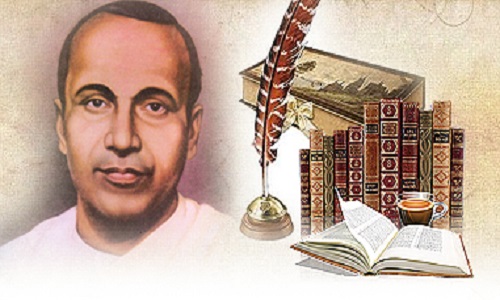सत्यदेव त्रिपाठी
सत्यदेव त्रिपाठी
बीसवीं शताब्दी के हिंदी के सबसे बड़े लेखक जयशंकर प्रसाद (30 जनवरी, 1890- 14 जनवरी, 1937) के निधन के 84 साल बाद रज़ा फाउंडेशन की मदद से लेखक-आलोचक सत्यदेव त्रिपाठी ने उनके विषय में प्रकाशित सूचनाओं, शोध और उनकी कृतियों में बिखरे सूत्रों के आधार पर प्रसाद की जीवनी -‘अवसाद का आनंद’- लिखने का उद्यम किया है जो अब पूर्णता की ओर है। प्रस्तुत हैं इसके एक अध्याय ‘उसकी स्मृति पाथेय बनी’ के सम्पादित अंश।
उद्दाम प्रेम है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन भारतीय समाज में विवाह के अलावा किसी प्रेयसी का होना अच्छा तो आज भी नहीं माना जाता, तब तो बहुत बुरा माना जाता था। बड़ी बेइज्जती का सबब होता था- प्रसादजी जैसे सम्भ्रांत समाज में तो और भी ज्यादा। अत: तब उदार व उदात्तवादियों ने किसी निजी पीड़ा को ख़ारिज़ करते हुए बड़ा सटीक व सरल तर्क दिया है कि ‘आँसू’ के सृजन के वक्त कवि के निजी जीवन में कोई दुख न था। कमलाजी से हुई तीसरी शादी के बाद अंतिम रूप से जीवन में व्यवस्थित होकर कवि प्रसन्न थे।
तो इन प्रमाणों से तर्क यह दिया गया कि इस परम सुख के बीच ग्लानि-पीड़ा-तड़प आदि, जो उस कालावधि में कवि के जीवन में थे ही नहीं, रचना में कैसे आ सकते हैं! यानी यह सब उनके निजी जीवन से बावस्ता नहीं, आम जीवन की अभिव्यक्ति है. वह पीड़ा सबकी है। इसका निष्कर्ष यूँ कि ‘आँसू’ की पीड़ा ‘ग़मे जानां’ से नहीं, ‘गमे दौरां’ से उपजी है. कवि के निजी जीवन से उसका कोई वास्ता नहीं, वह तो रचना की पीड़ा है- रचना मात्र है।
लेकिन यह तर्क व व्याख्या सृजन के ककहरे (क ख ग) से भी अनभिज्ञ सिद्ध होती है या उसे नज़रन्दाज़ करके लिखी गयी है। दूर न जाकर ‘आँसू’ के उक्तोद्धृत उसी मशहूर छंद –
‘जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति-सी छायी.दुर्दिन में आँसू बनकर वह आज बरसने आयी’
पर ही ध्यान दे दिया जाता, जो कृति में प्रवेश करने के पूर्व लिखा मिल भी जाता है, तो ऐसा तर्क त्रिकाल में न दिया जाता… अभी तो ऐसा भी लग रहा है कि इस छंद को प्रमुखता से कृति के पहले लिखने में कदाचित् कवि की मंशा भी रही हो, कि इसे फौरी सन्दर्भों से न जोड़ा जाये। फिर ‘आँसू’ में आकर तो ये पंक्तियां बहव: उदाहरणीय बन गयी हैं, प्राय: उद्धृत होती भी हैं; लेकिन इसमें न भी होता यह छंद, तो भी सृजन-प्रक्रिया का यह विश्रुत सच है कि साहित्य कोई रिपोर्ट नहीं, जो आज की घटना को कल अख़बार में दर्ज़ कर दे। अस्तु, यह कदापि जरूरी नहीं कि उसी वक्त जीया जाता जीवन ही रचना में आता है। घनीभूत पीड़ा कभी की भी हो सकती है, जिसका सिद्ध सन्धान या जिसे सिद्ध करता सन्धान ही यहाँ अभिप्रेत है कि कवि के जीवन में आख़िर वह थी कौन, जो स्मृति बनकर और स्मृतियों में अनगिन रूप धर-धर कर आती-जाती रही और पाठक के मन में भी आती रहती है।

लेकिन उसके पहले गमे दौरां का एक और ख़ास सन्दर्भ, जो प्रत्यक्ष भी है और अपनी कलात्मकता में रोचक भी। जीवन-सन्दर्भों के सिलसिले में क्रान्तिकारी प्रदर्शनकारियों की घटना पीछे विवेचित है, जिसमें सत्ता-विरोधी नारे वाले गीत गाते हुए पर्चे बाँटते बच्चों को पुलिस पीटे जा रही थी, पर बच्चे चिल्ला-चिला कर गीत गाये जा रहे थे, दो दिन ऐसा होने का जिक्र मिलता है और दोनों दिन इस दृश्य पर प्रसादजी की आँखों से आँसू बह निकले थे। सारे दृश्य के प्रत्यक्ष-द्रष्टा दुर्गादत्त त्रिपाठी अगले दिन प्रसादजी से मिले, तो उन्हें कुछ लिखते पाया। सुनने की इच्छा जतायी, तो प्रसादजी ने उन बच्चों के जुनून व जीवट की कुछ बातें कीं और वही क्रांति-व्यंग्य गीत गुनगुनाया भी। इसके कुछ ही दिनों बाद प्रसादजी ने त्रिपाठी-दम्पति को पहली बार ‘आँसू’ के शुरुआती तीन छंद गाके सुनाये थे। त्रिपाठीजी को लगा कि पता नहीं सर्वोत्तम पंक्तियां देने के निखार-सुधार के अधीन ‘आँसू’ की पहली चार पंक्तियां ही कितने संस्कारों के बाद अवतरित हुई होंगी! (वांग्मय -116)
लेकिन तीनो छंद सुनके सहसा उन्हें वह क्रांति-गीत याद आ गया- वही छंद, वही धुन– त्रिपाठीजी निश्चय पूर्वक कुछ कह सकने की हालत में नहीं कि ‘आँसू’ का पहला छंद पहले लिखा गया था या पहले उस लड़के के मुंह से वह गीत सुना गया था’, लेकिन यह संकेत बिल्कुल साफ है कि ये आँसू किसी ‘इसकी-उसकी’ स्मृति के नहीं, राष्ट्रीय चेतना के आँसू’ हैं– इसका बेहद रचनात्मक प्रमाण यह भी कि लिखने-पढ़ने-गाने, सबमें दोनो प्राय: समान हैं- एक-एक चरण (अर्धविरामों में बँधे) बारी-बारी से साथ गाके देखें-
‘अंगरेजी रंगरेजवन के, दल-बादल आयल बाटैं, रँगने को धरा रुधिर से, बदरा गदरायल बाटैं’।
इस करुणा कलित हृदय में, अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में, वेदना असीम गरजती।
तीनों छंद सुनकर श्रीमती कुसुम दुर्गादत्त त्रिपाठी ने अपने बाला-सुलभ स्वभाव से कविता की पृष्ठभूमि पूछ ली। और प्रसादजी ने अपने चिर गोपन अन्दाज़ में कहा- ‘ऊपर वाला जाने’!
पूरे विवरण का लक्ष्यार्थ, बल्कि वाच्यार्थ यह कि ‘आँसू’ का उद्भव ही इतनी ज़हीन राष्ट्रीय चेतना से हुआ है कि वह निजी जीवन के प्रेम-बिरह की कविता नहीं हो सकती। अत: इन सबसे कहीं अधिक यह सामाजिक जीवन की कविता है। और इस बात को दुर्गादत्त जी दूसरी तरह कहते हैं और कहीं ज्यादा शिद्दत से कहते हैं-
‘ऐसी स्थिति में केवल कल्पना क्या काम दे सकती है। वास्तव में बाबू साहब अपने रूप पर आप ही इतने मुग्ध थे कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कभी किसी रूपवती से आसक्ति और उसके वियोग से कभी कोई पीड़ा हो सकती थी या नहीं। बाह्य आसक्ति उनके काव्य की विषय-वस्तु बन भी सकती थी या नहीं, इसमें सन्देह है। वे अत्यंत पवित्र व आत्मस्थ विचारों के स्वामी थे। दासता तो वे कदाचित् अपने प्राणों की भी स्वीकार नहीं कर सकते थे’ (वाङमय-120) ।
इस कथन में रूपवती से आसक्ति न होने की बात निरी भावुकता या प्रसादजी के व्यक्तित्व के प्रति प्रगाढ़ अनुरक्ति (ऑब्सेशन) है- बल्कि त्रिपाठीजी के ही शब्द लूँ, तो ‘दासता’ ही है, वरना प्रेम का मादन भाव प्राकृतिक है, इससे परे कोई नहीं- न ऋषि-मुनि, न त्रिदेव ही। लेकिन क्रांति गीत व उससे जुड़ी घटना के प्रत्यक्ष प्रमाण को न ख़ारिज कर सकते, न ऐसा करना उचित ही होगा। लेकिन पिटते हुए देशभक्त बच्चे के प्रति शोक-संतप्त उत्तेजना (स्पिरिट) को मान भी लिया जाये, तो यह सिर्फ़ उद्भव के साथ किंचित जुड़ पायेगी। माना कि देशभक्ति का जज़्बा बहुत भावावेग वाला है. लेकिन ‘आँसू’ की प्रकृति नितांत शृंगारी है। अत: इसमें उस बालक की याद के दो-एक बूँद आँसू कहीं एकाध छंद में हो सकते हैं, पर ऐसा कहने वाले त्रिपाठीजी प्रभृति लोगों की कवि व देश के प्रति सारी भावात्मकता की पूरी क़द्र के साथ कहना चाहूँगा कि ‘आँसू’की `समग्र रचनात्मकता के साथ इसे नहीं जोड़ा जा सकता। पूरे काव्य में व्याप्त आलम्बन से बनते अनगिन उद्दीपनों, आश्रय के अनंत अनुभावों व असंख्य संचारियों की संगति इतने-से सन्दर्भ के साथ कैसे बैठेगी? फिर उनमें निहित रूमानियत के मसृण आवेग और उनसे फूटती आकुलता की अतल-अतुल मार्दवता के रूपकों का परिपाक कैसे होगा? राष्ट्रीयता के साथ यह अदद शोकांतिका कैसे सधेगी? कुल मिलाकर यह सच या उद्भावना ‘आँसू’ के उद्भव का एक पूरक स्रोत तो बन सकती है, सृजन-यात्रा में थोड़ी भी दूर चल नहीं सकती, पाथेय बन नहीं सकती।
और संगति न बन सकने वाली इस बात का पता भी दुर्गादत्तजी को था। सो, उन्होंने असंगति की सम्भावना का भी एक तोड़ दिया है- ‘वादों और प्रदर्शन से सर्वथा विमुख एकांत स्वाध्यायी और स्थितप्रज्ञ चिंतक बाबू साहब के ‘आँसू’ से यदि फिर भी उनका (तत्कालीन स्थितियों का) सीधा सम्बन्ध न जुडता हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा और सत्य मौलिक है। इसलिए वातावरण ऐसी आत्मनिर्भर कृति पर अपना आरोपित नहीं कर पाता (वांग्मय-117) ।
यानी प्रकारान्तर से यही कहा जा रहा कि ‘आँसू’ अपने समकालीन वातावरण से परे भी है, जिसका मतलब साफ है कि वह रूमानियत प्रसादजी के मन की बात है। और सिद्ध सत्य है कि बिना कुछ हुए सिर्फ हवा में तो मन में भी कुछ बनता-पकता नहीं। सो, इसके आधार व प्रमाण भी हैं, जो अभी आगे आकलित होंगे।
अभी यह कि दुर्गादत्त जैसे तिसरइते की इस राष्ट्रीय चेतना के बाद ‘उसकी’तलाश में दो ऐसे परिणाम मिलते हैं, जिन्हें पारिवारिक कहा जा सकता है। जो घर व सगे-सम्बन्धियों की तरफ से बड़े सु-मन व सलीके से आये हैं। अपने प्रयोजन में तो इन्हें बालमत, लोकमत कहा जाना चाहिए, पर उद्भव व प्रवृत्ति में ये बालमन और लोकमन ठहरते हैं।