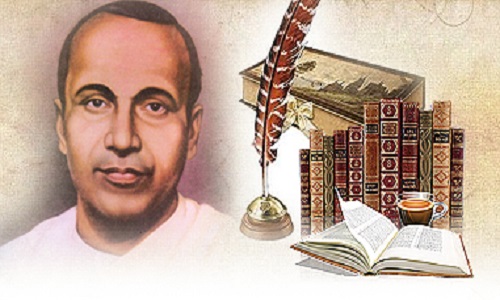सत्यदेव त्रिपाठी
बीसवीं शताब्दी के हिंदी के सबसे बड़े लेखक जयशंकर प्रसाद (30 जनवरी, 1890- 14 जनवरी, 1937) के निधन के 84 साल बाद रज़ा फाउंडेशन की मदद से लेखक-आलोचक सत्यदेव त्रिपाठी ने उनके विषय में प्रकाशित सूचनाओं, शोध और उनकी कृतियों में बिखरे सूत्रों के आधार पर प्रसाद की जीवनी –‘अवसाद का आनंद’- लिखने का उद्यम किया है जो अब पूर्णता की ओर है। प्रस्तुत हैं इसके एक अध्याय ‘उसकी स्मृति पाथेय बनी’ के सम्पादित अंश :
घटित के कालक्रम के अनुसार बालमन को पहले लिया जाये, तो यह प्रकरण सिर्फ कवि के मौसेरे भाई मुकुन्दीलाल गुप्त के यहाँ मिलता है, जो इस कार्य के एक महत्त्वपूर्ण सामग्री-स्रोत भी सिद्ध हुए हैं। उनका यह प्रकरण प्रसादजी की शुरुआती रचना ‘प्रेमपथिक’ से बावस्ता है। उसे कई बार पढ़ने के बाद एक मुँहलगे अनुज की तरह उन्होंने प्रसादजी से पूछा था– ‘भइया मैं ‘प्रेमपथिक का रहस्य जानना चाहता हूँ। उसे पढ़कर मुझे शंका होती है’।
प्रसादजी का उत्तर था– ‘कुछ शंकाएं ऐसी होती हैं, जिनका समाधान किया नहीं जाता, हो जाता है। ‘प्रेमपथिक’ को पढ़ना ही उसका समाधान है’। ऐसे उत्तर देकर बहला देना प्रसादजी को आता था। यह बहलाना सामने वाले की औकात व स्तर का होता था। कभी विनोद व्यासजी ने पूछा, तो कह दिया– ‘जब लिखना, तो बताना – फोटो दे दूँगा’।
जब कलकत्ते में छात्रों ने ‘शशिमुख पर घूँघट डाले…’ वाले छंद का आशय पूछा, तो यह कहकर टाल गये कि जिस मानसिक दशा में लिखा था, उस दशा में पहुँचूँगा, तभी उत्तर दे सकूँगा। इस पर बच्चों ने कह दिया– आप तो शेक्सपीयर जैसी बातें कर रहे हैं, तो प्रसादजी का प्रति उत्तर पुन: रोचक रहा– ‘मैं क्या जानूँ शेक्सपीयर वग़ैरह मुझे तो अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती’। (वाङमय – 246)।
कहना होगा कि प्रसादजी की एक रचना-प्रवृत्ति है आँसू, जो उनकी तमाम कविताओं में वापी-कूप-तड़ागादि के किसी न किसी रूप में मिलती है। परंतु वही प्रवृत्ति ‘आँसू’ में आके नदी बन जाती है। और इसी रूपक को आगे बढ़ायें, तो फिर ऐसे उमगती है कि ‘नदी उमगि अम्बुधि महँ जाई’ को गोया सार्थक करती हुई ‘कामायनी’ में अगाध समुद्र बन जाती है। इस प्रवाह के उत्तरोत्तर क्रम में तीन प्रमुख पड़ाव पड़ते हैं – प्रेमपथिक, आँसू और कामायनी। वही प्रवृत्ति व भाव ‘प्रेमपथिक’ में कथात्मक रूप-शैली में अन्य पुरुष में व्यक्त होकर सामान्य (जनरल) बनकर रह गया है। फिर भी अनुज मुकुन्दी का प्रश्न बना है, जिसका अहसास हर पाठक को भी हो सकता है। और वही भाव ‘कामायनी’ में पात्रमय-कथामय रूप धरकर, महाकाव्य के विधान में ढलकर दर्शन की विराटता में पर्यवसित होकर अति विशिष्ट हो गया है।

यही विशिष्टता न होती, तो वहाँ भी यही प्रश्न बनता, तात्पर्य यह कि ‘आँसू’ ही वह पड़ाव है, जहाँ सीधी समक्षता हुई है। मध्यम पुरुष (‘तुम सुमन नोचते-फिरते’… आदि) के सम्बोधन में ‘उसकी’ के सामने होने का अहसास भी साकार होता है। यहाँ माध्यम व रूपबन्ध का कोई अवगुण्ठन नहीं है। अवगुण्ठन तोड़ा-फाड़ा नहीं गया है– हटा दिया गया है, बल्कि हट गया है– गोकि इतना नहीं हटा कि उतना खुल जाये, जितना कि कला-समक्षता के लिए ग़ालिबन दरकार है-
‘वा कर दिये हैं शौक़ ने बन्दे-नक़ाबे हुस्न, ग़ैर अज़ निग़ाह अब कोई हाइल नहीं रहा’– यानी आवरण रह ही न जाये। यहाँ आवरण है– भले सघन न होकर झीना ही सही, जिसमें से उस प्रिय के प्रति हृदय की असीम वेदना कवि की एकालापी गीतमयता में उमड़ पड़ी है– ‘वेदना असीम गरजती’। अत: सारे सवालों-चर्चाओं का केन्द्र ‘आँसू’ बन गया है।
इस शृंखला में मुकुन्दी के सवाल में ‘उसकी’ की तलाश का एक मामला ख़ूब बनता है। हालाँकि वह सवाल ‘प्रेमपथिक’ से है, किंतु काफी दूर तक जा सकता है। और प्रसादजी के न बताने के बावजूद मुकुन्दी ने ‘उसकी’ का एक रहस्य या एक ‘उसकी’ का राज़ जान लिया, बचपन में एक सजातीय परिवार से प्रसादजी का घरेलू सम्पर्क रहा। वे उस सगोत्रीय परिवार से बहुत घुलमिल गये। उस परिवार में एक प्राय: हमउम्र बालिका थी। दोनो साथ खेला करते थे। किशोरावस्था में आते-आते यह खेल उस सुन्दर किशोरी के प्रति घनिष्ठता में बदलता गया, जो युवावस्था में प्रवेश करते-करते ‘हृदयग्राही प्रेम’ में परिणत हो गया– यानी ‘लरिकइंअवा के परेम’ बन गया- बालमन। समय पाकर उन्होंने अपनी आदरणीया भाभी से परामर्श किया। इस तरह रहस्य जान पाने का सूत्र मुकुन्दी ने कहके बतलाया नहीं है, लेकिन वह प्रकट हो जा रहा है और पुख़्ता भी ठहरता है। भाभी का उत्तर था– ‘तुम दोनों विवाह-सूत्र में नहीं बँध सकते, क्योंकि रक्तगत अंतर अभी सात पुरुषों का नहीं हुआ है’। यानी उस परिवार को इस जाति में आके अभी सात पुश्तें नहीं बीती हैं कि पूर्ण जातीय शुद्धता बने। सो, इस सम्बन्ध की परिणति दुखांत ही रही (वाङमय-223)। यह उद्घाटन मुकुन्दी ने प्रसादजी को बता भी दिया और उनसे ‘जिद्दी’ की उपाधि भी पा ली। इस व्रण को व्यक्त करती ‘प्रेमपथिक’ की दो पंक्तियां–
‘रूखा शीशा जो टूटे तो हर कोई सुन पाता है
कुचला जाना हृदय-कुसुम का किसे सुनायी पडता है?
कालांतर में उस युवती का अन्यत्र विवाह हुआ, जिसमें कवि निस्संग भाव से सम्मिलित भी रहे। इसे मुकुन्दीजी ने प्रसादजी के ‘अनुपम चारित्र्य’ का प्रमाण माना है। लेकिन ऐसे प्रेमांत और शादी में ऐसी मौजूदगियां उस समय की एक विवश प्रेमी-प्रवृत्ति रही कि जब प्रेमिका का सिन्दूर-दान हो रहा है, मुहल्ले या पड़ोस का प्रेमी बारातियों को भाजी परसते हुए उसकी तिखास के बहाने अपने ‘आँसू’ पोछ रहा होता है– ‘कुचला जाना हृदय-कुसुम का किसे सुनायी पड़ता है’?
उसके बाद से मुकुन्दी जब भी ‘प्रेमपथिक’ पढ़ते, कवि के भग्न हृदय की भावना उनके समक्ष मूर्त्त हो जाती। मुकुन्दी ने ‘आँसू’ का नाम लिया नहीं, पर क्या ‘प्रेमपथिक’ के भग्न हृदय की वही ‘घनीभूत पीड़ा’ ही यहाँ ‘आँसू’ बनकर तो नहीं बरस रही है? उसी किशोरी प्रेयसी की स्मृति ही ‘प्रेमपथिक’ के बाद ‘आँसू’ का भी पाथेय तो नहीं बनी है? स्रोत सही है और घनीभूत पीड़ा की स्मृति का कालांतर में बरसने की पूरी प्रक्रिया व सारे परिणामों की कसौटी पर ख़रा उतरता है। स्मृति में छायी ‘उसकी’ का सटीक तोड़ देता है, लेकिन अभी और आगे चलें और लोकमन पर आयें, जिस तरह सुखमय जीवन-काल में ‘आँसू’ के लिखे जाने में किसी प्रिय के अनहोने (न होने) या किसी दुखद भाव के अभाव को व्याख्यायित किया गया, उसी तरह अपने ख़ासों एवं शुद्धतावादियों की तरफ से इसमें औरों के साथ कुछ ऐसा भी आना ही था या उन्हें ऐसा लाना ही था, जो लोक-अनुमोदित हो, और लोक में दाम्पत्य प्रेम ही काम्य है। वही चिरकाल में आदर-सम्मान पाता है – सराहनीय-आदरणीय बनता है।
इधर प्रसादजी की पहली पत्नी बिन्ध्यवासिनी देवी की सुन्दरता व शालीनता की धनक प्रसाद-विषयक अध्ययन-मनन एवं परिवार-जनों से संवाद के दौरान बराबर सुनी जा सकती है। उनके प्रति प्रसादजी की अनुरक्ति का अहसास निरन्तर होता है। उनके दिये नाम ‘प्रसाद’ का कवि द्वारा अंतरिम स्वीकार और गृह-त्याग की अवधि में उनके नाम वाले स्थल ‘विन्ध्य’ पर वास, आदि सन्दर्भ पीछे आये भी हैं। लेकिन यहाँ इस सन्दर्भ को विवेचित करने के आधार हैं- रत्नशंकरजी के उल्लेख। उन्होंने ‘कानन कुसुम’ की अवतरणिका में बड़ी स्पष्ट चर्चा की है और ‘उसकी’ को लेकर तमाम वाह्य अनुमानों का खुला प्रतिवाद भी किया है। रत्नजी ने इस स्मृति और पीड़ा को विशेषत: कवि की प्रथम पत्नी से जोड़ते हुए धारणा बनायी कि ‘उसकी’ यानी बिन्ध्यवासिनी देवी की, जो कवि को बहुत प्रिय थीं।
रत्नजी अपनी बात का सिरा कवि की भाभी लखरानी देवी से जोड़ते हुए लिखते हैं- ‘बिन्ध्यवासिनी देवी को लखरानी देवी लावण्य की देवोपम एक ज्योतिमती मूर्त्ति मानती थीं। वे बताती थीं कि बहू के गले से उतरती पान की पीक झलकती थी। यह मूर्त्त पहचान अप्रतिम सौन्दर्य के मानक रूप में प्रतिष्ठित है– एलिज़ाबेथ के साथ चस्पा है। और यहीं से अपनी बात मिलाते हुए रत्नजी लिखते हैं–
‘सौन्दर्य लावण्य के द्वारा ही अनुप्राणित रहता है अथवा उत्क्रांत लावण्य अपनी घनीभूत अवस्था में जहाँ उद्योतित होता है, वहाँ सौन्दर्य की प्रतिष्ठा पद-ग्रहण करती है। सुतरां सौन्दर्य का आंतरहेतु लावण्य है। ‘आँसू’’ की ये पंक्तियां इस प्रसंग से आसूत्रित हैं, जिसके प्रियतम को लेकर प्राय: अनर्गल अनुमान लगाने का साहस करना कवि पर कुछ लिखने वालों का स्वभाव-सा हो गया है– ‘लावण्य शैल राई सा, जिस पर वारी बलिहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी-प्यारी’।
फिर बिन्ध्यवासिनीजी की जानिब से रत्नजी अपनी बात शुरू करते हैं– प्राचीन लिच्छवी वंश के प्रत्यंत पर जन्म लेने वाली देवि बिन्ध्यवासिनी का शरीर जिन परमाणुओं से रचित रहा, कदाचित् वे उन अंतर्जात व लिच्छवी संस्कारों से संवलित रहे’। इसका प्रमाण देते हुए वे उद्धृत करते हैं ‘काव्य कला एवं अन्य निबन्ध’ से प्रसादजी का कथन–
“(लिच्छवियों की) अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतर-स्पर्श करके भाव-समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति-छाया कांतिमती होती है”। और फिर इसका सूत्र जोड़ते हुए कहते हैं– ‘कवि के अंतर्जगत पर वह छाया ‘आँसू’ में जाकर कुछ इस प्रकार घनीभूत हुई, जिसका परिणाम-बिम्ब ‘कामायनी’ के ‘स्वप्न सर्ग’ की इन पंक्तियों में उस स्वप्नभूत जगत का एक इतिवृत्तपरक चित्र सँजोये है –
‘मानस का स्मृति-शतदल खिलता, झरते बिन्दु मरन्द घने, मोती कठिन पारदर्शी ये इनमें कितने चित्र बने/ आँसू सरल तरल विद्युत्कण नयनालोक बिरहतम में, प्राणपथिक यह सम्बल लेकर लगा कल्पना-जग रचने।
‘कामायनी’ के इस ‘स्मृति-शतदल’ के साथ रत्नजी ‘स्कन्दगुप्त’ से मातृगुप्त का वाक्य भी उद्धृत करते हैं– ‘वह स्मृति दूसरे प्रकार की होगी। उसमें ज्वाला न होगी, धुआँ उठेगा और तुम्हारी मूर्ति धुँधली होकर सामने आयेगी’ (चतुर्थ अंक, तृतीय दृश्य)। यही स्मृति ‘कानन कुसुम’ के ‘समर्पण’ में भी बड़ी गहनता से प्रकट हुई है, जिसका भी उल्लेख रचना-क्रम के अंतर्गत ‘कानन कुसुम’ के सन्दर्भ में हुआ है। इस सारी क़वायद का मंतव्य यही रहा कि ‘आँसू’ की ‘उसकी स्मृति’ किसी अन्या की नहीं, वरन परिणीता पत्नी की है- स्वकीया प्रेम की है। और वह इतनी विशद है कि पूरे प्रसाद-साहित्य में यत्र-तत्र व्याप्त है।
इस तर्क-प्रमाण के पूरे विधान के समक्ष पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि बात इतनी शिष्ट थी, तो स्पष्ट कहने में क्या हर्ज़ था? बल्कि ज्यादा गौरव की बात होती– अधिक सम्मान्य व सबके लिए सराहनीय। फिर ‘उसकी स्मृति’ भी क्यों कहते, ‘प्रिया की स्मृति’ न कहते– निराला के राम की तरह ‘उद्धार प्रिया का कर न सका’! आँसू को स्वर्गीया विन्ध्यवासिनी के नाम समर्पित कर सकते थे, जिसके लिए उनके जैसी प्रतिभा के शब्दकोश में एक से एक मसृण-अनुरागमय सम्बोधन होते, फिर इसे अवगुण्ठन-आवरण में क्यों रखा गया?
दूसरी बात यह कि पत्नी पर ऐसे पूरा काव्य लिखने का कोई सीधा-सधा प्रमाण भी नहीं है। क्योंकि पत्नियां तो मिल जाती हैं– और प्राय: बिना तरद्दुत के। फिर क्या मज़ा? मज़ा तो ‘पाने में नहीं, पाने के अरमानों में’ होता है –‘पा जाता, तो हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला’। फिर वह अरमान अप्राप्त रहकर टूटे, तो काव्य बने, चित्र-मूर्त्ति बने, लेकिन यह पत्नी की नियति से उलट है। हाँ, इस सन्दर्भ में ‘निशा निमंत्रण’ व ‘एकांत संगीत’ के नाम लिये जाते हैं, जहाँ प्रेयसी-पत्नी से असमय चिर-विछोह हुआ था। लेकिन इन कृतियों का भी अंतरिम सच यह है कि ये दोनों काव्य लिखे जरूर गये हैं पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद, पर वे पत्नी-वियोग की पीड़ा के नहीं, मूलत: कवि की पीड़ा के गान बनकर रह गये हैं। इनमें पत्नी श्यामा की स्मृति उस तरह नहीं आती। उनकी याद में फुटकर कवितायें अन्यत्र हैं, जो काफी स्पष्ट भी हैं। उनमें कोई अवगुण्ठन नहीं है।
बच्चनजी के अलावा केदारनाथजी ने पत्नी की 28वीं जयंती पर इसी नाम से कविता लिखी है। और भी कवियों ने कुछ-कुछ कविताएं लिखी हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट ही लिखी हैं– कह-बता के। कोई अवगुण्ठन नहीं रखा है। और इन कविताओं में मेरे देखे-लेखे न वह दर्द आया है, न ‘आँसू’ जैसा उच्च स्तरीय काव्यत्व, जो प्रसादजी के समक्ष अपनी-अपनी औकात का भी मामला है। पत्नी के प्रति तुलसीदास के भीषण प्रेम की कथा है, जिसमें पत्नी की फटकार से उनके महाकवि बन जाने की बात आती है, लेकिन फिर काव्य में रत्नावली कहीं नहीं आतीं। हाँ, सीता-हरण के बाद पत्नी-वियोग में राम रोते हैं, ‘रघुवंश’ में पत्नी-मृत्यु पर ‘अज-विलाप’ विख्यात है। इनमें परित्यक्त तुलसी व विधुर कालिदास के अपने भाव आ गये हों, तो आश्चर्य नहीं, पर इनके भी उस तरह संज्ञान तक नहीं लिये गये हैं। उदाहरण देने की रौ में नागार्जुनजी के ‘अज रोया या तुम रोये थे’ के सिवा किसी ने शायद ही राम व अज के विलापों को तुलसी व कालिदास से जोड़कर देखा हो! इस प्रकार इन संक्षिप्त उल्लेखों के विवेचनों से सिद्ध है कि दाम्पत्य व इतर प्रेम को लेकर सामाजिक चलनों से बनी मनोवैज्ञानिकता के तहत ही सही, किंतु पत्नी-वियोग अब तक अमूमन सीधे-सीधे किसी बड़े काव्य की प्रेरणा न बन सका, प्रतिफलित न हो सका, जिसका अपवाद शायद प्रसादजी भी न हों।
श्यामा धुन सरल रसीली- अब ‘उसकी स्मृति’ को लेकर उस कुतूहल की तरफ चलें, जो इस प्रसंग की अति ख्याति का सबब है। इसमें ‘उसकी’ के लिए अन्या रूप में प्रेमिका का प्रमाण भी सामने है यानी ‘कौन थी वह’ में परकीया के भी ऐसे-ऐसे जीवंत व पुष्ट उल्लेख हैं, जो क़तई नज़रन्दाज़ नहीं किये जा सकते।
इस सन्दर्भ में जो नाम चर्चा के केन्द्र में है, वह श्यामा गौनहारिन का है। इसकी बावत सबसे पहले सीताराम चतुर्वेदीजी का उल्लेख देखें, जिन्होंने ‘उसकी स्मृति’ का सन्धान करते हुए बिना किसी संकोच-सन्देह के निछद्दम भाव से सीधे-सीधे यूँ लिखा है, जैसे कोई प्रत्यक्ष देखी-सुनी कथा हो-
‘प्रसादजी का ‘आँसू’ लघु काव्य उनकी व्यक्तिगत भावना का उद्गार है। काशी में श्यामा नाम की विवाहिता गौनहारिन कबीरचौरा मुहल्ले में रहती थी। वह ठुमरी, टप्पा, कजरी और चैती गाने में दूर-दूर तक विख्यात थी। यों तो काशी में बड़े रामदास, छोटे रामदास, सिद्धेश्वरी बाई आदि ठुमरी के प्रसिद्ध संगीतकार थे, लेकिन चैती और कजरी में श्यामा की जोड़ का कोई न था’ (अंतरंग-94)।
रात-रात भर होने वाले कजरी के तमाम दंगलों में ‘जिस हाव-भाव के साथ श्यामा सुनाती थी, वहाँ तक कोई न पहुँच सका। प्रसादजी को उसकी ठुमरी, चैती, कजरी सुनने का बड़ा चाव था। वे अपने घर पर न सुनकर अन्य स्थानों पर उसके गायन की योजना कराते थे, जिसका पूरा प्रबन्ध वे और विनोदशंकर व्यास ही करते। संयोग से अकस्मात थोड़ी अवस्था में श्यामा का निधन हो गया, जिससे प्रसादजी को बड़ा धक्का लगा। यद्यपि उन्होंने उस समय तो कोई रचना नहीं की, किंतु बहुत वर्षों के पश्चात ‘आँसू’ की रचना कर डाली, जिसके आरम्भ में ही कहा– ‘जो घनीभूत पीड़ा थी’।
इस छंद से ही ज्ञात होता है कि बरसों पहले जिसका निधन हुआ था, उसकी स्मृति उनके मन में निरंतर घूमती रही और अंत में कविता के रूप में प्रकट हुई। यों तो काशी में श्यामा की गायन-शैली के प्रशंसक बहुत थे, तथापि एक प्रसादजी ही ऐसे थे, जिनकी कल्पना में ‘शशिमुख पर घूँघट डाले, आँचल में दीप छिपाये’ वह निरंतर आती रहती थी, जिसे उन्होंने काव्य-समाधि देकर ‘आँसू’ में चिरस्मरणीय कर दिया है (वही- 95)।
चतुर्वेदीजी ने कला-आयोजन के रूप में वाह्य जीवन की जानिब से प्रसादजी के अंतस् में बसी श्यामा की चर्चा की है, लेकिन प्रसादजी के घर में श्यामा के प्रवेश का मुख़्तसर-सा जिक्र संकोच के साथ सन्दिग्ध ढंग से किया है मैत्रेयी सिंह ने, जो बचपन से ही पारिवारिक रूप से प्रसादजी के घर के भीतर तक नियमित आने-जाने वाले लोगों में थीं। वह भी प्रसाद-मन्दिर में किसी मांगलिक आयोजन का ही अवसर था। प्रसादजी की भावज के साथ मैत्रेयी की माँ की ‘खुसुर-फुसुर’ चल रही थी। प्रसादजी किसी काम से आँगन का दरवाज़ा पार करके जैसे ही अन्दर घुसे, वैसे ही गोरी-सी एक लम्बी महिला उठी। उसके दाँत अति पान खाने से काले पड़ चुके थे। उसने एक हाथ फैलाकर प्रसादजी की तरफ गाने के लहजे में कुछ ऐसा गाया कि वे फिर उलटे पाँव वापस लौट गये, महिलाएं गाना रोककर एक दूसरे से इशारे-इशारे में कुछ कहने लगीं। उस इशारे का अर्थ कुछ ऐसा था, जिसे क्या कहूँ, समझ में नहीं आता। उस महिला का नाम श्यामा था। वह गौनहारिन थी’ (अंतरंग-102-3)।
प्रसादजी के काफी घनिष्ठ विनोदशंकर व्यास ने श्यामा की बावत कुछ प्रच्छन्न यानी ‘छिपाते-छिपाते बयां’ करने के बदले बयां करने के बाद छिपाने के अन्दाज़ में लिखा है–
‘बनारस के धनी परिवारों में संगीत व मनोरंजन के लिए गौनहारिनें आया करती थीं। उनका ‘घरेलू संगीत विला’ महीने में दो-एक बार हर घर में चलता। प्रसादजी के भाई के समय में रजवंती नाम की विख्यात गौनहारिन आती। उसके साथ श्यामा नाम की एक कथकिन भी होती। वह दुबली-पतली, सँवलिया रंग की थी। उसकी बड़ी-बड़ी आँखें थीं व लम्बा क़द था। प्रसाद बड़े हंसमुख और दिल्लगी पसन्द थे। मजाक में ही यह सम्बन्ध बढ़ता गया, श्यामा हारमोनियम बजाकर गाती थी, उसकी आवाज ज़ोरों से लड़ती थी। उसमें कोई सौन्दर्य तो न था, पर हाव-भाव-प्रदर्शन करने में कुशल थी। प्रसादजी के पड़ोस में मेरे एक सम्बन्धी रहते थे, उनसे भी उसका संबन्ध था। प्रसादजी के मकान के सामने एक दूसरा मकान था। उसमें भगवती नाम की वेश्या प्राय: आती थी। उसके सम्बन्ध में दिल खोलकर एक दिन सब वृत्तांत उन्होंने मुझसे कहा था। प्रसादजी के शब्दों में वह उन पर रीझ उठी थी। एक दिन 10-15 हजार के आभूषण लेकर वह आयी। कहा ‘यह सब मेरी सम्पत्ति है। मेरी कोई व्यवस्था कर दीजिए। अब मैं बाज़ार में बैठकर व्यवसाय नहीं करना चाहती। प्रसादजी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। वे इस स्थायी झंझट में नहीं फँसना चाहते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रसादजी का आकर्षण उसके प्रति था। वह सुन्दरी थी और सरल भी। स्पष्ट शब्दों में कुछ न कहकर दूसरे प्रयत्नों से प्रसादजी उससे अलग हुए। (भगवती के इस तथ्य पर सम्पादक रत्न शंकर प्रसाद की टिप्पणी है कि वह प्रसादजी के बड़े भाई शम्भू प्रसादजी के समय में रहती थी। उनके निधन के बाद विरक्त होकर वृन्दावन जाने का निश्चय किया। प्रसादजी ने आभूषण नहीं लिये, पर उसकी व्यवस्था कर दी (139)।