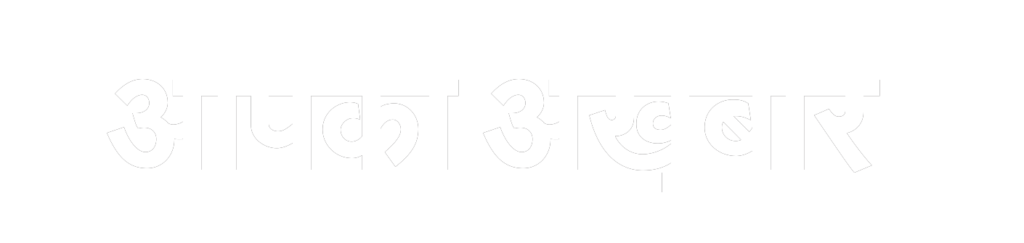प्रदीप सिंह।
प्रदीप सिंह।
क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन कर रहा है? क्या देश का संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह संविधान में संशोधन कर सके? ये मुद्दा इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यों की खंडपीठ का फैसला आया है जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश दिया गया है जो आज तक कभी नहीं हुआ। यह अभूतपूर्व है। भारत का संविधान देश ने 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। तब से ऐसा कभी नहीं हुआ।
लेकिन, अब यह हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार के तहत यह किया है इसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं। मैंने इस बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की है उसके आधार पर आम जनता के मन में उठ रहे सवालों-शंकाओं के समाधान की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी अदालत पर चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, कॉन्सिट्यूशनल कोर्ट हो, या कोई और उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं संसद और सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। केवल अपनी बात रख रहा हूं लोगों के सामने।
पहली बात, यह मामला शुरू कैसे हुआ? मामला शुरू हुआ तमिलनाडु से। तमिलनाडु के गवर्नर ने तमिलनाडु विधानसभा से पास कई विधेयकों को मंजूरी देने से रोक दिया। फिर लंबे समय बाद उन्होंने उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की और जो किया वो बिल्कुल आसमान फटने जैसा है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्देश दिया कि आपके पास जो विधेयक मंजूरी के लिए आएगा उसको आप 90 के दिन के अंदर मंजूरी देंगे- और नहीं देंगे तो मान लिया जाएगा कि मंजूरी मिल गई। इस फैसले का नतीजा यह हुआ कि तमिलनाडु विधानसभा से पारित 10 विधेयक बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति के मंजूरी के कानून बन गए। ऐसा इस देश में पहले कभी नहीं हुआ।
सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार कहां से मिला? सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 142 से मिला है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रीशनरी पावर देता है। ये डिस्क्रीशनरी पावर इसलिए दी गई है कि अगर कोई प्रक्रियागत अड़चन आ रही है या किसी कानून की वजह से पीड़ित या याचिकाकर्ता को पूर्ण न्याय नहीं मिल रहा है, तो पूर्ण न्याय देने के लिए इन दोनों अड़चनों को लांघकर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। लेकिन याद रखिए यह पूर्ण न्याय देने के लिए है। कोई भी पावर एब्सोल्यूट नहीं होती, अनु. 142 में सुप्रीम कोर्ट दी गई पावर भी एब्सोल्यूट नहीं है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को क्वासी लेजिस्लेचर और कुआसी एग्जीक्यूटिव पावर (अर्ध-विधायी शक्ति और अर्ध-कार्यकारी शक्ति) भी देता है।
अब आप इस बात को समझिए कि संविधान से संबंधित कोई मामला हो, अगर सरकार ने कोई कानून पास किया है, उसको संविधान की कसौटी पर कसना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। लेकिन यह काम सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर सकती है। यहां यह काम खंडपीठ ने किया है। यह मामला अगर संविधान पीठ के पास गया होता, वहां से फैसला होता तो स्थिति थोड़ी अलग होती। लेकिन यहां पर 142 का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया है उस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की यह टिप्पणी बहुत बड़ा बयान है कि सुप्रीम कोर्ट ने 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया है। जगदीप धनखड़ एक संवैधानिक पद पर हैं और वकील भी रहे हैं। वो जानते हैं कि जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है।
तो यह अब मामला किसी एक मुद्दे पर अदालत के फैसले का नहीं रह गया है। यह सीधी लड़ाई संविधान के तीन अंगों न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों के बंटवारे पर आ गई है। संविधान का अनुच्छेद 50 तीनों की शक्तियों का बंटवारा करता है और इनमें एक संतुलन स्थापित करने की बात करता है। यह फैसला विधायिका और कार्यपालिका दोनों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। यह एक तरह से सरकार और संसद दोनों को चुनौती है कि पास करते रहो कोई कानून उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे बदल देंगे, पलट देंगे।
आप पिछले 77 साल का भारत का इतिहास देखें तो जब-जब सरकार ने कमजोरी दिखाई है तब-तब न्यायालयों ने ऐसा ही काम किया है। और जब सरकार ने मजबूती दिखाई है तो सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया है।
अभी तक हम लोग यह देखते रहे हैं कि जो रसूख वाले- पहुंच वाले- प्रभावशाली लोग हैं, उनके लिए कानून अलग तरह से व्यवहार करता है और आम आदमी के लिए अलग। अब यह नया फिनोमना देखने को मिल रहा है कि न्यायाधीशों के लिए भी कानून अलग तरह से व्यवहार करता है। यह सिलसिला अगर चलता रहा तो लोगों का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा।
विस्तार से जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक और ‘आपका अख़बार’ के संपादक हैं)