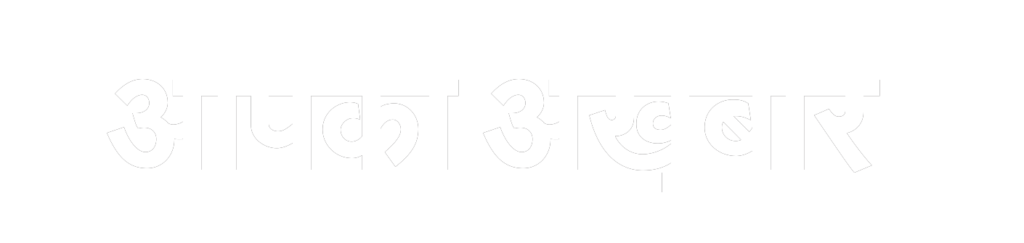सत्यदेव त्रिपाठी।
सत्यदेव त्रिपाठी।
मुम्बई के सातबंगला इलाक़े में स्थित ‘रंगशीला’ थिएटर में मध्यप्रदेश की सरज़मीन के लोगों के किये नाटकों का एक नाट्योत्सव आयोजित हुआ…। यह इलाक़ा मुम्बई महानगर में एक अच्छे नाट्यकेंद्र के रूप में उभर कर नामचीन हो रहा है। जब ‘पृथ्वी’ थिएटर जैसे ऐतिहासिक केंन्द्र व नेहरू सेंटर, रवींद्र नाट्यमंदिर, एनसीपीए…आदि नाट्यस्थल आम रंगकर्मी के लिए कालिदास के ‘प्रांशुलभ्ये फले’ (बड़ी बाँहों से पाये जाने वाले फल) के समान उनकी पहुँच व औक़ात से बाहर होने लगे, तो पिछले कुछ सालों से नयी राहों के कुछ अन्वेषी एवं उत्साही व ज़हीन रंगकर्मी इस इलाक़े में प्रयोग करने लगे…और आज यहाँ छोटे-छोटे आधे दर्जन नाट्यस्थल विकसित हो गये हैं और नितांत अल्प सुविधाओं में भी अपेक्षाकृत अच्छा नाट्यकर्म करके ये लोग सिद्ध कर रहे है कि ‘क्रिया सिद्धि: सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे’ (महान (कर्मठ) लोगों के काम साधनों से नहीं, साधना से होते हैं)। बहरहाल,
१६ से १९ जून के दौरान हुए इस उत्सव में चार नाटक खेले गये – बेटर हाफ़; डार्लिंग, अपनी बात ही कुछ और है; गंध एवं मटियाबुर्ज। ‘मटियाबुर्ज’ की विस्तृत चर्चा यहाँ पहले हो चुकी है। हालाँकि इस बार तीन मुख्य पात्र बदल गये हैं, फिर भी नाटक और उसका रचनाविधान तो वही है। अस्तु, तीन ही विवेच्य हैं।
लेकिन उससे पहले इस आयोजन की बावत यह कहना बनता है कि साढ़े तीन दशकों की मेरी जानतदारी में ऐसा शायद मुम्बई में पहली बार हुआ है कि एक ख़ास प्रदेश के निर्देशकों के नाटकों का उत्सव आयोजित किया गया हो! और ऐसा करने का श्रेय जाता है आज के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी जयंत देशमुख को, जो नाम और कहने-कहाने में नहीं, काम में विश्वास करते हैं। इसीलिए तो आयोजक का नाम कहीं उजागर नहीं हुआ…। बस, शीर्षक दिया गया – ‘मध्य रंग़ नाट्य उत्सव, २०२५’। इससे भान होता है कि २०२५ के बाद २०२६-२७…के रूप में यह वार्षिक आयोजन हुआ करेगा…। हमारी शुभकामनाएँ इनके साथ होंगी और शहर को अच्छे नाटक देखने का सुख मिलता रहेगा – आमीन!!
इससे प्रेरित होकर शायद अन्य प्रांतों के नाटकों के उत्सव भी हों – बिहार की नाट्य-सम्पदा और वहाँ के लोगों की मुम्बई में विपुल मौजूदगी को देखते हुए उनसे तो अवश्य उम्मीद रहेगी – काश, वहाँ व अन्य प्रांतों से भी कोई-कोई जयंत देशमुख आगे आयें…। बस, नाम में ‘रंग़’ व ‘नाट्य’ दोनो शब्द आके दुहराव कर रहे हैं…इसे ‘मध्यांचल नाट्योत्सव /रंगोत्सव’ करके ज्यादा सही व अर्थवान किया जा सकता था…और इस बात को ‘नाम में क्या रखा है’, कहके टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ‘राम ते बड़ो राम को नामा’!! बहरहाल,
यह उत्सव बेहद सादगी के साथ आयोजित हुआ – याने न कोई ताम-झाम, तड़क-भड़क, गहमागहमी…। न उद्घाटन, न मुख्य अतिथि…। बस, नाटक पूरा होने पर निर्देशक को पुष्पगुच्छ के अलावा सिर्फ़ नाटक व नाटय-कर्म…। हाँ, नाटक में पिजे तमाम ज़हीन व कुछ नामचीन लोगों की शालीन उपस्थिति एवं प्रदर्शन के पहले व बाद में उनकी आपसी बातचीतों से गुंजायमान होती रहीं शामें…!!

पहली शाम खेला गया – ‘चेतना’ रंग़ समूह का नाटक – ‘बेटर हाफ़’ और एक बार फिर कयास बढ़ा कि अंग्रेज़ी नाम रखने से हिंदी नाटक आधुनिक व स्तरीय हो जाते हैं…। दूसरी बात यह कि ‘बेटर हाफ़’ तो मूलतः पति-पत्नी दोनो के लिए होता है और नाटक में इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन व्यवहार में आज यह सिर्फ़ पत्नी के लिए रूढ़ हो गया है, जो कहीं उसके दोयम नंबर होने की ज़ाहिर सामाजिक स्थिति की क्षतिपूर्त्ति स्वरूप सांत्वना के लिए हुआ होगा। लेकिन नाटक में पति की भूमिका निर्णायक है, जो ‘बेटर हाफ़’ के दोनो अर्थों से किंचित अलग है!!
अब नाटक की बात पर आयें…तो पति-पत्नी के प्रेममय जीवन वाले इस नाटक को दाम्पत्य-प्रेम में अनुरक्ति की मिसाल कहा जा सकता है। जीवन में इस हद तक का प्रेम वांच्छित है, पर सम्भव नहीं। लेकिन साहित्य-कला तो ‘असम्भव का संधानी’ हैं, तो यहाँ होता है। नाटक के लेखक-परिकल्पक व निर्देशक आशीष श्रीवास्तव ने यही किया है, जिसमें वे आशातीत रूप से सफल होते दिखते हैं। इस सफलता में चार चाँद लगा रहा है आज का ताज़ा-तरीन माहौल, जिसमें हनीमून-यात्रा में ही पत्नी अपने पति का क़त्ल कर देती है। पति से बचकर प्रेमियों से मिलना भी बारहा उजागर हो रहा…। अब के पहले पति ही ऐसा करता था। सो, ऐसे नये विकास के समक्ष यह नाटक एक नज़ीर बनता है…ख़ुदा करे, इसे देख-सुन कर कुछेक वारदातें रुक जायें…!!
पहले दृश्य में ही पति-पत्नी -प्रशांत चटर्जी व सुधा चटर्जी- बगीचे में बैठे हैं और मीठी-मीठी आपसी बातों में तो प्रेम बरसता ही है, पति की कविता और पत्नी का गायन उनके प्रेम के माध्यम व मानक बनते हैं। कविताएँ व गीत भले कवियों के हों, जीवंत गायन तो सुधा चटर्जी बनी नीति श्रीवास्तव का ही है। बातचीत, हाव-भाव से युक्त उनका पूरा अभिनय कौशल भी समर्पित पत्नी की सारी स्त्रियोचित भावुकता से बना है, जो आज के आधुनिक युग को पिछड़ापन भी लग सकता है, पर नाटक इसी का है। यूँ दोनो एक दूसरे में भूले व डूबे होकर असली जोड़े जैसे अच्छे लगते हैं, जो उनकी सुंदर अभिनय कला का प्रमाण है। उनका थोड़ा-सा झगड़ा भी प्रेम के लिए ही होता है और प्रेम से ही समाप्त होकर और भी विलसने लगता है। कुल मिलाकर दोनो सचमुच के प्रेमी-प्रेमिका लगते हैं, जो निर्देशक व कलाकारों के योगदान से होते हुए नाटक का श्रिंगार बनता है।

इन दोनो की सधी हुई युति में तो प्रेम खिलता है, पर प्रेम की असली परीक्षा तो बिछड़ने के बाद होती है। और यहाँ प्रिया के चिर वियोग की स्थिति बनती है। लेकिन इकला वियोग-वर्णन निराधार होता…, तो मौत में अस्पताल की गलती को जोड़कर समय व समाज को भी शामिल कर दिया गया है। अब पति को लड़ाई में तन-मन-धन…सब लुटा देने का अवसर मिलता है…। इस लड़ाई में अस्पताल की तरफ़ से गुंडे द्वारा धमकी दिला के मुक़दमा वापस लेने की भ्रष्टता भी नाटक को जमाने के कटु यथार्थ से जोड़ती है, जिससे एक और नाटकीयता भी बनती है। इससे प्रशांत को प्रेम में जान की बाज़ी लगाने का अवसर व श्रेय मिलता है एवं इससे नाटक में नैतिक मानदंड भी बनते हैं।
इस लड़ाई के दौरान प्रेम का एक और रूप सामने आता है, जब अकेले में प्रशांत को अपनी सुधा दिखने लगती है -बातें होती है, मान-मनौवल होती है…। इस रूप में नीतिजी को पुनः मंच पर आने का अवसर व इकले तड़पते प्रशांत को सहारा मिलता है…और इस तरह मंच भी सूना न होकर दुकेला हो जाता है। मृत का यूँ प्रकट होना प्रेम की असीम गहनता का पराभौतिक रूप है, जिसे व्यवहार में सनक (आँब्सेशन) भी कहा जाता है। लेकिन प्रशांत के प्रेम की यही दीवानगी मुक़दमे में अधिक परवान चढ़ती है। असल में इनके वकील को भी शुरू में पैसाखाऊ होने की छाप दी गयी है, लेकिन जब वह प्रशांतजी से सुन लेता है कि पत्नी का मंगलसूत्र तक बिक गया है, फिर भी उन्हें मुआवज़े में नहीं, पत्नी के लिए न्याय मात्र में रुचि है, तो वकील का पात्र बदल जाता है। हालाँकि नाटक में इस बदलाव का कोई संकेत नहीं होता – बस, समझने की बात है। इससे नाटक पुनः अपनी भावात्मक ज़मीन पर आ जाता है। फिर तो फलागम तक पहुँचता है – वकील साहब फ़ोन पर प्रशांत एवं दर्शकों को केस जीतने व अस्पताल को हरजाना भरने के फ़ैसले की खबर सुनाते हैं, तो नायिका की मृत्यु के बावजूद नाटक आधा सुखांत भी बन जाता है…।

मुख्य भूमिका के अनुरूप प्रशांत बने राजीव श्रीवास्तव ने पूरे नाटक को अपने सबल कंधों पर यूँ उठाया है कि देखते ही बनता है। वही कर्त्ता भी हैं, भोक्ता भी। संयोग व वियोग दोनो में उत्कट प्रेमी हैं, तो प्रेम में बदले के लिए लड़ाकू भी। इन सबको बखूबी निभाते हैं। उनके रूप-रंग़-उम्र-वेश-गति एवं आवाज़ के साथ उच्चारण में भाषिक शुद्धता है, तो प्रसंगानुसार भाव-परिवर्तन एवं तदनुसार सही लहजा भी। फिर अनुरूप हाव-भाव एवं अंग-संचालन…आदि को मिलाकर एक अदद कलाकार की छबि बनती है, जिसके सामने वेश-भूषादि गौण हो जाते हैं – वैसे राजीवजी का व्यक्तित्व ‘सर्वं शोभनीयं सुरूपम् नाम’ भी है। अन्य कलाकरों में पहले प्रवेश में वकील बने आशीष अरोड़ा ज्यादा फबते हैं, फिर उसके बाद भूमिका ही हस्बमामूल हो जाती है। नाटक लिखा-खेला ही ऐसा गया है कि राजीव-नीति के अलावा किसी की भूमिका ख़ास है ही नहीं…और नीति भी शुरू से अंत तक एकरस – महज समर्पिता पत्नी।
बेहद ख़ास होकर बड़ी फ़ालतू-सी बन गयी भूमिका इकले बेटे राहुल चटर्जी की है – गोया अनाथ बच्चा हो!! उस भूमिका पर बिलकुल काम नहीं किया गया है – न करने में न दिखने में…!! पल्लवी का वस्त्र-विन्यास एवं आशीष का मेकअप या तो राहुल को छू ही नहीं गया…या फिर छुआ, तो बोहार गया…!! इकलौते बेटे का इस तरह बेउकुर हो जाना न जँचता है, न पचता है, क्योंकि जीवन में ऐसा होता नहीं – जब तक कि गम्भीर नालायकी जैसी कोई वजह न हो। शहर से दूर बाहर पूना में नौकरी करता वह क्या परिवार में भी बाहरी हो गया है? ये सब सवाल लेखन से जुड़े हैं। यह एकांगिता उनके दाम्पत्य प्रेम की भी बड़ी हानि है। पति-पत्नी अपने में क्या इस तरह खोये हैं कि लेखक की जानिब से बेटे के लिए कोई वास्ता ही नहीं। पत्नी का मुक़दमा लड़ने में ऐसा भी क्या एकाधिकार कि इतने सयाने बेटे से कुछ साझा ही न हो – गोया उसकी माँ मारी ही न हो! है न आश्चर्यजनक…!!
गुंडे के रूप में शिव कटारिया ध्यान खींचते हैं, लेकिन डॉक्टर रूप में उनकी भूमिका चलताऊ ही बनी है – वैसे मुख्य दोनो पात्रों के अलावा सब चलते-फिरते ही हैं। नाट्य-विधान भी चलता-फिरता है – घर से अस्पताल और वकील के ऑफ़िस जैसे स्थल बदलने में नाटक का चलना उसके चलता-फिरतापन को और उजागर कर देता है…। इस आवाजाही को साधने में कमाल जैन के सुविहित रंगदीपन को भी काफ़ी मशक़्क़त करनी पड़ी है। यूँ तो वकील से मिलने वाला दृश्य भी फबता नहीं, पर अस्पताल का दृश्य तो निहायत कामचलाऊ हो गया है। हाँ, यह सब मंचन की दृष्टि से एक मायने में काफ़ी मुफ़ीद यूँ कहा जायेगा कि कहीं भी कभी भी कर लेने के उपयुक्त है। और यही इस प्रस्तुति का सबसे बड़ा ग़ुण है, लेकिन कर लेने और होने के फ़र्क़ को खूब जहिरा देता है…। इसी सबमें फाँसी लगाने वाला किंचित मुश्किल दृश्य बड़ा सटीक घटित होता है – असरकारक एवं सराहनीय। नाटक एक बार अवश्य देखने लायक़ है, लेकिन किसी ख़ास द्व्न्द्व के बिना सपाट होने से विचार लायक़ नहीं बन पाता…!!

इस उत्सव की दूसरी प्रस्तुति रही – ‘पाहुना लोक जनसमिति’, टीकमगढ़ (म.प्र.) के लिए बनी ‘डार्लिंग, अपनी बात ही कुछ और है’। इसमें भी ‘बेटर हाफ़’ के सजातीय ‘डार्लिंग’ को यदि ‘प्रिये’ कह देते, तो हिन्दीभाषी प्रदेश में बड़ा फ़र्क़ पड़ जाता!! याने संवेदना हिंदी की है, पर दिमाँगी सोच का ढाँचा गढ़ती है – अंग्रेज़ी!! इस पीढ़ी को ‘माडर्न’ होने से कोई रोक नहीं सकता!! यूँ नाटक का नाम जितना अदामय (स्टाइलिश) है, वैसी ही अदा में नाटक बनाया भी गया है, जो बना तो है – मीडिया (फ़िल्म-टीवी) में काम करने के लिए गाँव से मुम्बई आये एक युवक की संघर्ष-कथा पर, लेकिन यह बन गया है – एक झूठे व बेवजह फ़रेब रचने वाले युवक की प्रपंच-कथा।
क्या मीडिया में काम करने की इच्छा ने उसे झूठा बनाया है? यदि हाँ, तो न ऐसा दिखाया गया है, न ऐसी छबि है मीडियाकर्मियों की। याने पेशा गौण है – बात उस शख़्स की वृत्ति की है। वह कुछ भी करने आता, यही करता…, क्योंकि लेखक को कराना यही था।। बस, अभिनय-परीक्षण (ऑडिशन) के बदले तब दूसरा कोई परीक्षण होता…। तब भी वह ऐसे ही अपने लिए भाड़े का कमरा लेता और निर्मल जैसे किसी को मौसेरा भाई बनाकर उससे भाड़ा लेता। मकान मालिक तो ऐसा ही तक़ादा करने वाला होता…। क़र्ज़ देने का धंधा करने वाला कोई वहाँ भी होता ही…। वह फ़िल्म निर्माता के बदले कहीं और नौकरी-धंधे के लिए घूस देने के नाम पर पैसे लेता – धोखा खाता…। क़र्ज़दार ऐसे ही ग़ुलाम बना लेता!!…आदि-आदि। याने यह कथा नकारात्मक वृत्ति के युवक की है – मीडिया तो बस लेबल है।
बस, एक फ़र्क़ पड़ता – तब इसे ठगने वाले फ़िल्म-निर्माता के साथ जाँघें दिखाने वाली नायिका नाचने न आती!! तो क्या नाटक इसलिए बना है कि मीडिया में व्याप्त वीभत्सता दिखाये…? यदि हाँ, तो क्या यह नग्नता मीडिया की सामान्य वृत्ति है? चलो, हो भी…तो इसे लेकर नाटक की दृष्टि क्या है? यदि मीडिया की कुरूपता दिखाना इष्ट है, तो इस कोशिश में क्या नाटक ज्यादा कुरूप नहीं हो गया है? फिर मंच पर ऐसा दिखाना…नाटक को सरनाम करके ज्यादा चलाने-कमाने का वीभत्स नुस्ख़ा भी नहीं है? यह नाटक ऐसे ऑडीशनशील युवक की कथा बन गया है, जिसमें तर्क, संगति और समझदारी के सिवा सब कुछ है। नाटक देखने, उन पर लिखने के मेरे साढ़े तीन दशक की गवाही में इतना वीभत्स खुलापन मंच पर नहीं आया था। और वह भी मुम्बई नगरिया से नहीं, टीकमगढ़ से आया है!! १९९० के आसपास शफ़ी इनामदार ने बोल्ड प्रयोग के दो नाटक किये थे – ‘अदा’ और दूसरे का नाम भूल रहा हूँ, जिन पर ऐसी बमचख मची, कि जो बंद हुआ, तो फिर अब तक नहीं आया। देखें, इस बदले समय में ‘डार्लिंग…’ का क्या होता है? लेकिन नर्तकी-अभिनेत्री टीना बनी वृंदा ठाकुर की ढिठाई (बोल्डनेस) भी ऐसे ग़ज़ब की है कि अभिनेत्री के देह की चकाचौंध अभिनेयता की ही बाड़ बन जाती है…!! इस ठगहारी वाली फ़िल्म के निर्माता व धौलिया के कमरे वाले मकान के मालिक की दोनो भूमिकाओँ में मिहिर मौशू यथोचित हैं।
दूसरी बात कि दशक भर से मुम्बई में संघर्षरत बंदा मि. धौलिया इतना भोहर (मूर्ख का हल्का संस्करण) है कि इतना पैसा यूँ फेंक आयेगा!! उधर वह पेशेवर काइयाँ क़र्ज़दाता इतना अनाड़ी है कि गाँव में खेत की बात सुनकर इतने पैसे दे देगा!! लोग तो खेतों के काग़ज़ कोर्ट तक जँचवा के लेते हैं। फिर आज का डिजिटल युग और इतना फ़रेबी धौलिया…लेकिन शहर के किसी कोने में उस क़र्ज़दाता का दरबान होकर क़ैदी बना बैठा है…याने कुछ भी!! वह तो बिना टिकिट भी शहर बदल लेता – फ़िल्म ‘कथा’ के फ़ारुख शेख़ को याद कर लो। याने पूरा का पूरा कथा-वितान हवा में उड़ रहा है…। अपने ही गढ़े चरित्र के साथ भी इतनी मनमानी नहीं चलती मान्यवर संजयजी!!
लेकिन इस मि. धौलिया की करनी लेखक की भरनी के चलते चाहे जितनी ऊलजलूल हो गयी हो, धौलिया बने आदित्य शर्मा का अभिनय इतना बेहतरीन है कि यदि आप नाटक पर सोचें न, दिमाँग बंद करके सिर्फ़ देखें, तो उसका अभिनय देखने के लिए भी नाटक देखा जा सकता है। नयनाभिराम काम है बंदे का। उसका अंग-अंग नहीं, पोर-पोर नहीं – रोम-रोम बोलता है। उसमें नख-शिख भरा है अभिनय…। लम्बी-गोरी-छरहरी देहयष्टि को इतना लचीली बना लेता है, कूदने-फाँदने-भागने-गिरने-लड़खड़ाने-लटकने…आदि जैसी सभी गतिविधियों को ऐसे निभा जाता है – गोया यही उसका २४ घंटे का रमना हो। हाथ-पाँव व उँगलियों से लेकर होठों-आँखो-पलकों-भौहों-ललाट…आदि सभी गतिशील व अदामय अंगों से कुछ भी कहने व भावों को व्यक्त करने को ग़ज़ब का अंजाम दिया है। बंदे की वाचा भी विराम व गति को साधती हुई प्रांजल भी है और मंथर भी। भाषिकता तो इतनी सही…कि क्या कहने!! पूरे समय में शायद दो ही शर्ट बदलता है, पर दोनो इतने फबते हैं कि जैसे धौलिया के लिए ही ये ख़ास बने हों।

पर ऐसे अभिनेता को नाट्यालेख में इतना बुद्धिहीन बना देना कभी खलता है, पर यह दूसरे सिरे से ‘विरुद्धों का सामंजस्य’ भी यूँ बन जाता है कि धौलिया की इस गति-अदा-जोश-चंचलता के समक्ष व समानांतर उसके साथ रहने वाला और मीडिया-लेखक बनने आया निर्मल बड़ी शांति-संजीदगी से अपना रास्ता बनाता है। यही स्थिति निर्मल बने रामप्रिय गंगवार (गैंगवार नहीं) की अदाकारी की भी है। धौलिया यदि खल-खल, छलछल बहती तेज धार है, तो गंगवार शांत-निश्चल गहरा जल। इस तरह दो भिन्नरूपी अभिनय की समक्षता का सौंदर्य आपोआप बन जाता है, जो संजय की सूझ से नाटक की बूझ बन गया है। निर्मल का चरित्र कथ्य में भी धौलिया का पूरक है कि मीडिया में सफल होने की संभावनाएँ बनी रह जाती हैं…और यह भी इस जीवन का बहुत बड़ा यथार्थ है। नाटक के धोखे-छल-फ़रेब की दुनिया में इन दोनो की दोस्ती या फिर निर्मल की सज्जनता-समझदारी भी व्यक्त होती है अंत में, जब वह कमा के धौलिया का सारा क़र्ज़ चुकाने की बात करता है, तो जाने या अनजाने ही सही, मनुष्यता जी उठती है, जो पूरे नाटक के छल-प्रपंच वाले यथार्थ पर भारी है। मकान मालिक पाटेकर और फ़िल्म-निर्माता सातविंदर की दोनो भूमिकाएँ करने वाले मिहिर मौशू दोनो के अनुरूप यूँ अंजाम देते हैं कि सहसा पहचान में भी न आयें…!
मुझे लगता है कि जो भी नाटक में हुआ है, सब पर पैनी नज़र है निर्देशक संजय श्रीवास्तव की। इसलिए जो हुआ है, वही नाटक में होना तय था। अतः जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की कहावत चरितार्थ हुई है और इस सृष्टि में निहित दृष्टि तथा दृष्टि से निरूपित सृष्टि पर चर्चाएँ होती रहेंगी – यही रंगकर्म की प्रकृति है।

संयोग देखें – उत्सव की तीसरी प्रस्तुति और तीन कहानियों की नाट्यत्रयी! हिंदी में ‘कहानी का रंगमंच’ तो है ही, जो शुरुआती बाढ़ के बाद इधर अब रिमझिम-सा हो रहा है…; लेकिन मनीश शिर्के का यह नाटक ‘गंध’ मूल में वैसा ही होते हुए भी प्रयोग में वैसा इकहरा व कामचलाऊ न होकर अधिक नाट्यमय है। इसे करने के लिए ख़ास सूझबूझ की दरकार है, जो इस प्रस्तोता में है। मेरी जानकारी में ऐसा पहली बार हो रहा है…और ऐसा है, तो मनीश शिर्के इसके पुरस्कर्त्ता होंगे, लेकिन भारत की ‘विपुला अनंत धरणी’ में शायद कहीं हुआ भी हो।
इसमें एक ख़ास विषय से जुड़ी काहानियाँ होती हैं – जैसे ये तीनो ‘गंध’ से जुड़े हैं। हालाँकि ‘गंध’ शब्द के तनीकी तौर पर दो भेद है – सुगंध एवं दुर्गंध। लेकिन व्यवहार में आजकल गंध शब्द दुर्गंध की तरफ़ झुक गया है – ‘गंध आ रही है’ का मतलब दुर्गंध ही है। क्लासिक फ़िल्म ‘भवनी भवाई’ के ‘गंध केम जती नथी’ (गंध क्यों नहीं जाती)? में यह अर्थ विश्रुत है। इसी से यहाँ ‘गंध’ शीर्षक उतना सही व संगत नहीं ठहरता, क्योंकि इसमें सभी गंधें जिन्हें भी आती हैं, उन्हें प्रिय हैं। अतः होना तो चाहिए सुगंध। अथवा गंध-सुगंध के बदले निरापद शब्द हो सकता था ख़ुशबू। हिंदी का अच्छा शब्द है – ‘महक’, जिसका विलोम होता है – झझक, जो कम ही चलता है। लेकिन शब्दों पर इतना सोचना शायद आज की वृत्ति नहीं, जो रंगकर्म जैसे शब्द-संधानी कलारूप में ठीक नहीं। लेकिन ये लोग भी जितना विस्तृत विवरण व दस्तावेज (डिटेल डेटा) खुद का देते हैं, नाटक का नहीं देते। तीनो कहानियों में अलगाव यही है कि इनके लेखक और कथानक अलग-अलग हैं। लेकिन दो समानताएँ बहुत ख़ास हैं। पहली कथ्य की – सबमें कोई न कोई गंध आ रही है और वे भिन्न-भिन्न उम्र व क्षेत्र तथा अलग-अलग सम्बंधों-सरोकारों के लोग हैं। दूसरी है कि वृंदा ठाकुर एवं राम गंगवार ने तीनो में मुख्य भूमिकाएं निभायी हैं…और वे जिस तरह एक के बाद दूसरे-तीसरे कथा-प्रयोग में तुरत-फुरत वेश-भूषा से लेकर भूमिका और मानसिकता तक को बदल लेते हैं, जिसे ‘भूमिका में आना’ (बीइंग इन रोल) कहते हैं, वह ग़ज़ब का है!! वेश-भूषा भी अलग है, जिसे बदलकर समय से मंच पर आ जाना भी एक पूरा नाटक है। यह सारी सिफ़त ऐसी कि एक से दूसरे में आकर सहसा ये पहचान में नहीं आते। इन सबके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाये, कम है। लेकिन असली प्रशंसा तो निर्देशक मनीश शिर्के की करनी होगी, जिनका यह आइडिया है और जिनने कहानियों के चयन से लेकर उनके रूपायन तक का इतने कौशल से विधान रचा। सही कलाकार चुने, नक्षत्र शिर्के से प्रकाश-नियोजन तथा संगीत-संयोजन कराया।

और अब नाटकों पर आयें…स्कूल के दो बच्चों पर आधारित पहली कहानी समता सागर की लिखी हुई है – ‘स्कूल की ख़ुशबू’। कितना स्थूल नाम है!! इसमें लड़की चित्रा और लड़के सागर के बीच दोस्ती होती है और किशोर वय से कम उम्र के दोनो बच्चे विद्यालय की छोटी-छोटी बातों को आपस में साझा करते हुए खुश होते रहते हैं…। इस दौरान दोनो युवा कलाकार बिलकुल बच्चों जैसी छाप छोड़ते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे एक दूसरे के कितने पास आ गये। अहसास तब हुआ, जब लड़की के पिता के दूसरी शादी कर लेने के बाद मां की ग़रीबी वश उसकी पढ़ाई छूट गयी…। फिर दोनो ही उन बीते क्षणों की महक में एक दूसरे को याद करते रहे…!!
दूसरी कहानी रही – हर्शल अल्पे की ‘देहगंध’। कितना अच्छा नाम है!! इसमें टैक्सी चालक मोहन के पसीने-सने कपड़े वाली देह-गंध से सम्भ्रांत लड़की मोयरा इतना मुतासिर हो जाती है कि फिर उच्च वर्गीय जीवन की इत्र-फुलेल की ख़ुशबू उसे भाती ही नहीं…और उसी देहगंध की याद में उसी की मुंतज़िर रहती है। इससे ठीक उलट है सर्कस के जीवन पर आधारित विशाल कलमबकर लिखित ‘ज़िंदगी की ख़ुशबू’। कितना सपाट-सा नाम है!! इसमें करतब करने वाली लड़की सोना को इत्र-फुलेल वाली उच्चवर्गीय ख़ुशबू पसंद है और उसके सहकर्मी जोकर बने बबलू को पसंद है – मां के सिले हुए कपड़ों की घरेलू गंध, जिसके छूट जाने के डर से वह क़मीज़ धोता ही नहीं। इसमें संवेदनात्मक पहलू बहुत ज़हीन व स्पष्ट है। लेकिन ‘पसीने की गंध बनाम इत्र की ख़ुशबू’ वाली इन दोनो कहानियों में एक तरह से दुहराव ही है। इससे बचने के लिए थोड़ी और मेहनत करके गंध से बावस्ता कोई अलग कहानी चुन लेना ज्यादा उपयुक्त होता…। मंटो की एक चर्चित कहानी (शायद ‘बू’) याद आ रही। ख़ैर, यदि यह पहला प्रयास है, तो आगे के लिए कुछ विविधता वाला बेहतर सोचा जा सकता है, क्योंकि कहानी या नाटकेतर गद्य पर बने नाटकों के लिए यह ज़मीन बड़ी उर्वर है और यदि इसे शिर्के साहब ने तोड़ा है, तो इस सोच के लिए वे साधुवाद के हक़दार हैं।

एक बात और – उत्सव के नाटक ‘डार्लिंग, अपनी बात ही कुछ और है’ से मिलते-जुलते खुले दृश्य इसमें भी हैं। यूँ यहाँ करतब वाले पहनावे की संगति है, पर ‘कारन ते कारज कठिन’ के मद्दे नज़र कसे हुए पूरी बाँह व भर पाँव के पहनावे पर भी तो सोचा जा सकता था…। याने इससे बचना रंगकर्म के लिए ज्यादा मुफ़ीद होगा – बनिस्पत सस्ती पसंदगी वाले उसके इस्तेमाल के। फिर दोनो में कलाकार वृंदा ठाकुर ही हैं और मुझे डर लग रहा है कि थिएटर में ये ऐसी भूमिकाओं के लिए कहीं टाइप्ट न हो जायें…!! बहराहल,
उत्सव की ये शामें बड़ी व्यस्त-मस्त बीतें – कई पुराने लोगो के ‘दरस-परस हुए, कुछ नयों से भेंट हुई, जिसमें ये मध्यप्रदेशीय रंगकर्मी सबसे प्रमुख हैं। इन्हें और इनके कामों को पहली बार देखने का अवसर मिला, जिससे हम काफ़ी समृद्ध हुए…। इस सब कुछ के लिए मुम्बई के रंग़-परिवार की तरफ़ से जयंत देशमुख का इस्तक़बाल…! अब अगले साल का इंतज़ार रहेगा…।