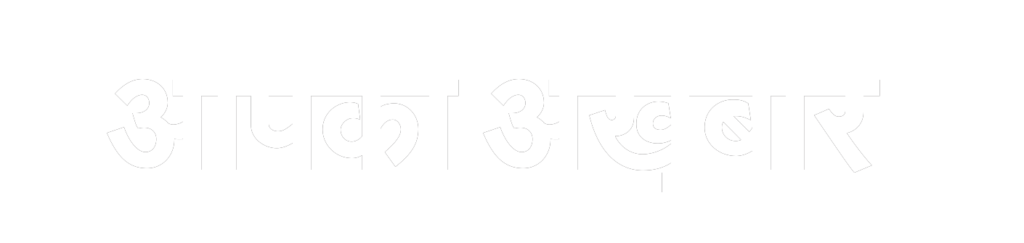डॉ. निवेदिता शर्मा।
डॉ. निवेदिता शर्मा। भारत एक ओर डिजिटल क्रांति, बुलेट ट्रेन और अंतरिक्ष अभियानों को लेकर उत्साहित है, वहीं दूसरी ओर कुपोषण जैसी बुनियादी सामाजिक समस्या अभी भी उसे चिंता में डाले हुए है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए पोषण ट्रैकर के ताज़ा आंकड़े यही दिखाते हैं कि आज भी देश का एक बड़ा हिस्सा पर्याप्त पोषण से वंचित है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि देश के 63 जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित पाए गए हैं।
 यह एक सच्चाई है कि वर्तमान में देश के 199 जिलों में कुपोषण का स्तर 30 से 40 प्रतिशत के बीच है। कुछ जिलों में यह आंकड़ा कहीं अधिक है। महाराष्ट्र का नंदुरबार (68.12%), झारखंड का पश्चिम सिंहभूम (66.27%), उत्तर प्रदेश का चित्रकूट (59.48%), और मध्य प्रदेश का शिवपुरी (58.20%) इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की दर 37.07 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि 0 से 6 वर्ष के 8.19 करोड़ बच्चों में से 35.91 प्रतिशत कुपोषित हैं।
यह एक सच्चाई है कि वर्तमान में देश के 199 जिलों में कुपोषण का स्तर 30 से 40 प्रतिशत के बीच है। कुछ जिलों में यह आंकड़ा कहीं अधिक है। महाराष्ट्र का नंदुरबार (68.12%), झारखंड का पश्चिम सिंहभूम (66.27%), उत्तर प्रदेश का चित्रकूट (59.48%), और मध्य प्रदेश का शिवपुरी (58.20%) इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की दर 37.07 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि 0 से 6 वर्ष के 8.19 करोड़ बच्चों में से 35.91 प्रतिशत कुपोषित हैं।यह आंकड़े केवल रिपोर्ट नहीं हैं, बल्कि उस सामाजिक संकट की सच्ची तस्वीर हैं, जो भविष्य की पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। फिर भी बात यदि समग्रता से देश के सभी राज्यों के बीच मध्य प्रदेश में बाल कुपोषण को दूर करने की होगी तो राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करनी ही होगी। मध्य प्रदेश में बच्चों में कुपोषण की स्थिति बीते दो दशकों में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखी है। वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-3) के अनुसार राज्य में कुपोषण की स्थिति बेहद चिंताजनक थी। उस समय प्रदेश में 60 प्रतिशत बच्चे कम वजन, 50 प्रतिशत लंबाई के हिसाब से कमजोर, और लगभग 35.4 प्रतिशत बच्चे उम्र के हिसाब से कम वजन वाले थे। इन आंकड़ों ने भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन दोनों के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी की थी।
वर्ष 2015-16 में जब एनएफएचएस-4 आया, तब निश्चित ही इसमें बड़ा सुधार दिखा। कम वजन वाले बच्चों की दर घटकर लगभग 42.5 प्रतिशत रह गई, स्टंटेड 42 प्रतिशत के करीब आ गया और उम्र के हिसाब से कम वजन वाले बच्चे लगभग 25.8 प्रतिशत पर आ पहुंचे थे। इसके बाद वर्ष 2019-21 में एनएफएचएस-5 के आंकड़े आए, जिसमें पाया गया कि कम वजनी बच्चों की दर घटकर 33 प्रतिशत पर आ गई है। उम्र के हिसाब से लम्बाई में कम 35.7 प्रतिशत पर बच्चों का आंकड़ा पहुंचा और आयु अनुसार कम वजनी बच्चे मात्र 19 प्रतिशत ही रहे। इसका सीधा मतलब है कि बीते 16 वर्षों (2005 से 2021) में कम वजनी बच्चों की दर में लगभग 45 प्रतिशत, लम्बाई में 46 पतिशत और आयु के हिसाब से तय वजन में 29 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
इस बीच हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि लगातार प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जहां वर्ष 2005 में छह वर्ष तक के बच्चों की संख्या 10.78 लाख के लगभग संभावित है। वर्ष 2021 में यह संख्या 12.6 लाख के करीब रही और अभी 2025 की स्थिति में यह जनसंख्या 0-6 वर्ष तक की 13.25 लाख बच्चों की है। कहने का अर्थ है कि हर वर्ष बच्चों की संख्या प्रदेश में बढ़ रही है और इसके साथ ही कुपोषण भी समय के साथ कम होता हुआ दिखता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार की ‘सुपोषित मध्य प्रदेश 2030’ नीति के अंतर्गत अब कुपोषण को केवल स्वास्थ्य या महिला-बाल विकास विभाग का विषय न मानते हुए इसे बहुविभागीय जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है। इस नीति के अंतर्गत पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा जैसे विभागों को मिलाकर एकीकृत कार्य योजना पर ज़ोर दिया गया है।
राज्य में तीव्र कुपोषण का एकीकृत प्रबंधन (आईएमएएम) और तीव्र कुपोषण का समुदाय-आधारित प्रबंधन (सीएमएएम) योजनाओं के माध्यम से गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों की पहचान और पुनर्वास का कार्य समुदाय स्तर पर किया जा रहा है। यह मॉडल विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान प्रभावी सिद्ध हुआ, जब स्वास्थ्य ढांचा दबाव में था। अब यह पहल संस्थागत स्वरूप ले चुकी है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को इसमें सक्रिय भूमिका दी जा रही है।
 वर्ष 2025 में आयोजित सातवें पोषण पखवाड़े (8-22 अप्रैल) के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवजी की अध्यक्षता में पहले 1000 दिन, स्वच्छ आहार-स्वस्थ बाल, और सीएमएएम-टीएचआर की दक्षता जैसे विषयों पर प्रदेशव्यापी अभियान चलाए गए। इसके अलावा, ‘ईट राइट स्कूल’ कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को पोषण सुरक्षा, स्वच्छ भोजन और जीवनशैली में सुधार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्कूलों में सेहत क्लब और न्यूट्री गार्डन जैसी पहलें चलाई जा रही हैं।
वर्ष 2025 में आयोजित सातवें पोषण पखवाड़े (8-22 अप्रैल) के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवजी की अध्यक्षता में पहले 1000 दिन, स्वच्छ आहार-स्वस्थ बाल, और सीएमएएम-टीएचआर की दक्षता जैसे विषयों पर प्रदेशव्यापी अभियान चलाए गए। इसके अलावा, ‘ईट राइट स्कूल’ कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को पोषण सुरक्षा, स्वच्छ भोजन और जीवनशैली में सुधार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्कूलों में सेहत क्लब और न्यूट्री गार्डन जैसी पहलें चलाई जा रही हैं।सरकार ने पोषण आहार सुधार की दिशा में भी कदम उठाए हैं। नई रेसिपी में चीनी की मात्रा घटाकर 16 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि दूध पाउडर और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई गई है, जिससे यह आहार 3.5 मिलियन बच्चों तक पहुँच पा रहा है। राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को केवल पोषण वितरण का केंद्र न मानते हुए अब इन्हें सामुदायिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संवेदनशीलता के केंद्रों में बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘Adopt an Anganwadi’ अभियान में सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवी संस्थाएं इन केंद्रों को विकसित करने में भागीदारी निभा रही हैं।
प्रदेश में आज मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुधार के लिए ‘संजीवनी रोडमैप’ लागू किया गया है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को पोषणयुक्त खाद्य सामग्री (दूध, अंकुरित अनाज आदि) वितरित की जा रही है। डिजिटल ट्रैकिंग के लिए ‘पोषण ट्रैकर’ ऐप का उपयोग शुरू कर दिया गया है, जिससे वास्तविक समय पर बच्चों की पोषण स्थिति की निगरानी संभव हो पा रही है। जिला स्तरीय कुपोषण मानचित्र तैयार किए गए हैं और अति-कुपोषित जिलों में विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रदेश में कुपोषण नियंत्रण बजट भी बढ़ाया गया है। देखा जाए तो यह सभी वास्तव में कुपोषण रोकने या कम करने की दिशा में अच्छी पहले हैं।
मप्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में महिला एवं बाल विकास विभाग को ₹27,147 करोड़ का बजट दिया है, जिसमें से पोषण संबंधी योजनाओं के लिए ₹3,729 करोड़ आवंटित किए गए हैं। विशेष पोषण आहार योजनाओं को ₹1,166 करोड़ मिले हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार द्वारा लिए गए इन कदमों से प्रदेश में कुपोषण की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है। अभी 2024-25 के एनएफएचएस-6 आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए हैं, उम्मीद है कि इसमें भी पहले से बेहतर राज्य में बच्चों की स्थिति होगी।
(लेखिका मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हैं)