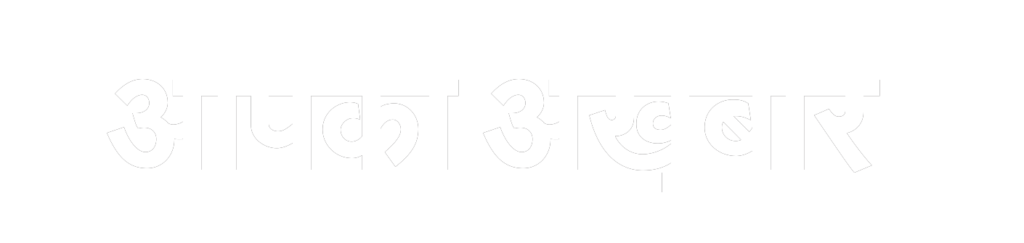धराली के उपजाऊ खेतों में मौत की इबारत किसने लिखी?
 व्योमेश चन्द्र जुगरान
व्योमेश चन्द्र जुगरान भागो-भागो… की आवाजें, सड़क और घरों से निकल जान बचाने को भागते लोग और तूफानी गति से घरों और होटलों को तबाह करता एक राक्षसी गुबार! ऐसे दृश्य हम-आप अमूमन हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में देखते आए हैं। मगर मंगलवार दोपहर करीब एक बजे पूरे देश ने टीवी चैनलों पर उत्तरकाशी जिले के धराली कस्बे पर बरपा कुदरती कहर देखा तो हर कोई सहम गया। उत्तराखंड शासन से लेकर केंद्र सरकार तक हर तरफ कोहराम मच गया। सब कुछ इतना भयावह था कि गंगोत्री धाम से करीब 23 किलोमीटर पहले स्थित एक बेहद खूबसूरत पड़ाव पल भर में खौफ और मौत की इबारत लिखते हुए मटियामेट हो गया।
 लोगों ने इससे पहले 13-14 मई 2013 की केदारनाथ त्रासदी और 7 फरवरी 2021 का चमोली जिले में ऋषिंगंगा और धौली गंगा के अप्रत्याशित सैलाब की दर्दनाक तस्वीरें देखीं थी। सबकुछ बिल्कुल वही था। ऊपरी हिमालय में अतिवृष्टि अथवा बादल फटने से ताल टूट गए और हजारों टन मलबे के साथ आए सैलाब ने नीचे बस्तियों को तहस-नहस कर डाला। केदारनाथ की विनाशलीला में मौतों का सरकारी आंकड़ा ही पांच हजार से ऊपर था। गैरसरकारी स्रोत आज भी दस हजार से अधिक लोगों के मरने की बात कहते हैं। इसी तरह चमोली जिले में ऋषिंगंगा और धौली गंगा पर बरपे कहर में करीब 200 लोग मारे गए जिनमें अधिकांश वहां बन रहे बांध की सुरंग में दफन हो गए।
लोगों ने इससे पहले 13-14 मई 2013 की केदारनाथ त्रासदी और 7 फरवरी 2021 का चमोली जिले में ऋषिंगंगा और धौली गंगा के अप्रत्याशित सैलाब की दर्दनाक तस्वीरें देखीं थी। सबकुछ बिल्कुल वही था। ऊपरी हिमालय में अतिवृष्टि अथवा बादल फटने से ताल टूट गए और हजारों टन मलबे के साथ आए सैलाब ने नीचे बस्तियों को तहस-नहस कर डाला। केदारनाथ की विनाशलीला में मौतों का सरकारी आंकड़ा ही पांच हजार से ऊपर था। गैरसरकारी स्रोत आज भी दस हजार से अधिक लोगों के मरने की बात कहते हैं। इसी तरह चमोली जिले में ऋषिंगंगा और धौली गंगा पर बरपे कहर में करीब 200 लोग मारे गए जिनमें अधिकांश वहां बन रहे बांध की सुरंग में दफन हो गए।वक्त इस बहाने बहुत बेहरम होता है कि घावों को भले भर दे, मगर मौतों को भी भुला देता है। …और यह ‘भूल जाना’ ही धराली जैसे कस्बों के लिए बहुत मंहगा पड़ गया। आज से कई साल पहले जब हम धराली आए थे तो गंगोत्री जाती सड़क के निचले छोर पर गिनती की दुकानें थीं और ऊपरी छोर पर बसा था, हरे-भरे खेतों से घिरा लकड़ी और पत्थर के खूबसूरत स्थापत्य वाले मकानों का यह गांव। तब धराली और आसपास के ऊंचाई वाले गांव जाड़ों में निचली घाटियों में बने अपने शीतकालीन बसेरों (बगडों) में शिफ्ट हो जाते थे। उन्हें इन बसेरों तक पहुंचाने के लिए उत्तरकाशी से आने वाली बस सिर्फ धराली तक का ही फेरा लगाती थी। यात्रा सीजन में हुई कमाई, कृषि उत्पाद और माल-असबाब के साथ गांवों के दर्जनों परिवार नीचे घाटियों में चले आते थे। वहीं हस्तशिल्प का उनका छिटपुट कारोबार और बच्चों का स्कूल हुआ करता था।
मगर आज सारा परिदृश्य बदल चुका है। मौसमी बदलाव के कारण ‘बगड़ों’ में जाने का चलन नहीं रहा। अन्न उपजाने वाले खेत कंक्रीट के बहुमंजिला होटलों और मंहगे होम-स्टे इत्यादि में बदल चुके हैं। धराली एक पर्यटन डेस्टीनेशन बन चुका है और यहां होटलिंग से आजीविका चलाने वाली एक ठीक-ठाक आबादी बस चुकी है। सीजन में यहां 300 से लेकर 400 तक लोग हरदम बने रहते हैं। पास में ही हर्सिल और मुखबा गांव हैं। मुखबा गंगोत्री धाम का शीतकालीन प्रवास है। भागीरथी की यह समूची उपत्यका बेहद खूबसूरत है। इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मुखबा की यात्रा पर आए थे। धराली के फैलाव और बसावट में सबसे बड़ी भूल यह होती रही कि इसके पास बहने वाला खीर गदेरा (छोटी नदी) अतिक्रमण का शिकार होकर निरंतर संकरा होता चला गया है। सालों पहले इसके जलग्रहण क्षेत्र के आसपास गांव के खेत, गौचर भूमि और सिंचाई की कूल इत्यादि थे मगर अब बहुमंजिला होटल/इमारते हैं। लगभग यही स्थिति धराली से तीन किलोमीटर पहले स्थित हरसिल की भी है। वहां भी इस तबाही से नुकसान हुआ है और सेना के एक कैंप के मलबे में दब जाने की खबर है।
 उत्तराखंड में चप्पे-चप्पे पर सड़कों, नदियों और गदेरों के किनारे बसावट के नियम-कायदों का कोई मतलब नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जनहित याचिकाओं में समय-समय पर गाइड लाइन जरूर दी हैं, मगर इन्हें ताक पर रखकर अनाप-शनाप निर्माण तो जैसे पहाड़ों में रिवाज हो चला है। यदि जलवायु परिवर्तन और मौसमी बदलावों के बीच हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी से तालमेल बनाने की बजाय हालात को मनमाने ढंग से रौंदते चले जाएंगे तो निश्चित ही ऊपरी हिमालय में होने वाली हलचलें धराली जैसे मंजर दोहराती रहेंगी। मौसमी बदलावों के कारण ऊपरी हिमालय में ग्लेशियरों के गलन की बढ़ती गति और भूगर्भीय हलचलें बड़े पैमाने पर मलबा जुटा रही हैं। वहां बारिश और हिमस्खलन से अस्थायी झीलें बन रही हैं। बादल फटने और अतिवृष्टि जैसे प्रकोपों के दौरान मौका पाते ही सारा मलबा बाढ़ और भूस्खलन को साथ लेकर कई गुना ताकत से बहकर नीचे तबाही मचा डालता है। धराली की जल प्रलय के पीछे भी विशेषज्ञ यही अनुमान लगा रहे हैं कि पानी का ऐसा रौद्र रूप ऊपर किसी अस्थायी ताल अथवा झील के टूटने से ही संभव है। पुराने समय में लोगों को प्रकृति के साथ रहने और उसका मिजाज समझने का गहरा और व्यावहारिक सलीका आता था। हिमालय मे उच्च पथों पर धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं का उद्देश्य ही यह था कि वहां होने वाली हर हलचल से वाफिक रहें। अब खासकर पहाड़ों में पर्यटन के बढ़ते रुझान ने नए तरह के दबाव पैदा किए हैं। पुरानी परंपराएं और परिपाटियां पर्यटन का आधुनिक चोला ओढ़कर उद्देश्यों से भटक चुकी हैं। बेशक पर्यटन से लोगों की आजीविका के रिश्ते को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर क्या इसे इतनी हद तक छूट दे दी जाए कि आपदा और मनुष्य के बीच बचाव की गुंजाइशें न रहें! भू-गर्भशास्त्री धराली को पहले ही बारूद का ढेर बताते रहे हैं लेकिन इन चेतावनियों को अनसुना कर सरकारें यहां पर्यटन संबंधी व्यापार का सपना संजोती आई हैं।
उत्तराखंड में चप्पे-चप्पे पर सड़कों, नदियों और गदेरों के किनारे बसावट के नियम-कायदों का कोई मतलब नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जनहित याचिकाओं में समय-समय पर गाइड लाइन जरूर दी हैं, मगर इन्हें ताक पर रखकर अनाप-शनाप निर्माण तो जैसे पहाड़ों में रिवाज हो चला है। यदि जलवायु परिवर्तन और मौसमी बदलावों के बीच हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी से तालमेल बनाने की बजाय हालात को मनमाने ढंग से रौंदते चले जाएंगे तो निश्चित ही ऊपरी हिमालय में होने वाली हलचलें धराली जैसे मंजर दोहराती रहेंगी। मौसमी बदलावों के कारण ऊपरी हिमालय में ग्लेशियरों के गलन की बढ़ती गति और भूगर्भीय हलचलें बड़े पैमाने पर मलबा जुटा रही हैं। वहां बारिश और हिमस्खलन से अस्थायी झीलें बन रही हैं। बादल फटने और अतिवृष्टि जैसे प्रकोपों के दौरान मौका पाते ही सारा मलबा बाढ़ और भूस्खलन को साथ लेकर कई गुना ताकत से बहकर नीचे तबाही मचा डालता है। धराली की जल प्रलय के पीछे भी विशेषज्ञ यही अनुमान लगा रहे हैं कि पानी का ऐसा रौद्र रूप ऊपर किसी अस्थायी ताल अथवा झील के टूटने से ही संभव है। पुराने समय में लोगों को प्रकृति के साथ रहने और उसका मिजाज समझने का गहरा और व्यावहारिक सलीका आता था। हिमालय मे उच्च पथों पर धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं का उद्देश्य ही यह था कि वहां होने वाली हर हलचल से वाफिक रहें। अब खासकर पहाड़ों में पर्यटन के बढ़ते रुझान ने नए तरह के दबाव पैदा किए हैं। पुरानी परंपराएं और परिपाटियां पर्यटन का आधुनिक चोला ओढ़कर उद्देश्यों से भटक चुकी हैं। बेशक पर्यटन से लोगों की आजीविका के रिश्ते को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर क्या इसे इतनी हद तक छूट दे दी जाए कि आपदा और मनुष्य के बीच बचाव की गुंजाइशें न रहें! भू-गर्भशास्त्री धराली को पहले ही बारूद का ढेर बताते रहे हैं लेकिन इन चेतावनियों को अनसुना कर सरकारें यहां पर्यटन संबंधी व्यापार का सपना संजोती आई हैं।अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित और अराजक पर्यटन को लेकर यहां तक कह डाला कि सूरते-हाल यही रहा तो हिमाचल देश के नक्शे से मिट जाएगा। अदालत ने वहां आई आपदाओं को कुदरती कोप नहीं, मानवीय कारस्तानी बताया है। सर्वोच्च अदालत 2013 में लगभग यही बातें उत्तराखंड के बारे में भी कह चुकी है। केदारनाथ की विनाशलीला के फौरन बाद 13 अगस्त 2013 को ‘अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाम अनुज जोशी व अन्य’ के केस में फैसला सुनाते हुए जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और जस्टिस दीपक मिश्रा ने उत्तराखंड के सूरत-ए-हाल के लिए जलविद्युत परियोजनाओं को जिम्मेदार ठहराया था जो कि अदालत के ही शब्दों मे ‘बगैर किसी ठोस अध्ययन के आनन-फानन मंजूर की जा रही हैं।‘
हमने देखा था कि केदारनाथ की त्रासदी पर पूरा देश एकजुट दिखा था और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, निजी घराने, समाचार पत्र समूह, न्यास, सामाजिक संगठन और विद्यार्थियों समेत देश का हर तबका तन-मन-धन से सहायता को आगे आया था। तब सरकारें चाहतीं तो सहानुभूति के इस जज्बे को हिमालय और इसके पारिस्थितिक-तंत्र की चिंताओं से जोड़कर देख सकती थीं। हिमालय की हिफाजत से संबंधित सिफारिशों, निर्णयों और नीतियों को अमली जामा पहनाने का इससे सटीक अवसर कोई और नहीं हो सकता था। यह देशभर से मिली सहायता और सहानुभूति का संतोषप्रद विनिमय होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरुआती टेंसुए बहाने के बाद सरकारें न सिर्फ पुराने ढर्रे पर लौट आईं, बल्कि सीमान्त पहाड़ों तक में पूंजीपतियों की घुसपैठ के रास्ते खुलते चले गए। हादसों के बावजूद सरकारें हिमालय की इकोलॉजी के मद्देनजर भू-वैज्ञानिकों की दीर्घकालिक चिन्ताओं से आंखें मूंद लेना चाहती हैं। वे ऊपरी हिमालय में होने वाली हलचलों और इसके खतरों के गहन वैज्ञानिक विश्लेषणों में नहीं जाना चाहतीं। हिमालय के संरक्षण को नियोजन का केंद्र बिन्दु बनाए बिना बात नहीं बनने वाली। धराली इस कड़ी में एक और नसीहत है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)