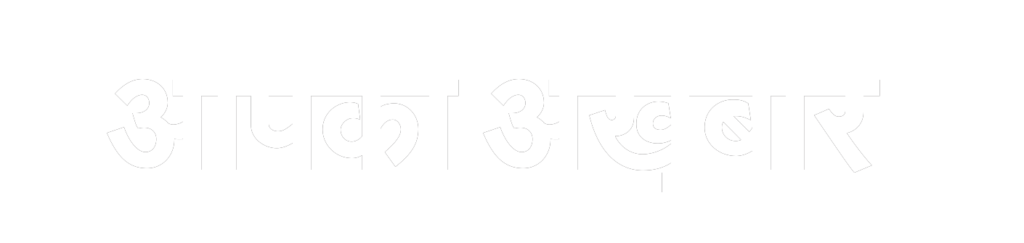अशोक झा।
अशोक झा।
कोलकाता की तरह दरभंगा का भी अपना कुमार या कुमोरटुली या कुम्हार टोली है। पर यह साम्य बस यहीं आकर समाप्त हो जाता है। लेकिन यह भी कम नहीं है। इसके बावजूद कि दोनों का raison d’être अलग अलग है, उद्देश्य एक ही है।
 कोलकाता के कुमोरटुली को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के किनारे पलासी की लड़ाई के बाद अठारहवीं सदी के अंत या उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में गोबिन्दपुर में बसाया था। आज जिस कलकत्ता जो अब कोलकाता है, को हम जानते हैं वह तीन गाँवों गोबिन्दपुर, सुतानुती और कलिकाता को मिलाकर शुरू हुआ था। कुम्हारों के अलावा अंग्रेजों ने तेली, बढ़ई, ग्वालों आदि को भी इस इलाक़े में बसाया था जिनका यहाँ अलग अलग टोली है। कोलकाताके कुमोरटुली की यात्रा एक अलग और बेहद समृद्ध करनेवाला अनुभव देता है। किसी अन्य शिल्प की तुलना में कुम्हारों के शिल्प का महत्व हमारे यहाँ विशिष्ट है क्योंकि मुख्य रूप से मूर्तिपूजा के लिए विख्यात इस देश में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों और मूर्ती पूजा से संबंधित दूसरी सामग्रियों का निर्माण वही करते हैं। वह ज़माना जब कलकत्ता में कुम्हारों और दूसरे शिल्पकारों को बसाया गया, दैनिक जीवन की कई बातों के लिए उन पर निर्भरता आज के मुक़ाबले काफी अधिक थी। स्टील, प्लास्टिक और दूसरे पदार्थों की बनी वस्तुओं के हमारे जीवन में प्रवेश ने कुम्हारों के महत्व को कम किया और उन पर हमारी निर्भरता लगभग ख़त्म कर दी। मिट्टी के बने बर्तनों के चलन से ग़ायब हो जाने के बाद अब सिर्फ कुछ ही बातों के लिए हम उन पर निर्भर हैं और मूर्तियों का निर्माण इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।
कोलकाता के कुमोरटुली को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के किनारे पलासी की लड़ाई के बाद अठारहवीं सदी के अंत या उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में गोबिन्दपुर में बसाया था। आज जिस कलकत्ता जो अब कोलकाता है, को हम जानते हैं वह तीन गाँवों गोबिन्दपुर, सुतानुती और कलिकाता को मिलाकर शुरू हुआ था। कुम्हारों के अलावा अंग्रेजों ने तेली, बढ़ई, ग्वालों आदि को भी इस इलाक़े में बसाया था जिनका यहाँ अलग अलग टोली है। कोलकाताके कुमोरटुली की यात्रा एक अलग और बेहद समृद्ध करनेवाला अनुभव देता है। किसी अन्य शिल्प की तुलना में कुम्हारों के शिल्प का महत्व हमारे यहाँ विशिष्ट है क्योंकि मुख्य रूप से मूर्तिपूजा के लिए विख्यात इस देश में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों और मूर्ती पूजा से संबंधित दूसरी सामग्रियों का निर्माण वही करते हैं। वह ज़माना जब कलकत्ता में कुम्हारों और दूसरे शिल्पकारों को बसाया गया, दैनिक जीवन की कई बातों के लिए उन पर निर्भरता आज के मुक़ाबले काफी अधिक थी। स्टील, प्लास्टिक और दूसरे पदार्थों की बनी वस्तुओं के हमारे जीवन में प्रवेश ने कुम्हारों के महत्व को कम किया और उन पर हमारी निर्भरता लगभग ख़त्म कर दी। मिट्टी के बने बर्तनों के चलन से ग़ायब हो जाने के बाद अब सिर्फ कुछ ही बातों के लिए हम उन पर निर्भर हैं और मूर्तियों का निर्माण इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।
कोलकाता के कुमोरटुली का इतिहास पुराना और व्यवस्थित है। दरभंगा के कुम्हार टोली का इतिहास न तो इतना पुराना है और न इतना व्यवस्थित ही। यह पूछने पर कि आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं, यहाँ के कुछ कारीगरों ने तो अतिरेकों के लिए प्रसिद्ध मैथिलों की विशिष्ट शैली में कहा : “हम सब त’ एहि ठाम पचासो साल स बसल छियैक”। कुछ ने कहा कि पंद्रह-बीस साल से। मैंने किसी और स्रोत से यह जानने की फ़िलहाल कोशिश नहीं की है कि ये कुम्हार लोग यहाँ कब से बसे हैं। इतना तो तय है कि इन्हें यहाँ बसाया नहीं गया है बल्कि बसने दिया गया है। वैसे दरभंगा में जो कुम्हार टोली है, उसको टोली या टोला कहना भी ग़लत होगा। जिसे हम टोला के रूप में जानते हैं वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये यहाँ वैसे ही बसे हैं जैसे घुमंतू जातियाँ सड़क के किनारे बस जाते हैं। पर एक अंतर यह है कि घुमंतू समुदाय, अपने नाम के अनुरूप जहाँ कुछ दिनों के बाद अपना ठिकाना बदल लेते हैं, कुम्हारों की यह टोली काफी सालों से यहाँ बसी है। ये लोग क़ादिराबाद से हसन चौक जो सड़क आती है उसकी बायीं ओर मदरसा से लेकर राज स्कूल तक उस सड़क के किनारे उपलब्ध जगह पर कोई दो-तीन सौ मीटर में फैले हुए हैं। इस सड़क के दूसरी ओर रामबाग की ऊँची दीवार है। इस दीवार की वजह से उस ओर इस टोली का विस्तार नहीं हो सकता इसलिए ये लोग सड़क के बिल्कुल किनारे दूसरी ओर उपलब्ध थोड़ी सी जगह पर सिमटे हुए हैं। कोलकाता के कुमोरटुली में कलाकारों के स्टूडियो भी हैं और इनमें से कुछ लोग वहाँ रहते भी हैं। कुमोरटुली का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। दरभंगा में ये लोग जगह के अभाव के कारण यहाँ सिर्फ़ अपना स्टूडियो खोलकर बैठे हैं जहाँवे मूर्तियां बनाते हैं जबकि ये सब के सब रहते हैं शहर के नज़दीक के दूसरे मुहल्ले में।
 दरभंगा के कुम्हार टोली में कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है। यहाँ के कुम्हार सड़क के दूसरी ओर मिट्टी, पुआल, बाँस के टुकड़े, लकड़ी आदि जिसकी ज़रूरत उन्हें मूर्ति का ढाँचा बनाने में होती है, रखते हैं। इसकी तुलना में कुमोरटुली के कुछ स्टूडियो काफी बड़े हैं। ऐसे ही एक स्टूडियो में कलाकारों को सुमेरु पर्वत लेकर उड़ते हुए हनुमान की विशालकाय मूर्ति बनाते हुए मैंने देखा था। दरभंगा के कुम्हार टोली के लिए कुमोरटुली के इस वैविध्य और विशालता के नज़दीक भी आ पाना अभी संभव नहीं है। हाँ, अगर सरकार उसके लिए वहाँ ज़्यादा जगह उपलब्ध कराए और दूसरी सुविधाएँ दे तो आगे चलकर इस टोली के विस्तार की पूरी संभावना है।
दरभंगा के कुम्हार टोली में कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है। यहाँ के कुम्हार सड़क के दूसरी ओर मिट्टी, पुआल, बाँस के टुकड़े, लकड़ी आदि जिसकी ज़रूरत उन्हें मूर्ति का ढाँचा बनाने में होती है, रखते हैं। इसकी तुलना में कुमोरटुली के कुछ स्टूडियो काफी बड़े हैं। ऐसे ही एक स्टूडियो में कलाकारों को सुमेरु पर्वत लेकर उड़ते हुए हनुमान की विशालकाय मूर्ति बनाते हुए मैंने देखा था। दरभंगा के कुम्हार टोली के लिए कुमोरटुली के इस वैविध्य और विशालता के नज़दीक भी आ पाना अभी संभव नहीं है। हाँ, अगर सरकार उसके लिए वहाँ ज़्यादा जगह उपलब्ध कराए और दूसरी सुविधाएँ दे तो आगे चलकर इस टोली के विस्तार की पूरी संभावना है।
कोलकाता के कुमोरटुली का फलक बहुत व्यापक है। वे बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी पूछ और पहुँच है।कुमोरटुली में काम करनेवाले कई मूर्तिकार अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं। मूर्ति शिल्प में उनकी प्रसिद्धि स्थापित सिद्धहस्त कलाकार की है और उनकी इस पहचान ने उनकी कीर्ति को दूर दूर तक फैलाया है। विशेषकर दुर्गा पूजा में कुमोरटुली के कलाकारों की माँग देश विदेश में होती है।यहाँ लगभग सभी स्टूडीओ के बाहर उसके मूर्तिकारों के नामों की पट्टी और उनके फ़ोन नंबर लिखे मिलते हैं। दरभंगा के कुम्हार टोली के कुम्हार अभी इतने पेशेवर नहीं हुए हैं। वे इतने व्यवस्थित भी नहीं हैं। “हम तो सड़क के किनारे बसे हैं, हमें तो इस जगह से कभी भी सरकार हटा सकती है”, एक कारीगर ने अपना नामबताने से मना करते हुए कहा।
कोलकाता का कुमोरटुली हुगली नदी के बिल्कुल किनारे बसा है और मूर्तिबनाने के लिए जरूरी काली मिट्टी उन्हें इसी हुगली नदी से मिल जाती है। पर दरभंगा के मूर्तिकारों को मुख्य रूप से धोई घाट से मिट्टी लाना होता है जो कुशेश्वर जाने के रास्ते में पड़ता है। यह स्थान उस स्थान से काफी दूर है जहाँ उनका कुम्हार टोली इस समय मौजूद है।
दुर्गा पूजा एक ऐसा समय है जब दरभंगा के मूर्तिकार भी बहुत व्यस्त होते हैं। मिथिला में दुर्गा पूजा की परंपरा काफी पुरानी है। शायद ही ऐसा कोई गाँव होगा जहाँ दुर्गा पूजा नहीं होती है। शहरों में तो एकाधिक स्थानों पर दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है।सो दुर्गा पूजा में मूर्ति बनाने के लिए दरभंगा के कुम्हार टोली के शिल्पियों को बुलाया जाता है। कोलकाता में होनेवाले दुर्गा पूजा का आयाम बहुत व्यापाक होता है और बहुत ही पेशेवर ढंग से इसका आयोजन होता है जिसमें बाज़ार और पूँजी की मुख्य भूमिका होती है। दरभंगा और इसके आसपास के इलाक़े में होनेवाली दुर्गा पूजा के बंगाल की दुर्गा पूजा के समकक्ष आने की बात करना भी कल्पनातीत है।
 एक छोटी मूर्ति पर मिट्टी लगा रही एक महिला से जब मैंने पूछा : अहाँ सभ दुर्गा के बड़का मूर्ति बनबैत छियैक? उनका जवाब था : “बड़का मूर्ति ओहि स्थाने पर बनैत छै। ऑर्डर देबई?”वह बोली कि उसका स्टूडियो जहाँ है उसको दुर्गा पूजा के दौरान बंद कर दिया जाता है इसलिए उसे दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए किसी और स्थान का चयन करना होता है। पर ये लोग दुर्गा की मूर्ति या फिर कोई और बड़ी मूर्ति बनाने के लिए दूसरे गाँव या शहर भी जाते हैं।
एक छोटी मूर्ति पर मिट्टी लगा रही एक महिला से जब मैंने पूछा : अहाँ सभ दुर्गा के बड़का मूर्ति बनबैत छियैक? उनका जवाब था : “बड़का मूर्ति ओहि स्थाने पर बनैत छै। ऑर्डर देबई?”वह बोली कि उसका स्टूडियो जहाँ है उसको दुर्गा पूजा के दौरान बंद कर दिया जाता है इसलिए उसे दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए किसी और स्थान का चयन करना होता है। पर ये लोग दुर्गा की मूर्ति या फिर कोई और बड़ी मूर्ति बनाने के लिए दूसरे गाँव या शहर भी जाते हैं।
कुमोरटुली जब पिछले साल मैं गया था उस समय दुर्गा पूजा को बीते तीन महीने हो गए थे और वहाँ बिल्कुल भी चहल-पहल नहीं थी। बहुत कम कारीगर वहाँ थे और मूर्तियों पर लगभग नहीं के बराबर काम हो रहा था। मैंने किसी महिला को मूर्ति बनाने या इससे जुड़ी किसी और काम में हाथ बँटाते नहीं देखा। पर ऐसा नहीं है कि महिलाएँ वहाँ मूर्ति बनाने में सहयोग नहीं करतीं। पर दरभंगा में मुझे कई महिलाएँ और लड़कियाँ मूर्ति बनाने के विभिन्न कार्यों में सहयोग करती दिखीं। जगनी कुमारी बीए में पढ़ती है और उसे जब भी समय मिलता है, वह मूर्ति निर्माण में सहयोग करती है। वह उन मूर्तियों पर पेंट स्प्रे कर रही थी जो सूख चुकी थी। यह पूछने पर कि क्या वह सिर्फ इस पारिवारिक कार्य में सहयोग देने के लिए यह काम कर रही है, उसने कहा नहीं, मूर्ति निर्माण में उसकी दिलचस्पी है। क्या यहाँ ऐसी कोई मूर्ति है जिसे उसकी परिकल्पना कहा जाए और जिसे पूरी तरह से उसकी कृति कहा जाए, उसने कहा नहीं, अभी यह काम उसका भाई और घर के दूसरे लोग ही करते हैं। पर जगनी जैसी लड़कियों के इस पेशे में दिलचस्पी लेने का मतलब यह है कि इस पेशे के अच्छे दिन आनेवाले हैं और इसमें बेहतर और अधुनातन तकनीक के भी प्रयोग के अवसर खुलेंगे। दरभंगा के कुम्हार टोली में सिर्फ मूर्तियाँ ही नहीं बनती। वे दैनिक प्रयोग की वस्तुएँ भी बनाते हैं जैसे गुल्लक, मटकूरी, घैल, चिलम आदि।
कोलकाता के कुमोरटुली से इसकी तुलना नहीं की जा सकती पर कुमोरटुली जाकर जो दृश्य आपको घेरता है लगभग वैसा ही कुछ आपके साथ यहाँ भी होता है जब आप हसन चौक से क़ादिराबाद की ओर जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ते हैं। पेशेवर तौर तरीक़े, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग और पढ़े-लिखे युवाओं के इस परंपरागत शिल्प में दिलचस्पी से दरभंगा का कुम्हार टोली भी निस्संदेह अपनी अलग पहचान बना लेगा।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)