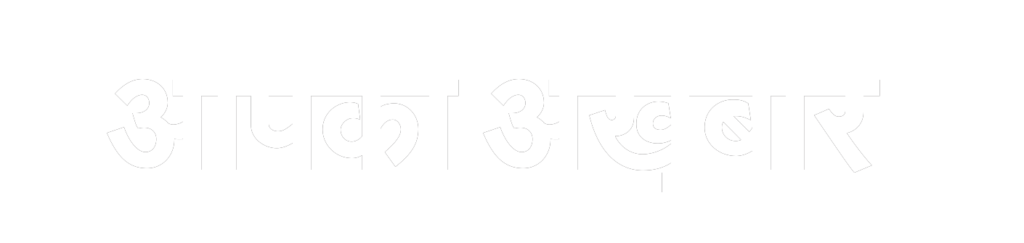बड़के बाबू: मेरे जीवन के बुनियादी निर्माता।
 सत्यदेव त्रिपाठी।
सत्यदेव त्रिपाठी।
इस प्रकार मेरे जीवन के बुनियादी निर्माता मेरे यही बड़के बाबू हैं। वे स्वयं प्राइमरी पाठशाला में प्रख्यात मुख्याध्यापक थे और संस्कृत के दबंग विद्वान। ‘प्रकांड विद्वान’ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी संस्कृत की पढ़ाई तो मध्यमा (इंटरमीडिएट के समकक्ष) तक ही हुई थी, पर शास्त्रार्थ में वे शास्त्री तो क्या, आचार्य की उपाधि वालों से भी भिड़ जाते थे और अपनी बुलंद आवाज़ व वक्त्तृत्व-कौशल से श्रोताओं के लेखे उन पर भारी पड़ते।
एक बार की तो ऐसी याद है कि ये हाथी पर थे और उधर द्वारपूजा पर अपनी तरफ़ का पंडित कमजोर पड़ रहा था। बस, बड़के बाबू ने पिलवान से चिल्लाकर कहा- हाथी को बिठाओ। और हाथी पूरा बैठा भी नहीं कि एकदम गोरे बदन वाले ये बड़के बाबू कंधे पर साफ़ा, बदन पर सिल्क का कुर्त्ता व फर्राटेदार धोती पर म्हरून रंग़ के पम्प जूते पहने ही कूद पड़े और भागते हुए द्वारपूजा-स्थल पर पहुँच के शास्त्रार्थ में दहाड़ने लगे।
इतना ही नहीं, वे क़ानून के दांव-पेंच भी बड़ा अच्छा जानते थे, जिसके चलते वे अपने सारे मुक़दमे जीत जाते, जो किसी से भी तनाजो आदि के कारण उन पर दायर होते या वे किसी पर दायर करते। इस पक्ष पर उनके व्यावहारिक ज्ञान का फ़ायदा एक बार मुझे भी मिला था, जब मेरे कारबारदारी काका मर गये और दसवीं में पढ़ते हुए मुझे घर की सारी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ी, तो चकबंदी में पता चला कि पितादि ने बिजौली गाँव के ज़मींदार संतन-संतोषी साहु से कुछ ज़मीनें ख़रीदी थीं, जिसमें एक गाटा मतरूक हो (पड़ताल में लेखपाल से छूट) जाने के कारण ग्राम समाज में चला गया था और मैंने अपने नाम की इंदराजी (नाम जोड़ने) का मुक़दमा दायर किया था। अब एक प्रमाण उस ज़मींदार की रसीद भी हो सकती थी, जो काकादि से खो-खा गयी थी। इस बड़के बाबू ने सुना, तो बताया कि उस ज़मींदार के वारिसों को कुछ लेके-देके पुरानी तारीख़ में मुसन्ना (रसीद) बनवा लो। उन साहुओं का दामाद मारकंडेय साहु वारिस था। उससे मैंने बनवा लिया। लेकिन वह काग़ज़ बड़ा ताज़ा लग रहा था। बड़के बाबू को मैंने अपनी शंका बतायी। उन्होंने कहा– जहां खाना बनता है, वहीं चूल्ह के ऊपर एक काँटी (खीला) गाड़ के इसे लटका दो। दो-चार दिन में धुँअठ के (धुआँ खाके) पुराना लगने लगेगा। वही किया और युक्ति काम कर गयी। इतने हरफ़नमौला बड़के बाबू के बारे में सोचकर आज लगता है कि अपने समय से पचासों साल आगे की सोचते थे। खेद है कि बहुत दिन उनके साथ रहने का मौक़ा न मिला, वरना काफ़ी कुछ सीखा जा सकता था।
उनकी चिरसंगिनी थीं– हमारी बड़की माई। हमारे यहाँ माइयों-दादियों के नाम नहीं होते– वे माई-दादी ही होती हैं। तो बड़की माई बड़ी सीधी, बड़ी स्नेहल। वही खाने-वाने के लिए बुलाके घर में ले जातीं। उनसे कुछ लम्बी बात सुनने का एक ही मौक़ा याद आ रहा है, जब वे बड़के बाबू के साथ तीर्थयात्रा से आयी थीं। और यात्रा का वह वृत्तांत बताया, जिसमें किसी स्टेशन पर बड़के बाबू गाड़ी में चढ़ गये थे और वे छूट गयीं थीं– ‘हड़बड़ी त ई हमेसे के हउएं। गाड़ी अवते ‘चढ़ो-चढ़ो’ कइके न जनी कब, कवने डिब्बा में घुस गइने– हम देखी ना पवली। गाड़ी चल गइल। अब बचवा, हम हैरान। भित्तर दुगदुगी- कि का होई! बकिन बहरे से एकदम सांत बैठल रहली कि ना पैहें, त अइबे करिहें’। ऐसा विश्वास व ऐसी निश्चिंतता उस समय के सम्बंधों का शाश्वत जीवनमूल्य थी– कहने-सुनने की बात नहीं। और बड़की माई ने बताया कि दो घंटे बाद अगले स्टेशन से फिर इस दिशा में आने वाली कोई गाड़ी पकड़ के आये बड़के बाबू।
भूपालपुर की यजमानी बहुत बड़ी थी और रामबिलास बाबूजी के अलावा कोई करने वाला न था। यूँ तो उस घर में तीन खूँटें थीं, जिनके वंशज आज भी हैं। लेकिन मेरे सामने उस पीढ़ी के अकेले बचे थे रामबिलासबाबू और तीनो खूँट अलग-अलग हो गयी थी– यानी चूल्हें अलग हो गयी थीं, घर एक ही था। खाते अलग थे, रहते साथ थे। तब अलगौझा का यही स्वरूप हुआ करता था। दूसरी खूँट में उनके दो भतीजे शुकदेव व सत्यदेव सरकारी नौकरियों में थे। शुकदेवजी दुनिया के सबसे सज्जन इंसानों में एक थे, लेकिन दुनियादारी की उनकी कमी को शायद पूरा करते हुए सत्यदेव भाई ज़रूरत से ज्यादा दुनियादार थे। और घर की दुनिया भी इन्हीं की थी, क्योंकि बड़े भाई तो नि:संतान थे। सत्यदेव का घर का नाम बंगाली हुआ करता था- हम ‘बंगाली भैया’ कहा करते थे। इन्हीं के बड़े बेटे हैं अपने ये एडवोकेट विनोद, जिनके कारण आज मेरा जाना हो रहा। दूसरी खूँट के दो भाइयों में बड़े वाले जगदीश गूँगे-बहरे थे। छोटे वाले हरदीस ने भी ठीक से पढ़ा-लिखा नहीं। घर का भी खुद कुछ खास काम न करते– बस, बड़े भाई से खेती का सारा काम कराते… (जैसा मेरे देखने में आया है)।
इधर रामबिलास बाबू के चार बेटों में सबसे बड़े रामसूरत भइया बीडीओ थे। बहुत कम बोलते। प्राय: पान भरा रहता मुँह में। शफ़्फ़ाक धोती-कुर्त्ता पहने सायकल चलाते हुए वही हमारे यहाँ के आयोजनों में शरीक होने (न्योता-हंकारी करने) भी आते। दूसरे थे राजदेव भाई। फ़ौज में थे। अपने घर भी आयोजनों में ही दिखते। तीसरे गौरीशंकर तब व्यापार-सा कुछ करते थे और बाहर रहते, पर प्राय: घर आते रहते… और घर होते हुए वही निर्द्वंद्व भाव से यजमानी करने भी जाते। वे तब भी सबसे छटपट, बड़े बात्यायी, चलता-पुर्ज़ा यानी हरफ़नमौला थे– आज भी हैं। चौथे उमाशंकर घर रहते– आज भी हैं। उन दिनों सबने मिलके वहाँ की स्थानीय ‘गोसाईं की बाज़ार’ में उमाशंकर के लिए कपड़े की दुकान खुलवायी थी। अभी खुली-खुली ही थी कि उस दुकान पे एक दोपहर हुआ वह भोज भी मुझे याद आ रहा, जिसमें हम दोनो के साथ हरदीस भाई और वहीं पास स्थित गाँव रजमो के हमारे एक और रिश्तेदार सुरेंद्र मिश्र भी शामिल हुए थे। शायद भूपालपुर के मुतालिक वही अंतिम जाना हुआ था मेरा। और समय के इसी मोड़ पर मैं मुम्बई प्रयाण कर गया था।
इस प्रकार उन दिनों दिव्यांग जगदीश को लेकर उस घर में कुल आठ युवा थे और उन्हें छोड़कर तथा आधे समय वाले गौरी भाई को मिलाकर ढाई लोग घर भी रहते थे, लेकिन यजमानी के काम पूरे हो नहीं पाते थे। हरदीस तो कभी चले भी जाते, उमाशंकर भाई तो कभी न जाते। इसलिए तब बड़के बाबू ने मुझसे कहा था– ‘तुम अपने ख़ाली समय में या समय निकाल के आ जाया करो। जितना बन पड़े, पूजा-पाठ कर-करा लिया करो। यजमान का काम भी हो जायेगा और तुम्हारी कुछ आमदनी भी हो जाया करेगी। मुझे पैसों की ज़रूरत भी होती थी और घर की मेरी यजमानी बहुत छोटी और छोटी जाति वालों की थी, जिसमें आमदनी बहुत कम होती थी। यहाँ की यजमानी ठाकुरों की भी थी, तो आमदनी ज़्यादा होती। लिहाज़ा बात काम की थी और मुझे भा भी गयी। सो, अपने घर के खेती-यजमानी के काम निपटाके मैं आ जाता। ख़ाली समय में शाम-सुबह पढ़ने के लिए दो-एक किताबें भी लेते आता। फिर तो दस में पढ़ने (1968) से लेकर मुम्बई-प्रयाण (1971) तक मैं सायकल से जाके आठ-आठ, दस-दस दिन वहाँ रहता और पूजा-पाठ कराके ठीकठाक कमाई करके लौटता, जिससे मुझे घर चलाने में काफ़ी सहूलियत हो जाती।
(लेखक साहित्य, कला एवं संस्कृति से जुड़े विषयों के विशेषज्ञ हैं)