भारतेंदु जयंती (9 सितंबर) पर विशेष।
 सत्यदेव त्रिपाठी।
सत्यदेव त्रिपाठी।
वैसे तो जब १८५७ की क्रांति का बिगुल बजा था, भारतेंदुजी केवल सात साल के थे, परंतु इस घटना के १०-१२ सालों बाद शुरू हुए इनके नियमित लेखन -ख़ास कर नाटकों- को देखें, तो लगता है कि बाबू साहब ने वहीं से शुरू किया, जहां उस आंदोलब को दबा दिया गया था – याने वह क्रांति दबी नहीं, बस स्थानांतरित हो गयी…। नाना फणनवीस, झाँसी की रानी, ताँत्या टोपे…आदि की तलवारें बाबू भारतेंदु एवं उनकी लेखक मंडली के हाथों में कलम बनकर आ गयीं…। प्रमाण है – इनकी वह साफ़गोई, जो सीधे-सीधे कह सकी – ‘भीतर-भीतर सब राज़ चूसै, बाहर से तन-मन-धन मूसै।
ज़ाहिर बातनि में अति तेज। क्यों सखि साजन? नहिं अंग्रेज’!!
या फिर वह भी – ‘आवहु सब मिलि कै रोवहु भाई, हा भारत-दुर्दशा न देखी जाई’
भारतेंदु के बाद ऐसी सीधी आलोचना (साहित्य समाज की आलोचना है -प्रेमचंद) फिर न देखी गयी। अंग्रेजों का नाम लेकर तो सीधे कुछ कहा ही न गया। संकेतों-प्रतीकों का सहारा लिए बिना जागृति की कोई चेतना मुखरित न हो पायी। क्रांतिकारी निराला तक में भी इन्हीं काव्य-आयामों में कविताई अवश्य निखरी, बात भी खिली, पर उस तरह न खुली…, तो व्यापारी आक्रांताओं को न खली…। ठीक ही कहा गया है कि भारतेंदु का मूल मक़सद था – समाज-सत्य को कहना, न कि कलात्मक उत्कर्ष के मानक स्थापित करना। इसी त्वरा में उल्लेख्य है कि आज़ादी की प्रेरणा देने के लिए प्रसादजी को भारतीय अतीत के स्वर्ण-काल में जाना पड़ा। परंतु अंग्रेज-राज को सीधे-सीधे ‘अंधेर नगरी’ तो भारतेंदु ही कह सके। ‘टके सेर भाजी, टके सेर खाजा’ वाली बदमली भरी व्यवस्था दो टूक ढंग से बेपर्द कर सके। ‘भारत-दुर्दशा’ का कारण सत्ता की बदनीयती है’, को बताने में बिना किसी संकोच के और बिना कोई कलात्मक गुर अपनाये भारत दुर्दैव नामक क्रूर-कुटिल सत्ताधारी पात्र के समक्ष कहलवा सके –
‘कौड़ी-कौड़ी को करूँ, मैं सबको मोहताज। भूखे प्राण निकालूँ इनका, तो मैं सच्चा राज’।।
क्या यह शब्दों की तलवार नहीं है? भारतेंदुजी क्यों ऐसा कर सके और प्रसादजी क्यों न कर सके? यहाँ मेरा मंतव्य प्रसादजी को कमतर या भारतेंदुजी को महत्तर बताने का क़तई नहीं है – ऐसा है भी नहीं बिलकुल। बस, विचारणीय यहाँ यह है कि ऐसी बेलाग अभिव्यक्ति की बेख़ौफ़ी भारतेंदुजी में कहाँ से आयी? और फिर परवर्तियों में वह कहाँ चली गयी और क्यों?

मेरा निश्चित कयास है कि यह फ़र्क़ १८५७ के आंदोलन से मिले अहसास का परिणाम है। उस क्रांति ने उस समय को यह हिम्मत दी कि ऐसा जज़्बा, ऐसी बेबाक़ी आ सकी। जब सरे आम लड़ कर दिखाया जा सका, तो कहने की धड़क क्यों न खुले? याने शब्दों की यह तलवार १८५७ ने दी – गोया क्रांतिकारियों की टूटी तलवारें साहित्यकारों के हाथों में कलम बनके आ गयीं। लेकिन फिर बाद में धीरे-धीरे अंग्रेज़ी शासकों का जलजला अपना शिकंजा कसता गया…और फिर सच की बेबाक़ी को कलात्मक आवेष्टन धारण करना पड़ा…। इसी परिवर्तन का परिणाम है – परवर्ती भारतेंदु-युग का लेखन। चूँकि इस चर्चा में नाटकों के संदर्भ में प्रसादजी का नाम सीधे-सीधे आया है, इसलिए यह बात कहे बिना आगे बढ़ना नाइंसाफ़ी होगी कि १९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होते, तो प्रसादजी के लेखन का तेवर भी काफ़ी कुछ भारतेंदु जैसा होता…। और बीसवीं शताब्दी के दूसरे-तीसरे दशक में भारतेंदु हुए होते, तो एक हद तक प्रसादजी जैसे हो सकते थे। और यह असर इस विवेच्य १८५७ का ही होता…। यहाँ एक पुराना दोहा उद्धृत करने की इजाज़त चाहूँगा – ‘पुरुष बली नहिं होत है, समय होत बलवान, भिल्लनि लूटी गोपिका वहि अर्जुन वहि बान’। १८५७ ऐसा ही सिद्ध समय साबित हुआ!! बहरहाल,
यदि १८५७ में भारतीय तलवार जीत गयी होती, तो भारतेंदु-युग का रचनात्मक परिदृश्य कुछ और होता…जीत की ख़ुशियाँ मन रही होतीं, राष्ट्रीय वीरता का जयगान हो रहा होता…लेकिन वह आज़ादी कोरी राजनीतिक आज़ादी होती…। कोरी इसलिए कि समय ने सिद्ध कर दिया है कि जन की व्यापक भागीदारी के बावजूद १९४७ में मिली आज़ादी भी बहुत सारे मायनों में राजनीतिक आज़ादी ही बनकर रह गयी है – फिर वह तो सैनिक क्रांति से मिलती, तो कितनी कोरी होती – प्रायः समूची ही…।
इसलिए मुझे यह कहने के लिए माफ़ किया जाये कि इस दृष्टि से उस आंदोलन का असफल होना अच्छा ही हुआ, वरना हम बहुत कुछ से वंचित रह जाते…शायद नवजागरण ही न आता…। सैनिक-विद्रोह के असफल होने से प्रमुख चेतना यह आयी कि सिर्फ़ सैनिकों और लड़ाइयों से आज़ादी पाने का कयास टूटा, जो लगभग सौ सालों से पूरा देश लगाये बैठा था। इस कयास के बनने में शायद वर्ण-व्यवस्था से बनी उस मानसिकता का भी हाथ रहा हो, जिसके तहत काम करने वालों का निश्चित खाँचा बन गया था – याने कि लड़ने का काम एक विशिष्ट वर्ग (क्षत्रियों से संतरित सैनिकों) का है। इस असफलता के बाद हर काम के लिए खानों में बँटी मानसिकता वाला तिलिस्म भी टूटना शुरू हुआ। जन-जन को जाग्रत करने की सुबुद्ध चेतना पनपी। यही नवजागरण का प्रस्थान बिंदु बना।
वरना इतनी बड़ी क्रांति के फेल हो जाने के बाद सैन्य-शक्ति बढ़ाने (नये सैनिकों की भर्ती एवं कुशल प्रशिक्षण…आदि) के बदले सती-प्रथा, बाल-विवाह…आदि रूढ़ियों को तोड़ने के प्रयत्न एवं स्त्री-शिक्षा… जैसे उपक्रमों का शुरू होना आश्चर्यजनक ही कहा जायेगा…। हम जानते हैं कि मुग़लों के साथ खुली लड़ाई में हम अवश्य हार गये, लेकिन उनके शासन के बावजूद हमारी संस्कृति नहीं हारी। लोक का आँखों देखा एक उदाहरण दूँ …बड़े रईस मुसलमान भी हिंदू घरों में बाहर बैठकर काँच-मिट्टी के फेंके जाने वाले बर्तनों में सहर्ष खाते रहे, लेकिन अपने घर के आयोजनों में भी हिंदू भाइयों को उनकी शर्तों पर खिलाते रहे…। सो, १८५७ की हार के बाद हमारा समाज अपनी इन्हीं अंदरूनी ताक़तों को संजोने-सन्नद्ध करने में लग गया…। इसके तहत तमाम सामाजिक जागृतियों के प्रयत्न उस युग के रहबर बने…, जिनका एकनिष्ठ व केंद्रीय मक़सद था – आज़ादी पाना…याने १८५७ की हार को जीतने की व्यापक तैयारी…। कहना होगा कि नवजागरण की यह मशाल भी १८५७ के आलोक से ही जली…।
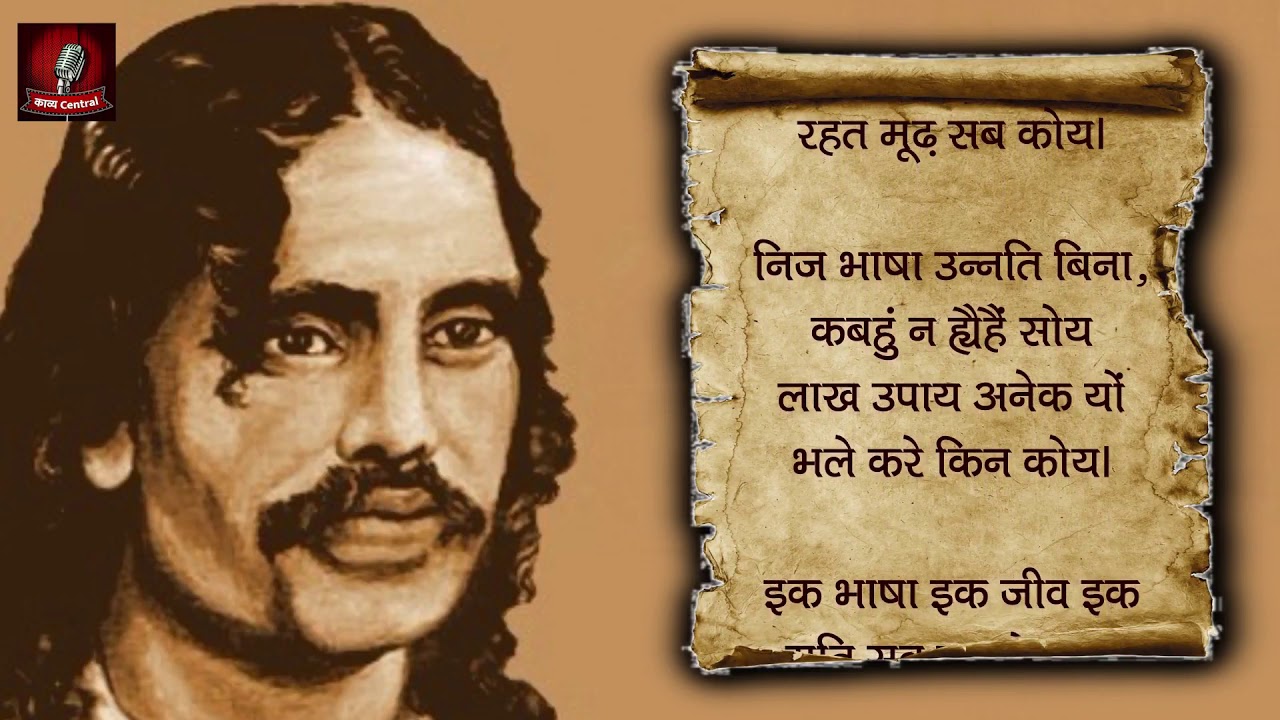
इस प्रकार आज़ादी की इस पहली क्रांति ने बाद के पूरे इतिहास, साहित्य-कला-संस्कृति…आदि को बदला-बनाया है, लेकिन यहाँ हमारा अभिप्रेत है – १८५७ के असर में सत्ता व उसके परिवर्तन की बावत भारतेंदुजी के नाटकों की जानिब से हुए प्रयत्नों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना।
पहले एक बात नाट्य-विधा के बारे में…नाट्य की प्रकृति में ही अन्याय व अत्याचार के प्रति प्रतिरोध का स्वर निहित है। यह है ही कला-समक्षता (एक दूसरे के आमने-सामने बात करने) की, सवाल-जवाब की, एक से दूसरे पात्र या पात्रों की टकराहटों के बीच बनती…स्थापित होती विधा। इसमें अनाचार-अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होती है…और अन्याय-अत्याचार की केंद्र होती हैं सत्ताएँ – राजनीति की, शासन की, संस्कृति की। इसलिए देखा जा सकता है कि औसत रूप से नाटक में साहित्य की अन्य विधाओं एवं कला के इतर रूपों के मुक़ाबले सत्ता के साथ टकराहट का भाव व चेतना अधिक भी होती है और पर्याप्त मुखर व प्रखर भी…। इतिहास गवाह है की जब सत्ता के सन्मुख सवाल उठे हैं, नाटक भी जाग उठा है या फिर नाटकों के साथ सत्ता के खिलाफ सर उठाने का जज़्बा भी जागा है – उसे नया जोश-खरोश भी मिला है। १८५७ के पहले सत्ता के दमन में जो कुछ दबा-टूटा-बिखरा, उसमें नाटक भी था। फिर १८५७ में सबके सर के उठने के साथ नाटक को भी उठना ही था। उस आंदोलन के थमने और विदेशी हुकूमत के पलट कर हावी हो जाने के बाद जब फिर दमन बढ़ा, तब तक भारतेंदुजी का अपने जीवनानुसार अवसान हो चुका था, तो फिर २०-२५ सालों तक नाटकों के अनुवादों के सिवा कुछ ख़ास न हो सका। जो हुआ, वह पारसी थिएटर का उत्कर्ष-चरमोत्कर्ष था…जिससे तो दूर ही रहना था सामाजिक प्रतिबद्धता की चेतना वाले नाटकों को या तो फिर उसका होना ही नहीं पाया।
ध्यातव्य है कि लगभग आधी सदी के इस दौर के बाद १९४० के दशक में नाट्य-चेतना ने फिर करवट बदली और रंग़-चेतना के रूप में उठ खड़ी हुई, जिसे बहुत ठोस रूप में मुम्बई के ‘इप्टा’ और ‘पृथ्वी थिएटर्स’ में देखा जा सकता है। इससे सत्ता की समक्षता में सोच को एक निर्णायक दिशा मिली। इसी ढर्रे पर कह सकते हैं कि भारतेंदुजी ने सिर्फ़ साहित्य ही नहीं रचा, अंग्रेज़ी-सत्ता के समक्ष एक लड़ाई लड़ी, जो नाटकों में सर्वाधिक ज्वलंत बनकर सामने आयी…। इसे इस तरह न देख-समझ पाने वाले वे विचारक बड़े मुग़ालते में रहे, जो सवाल खड़ा करते हैं – “अंग्रेज-सत्ता के दमन एवं भारतीय राज-महाराजाओं के विश्वासघात से १८५७ का उक्त प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, जिसमें नाना फड़ानवीस, रानी लक्ष्मीबाई, अहमद शाह, तात्या टोपे…आदि वीर काम आये। भारतेंदुकालीन साहित्य इस विषय में प्रायः मौन है, जो काफ़ी आश्चर्य की बात है’’। काश ऐसे विद्वान ‘वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति’ का वह संवाद ही पढ़ लेते – ‘महाराज, अंग्रेज सरकार के राज में जो उन लोगों के चित्तानुसार उदारता करता है, उसे ‘स्टार ऑफ़ इंडिया’ की पदवी मिलती है’ तो विश्वासघात पर मौन की बात न करते। और काश, वे यह समझ पाते कि भारतेंदुकालीन साहित्य उसी लड़ाई का विस्तार है। ख़ैर, लड़ाई व टकराहत तथा आत्मावलोकन व आत्मालोचन एवं अंग्रेज़ी सत्ता पर खुले वयंग्य व प्रहार…आदि संदर्भों में भारतेंदुजी के नाटक १८५७ की मशाल साबित होते हैं।
उस मशाल से निकलती लौ अंग्रेज सत्ता को जलाने की चिंगारी छोड़ती है एवं वह मशाल में लगे कपड़े की तरह जलती भी है। और मशाल का डंडा तो नाटक ही है, पर जलाने का काम करने वाला उसमें निहित जो तेल है, वह लोक-प्रहसन, गीत…आदि के मिश्रण से बना है। ये ही उपकरण हैं, जो भारतेंदु द्वारा निर्मित तो हैं ही, इनका वे मनचाहा तथा बेहद कारगर उपयोग भी करते हैं। इस लेखन-प्रक्रिया को हम भारतेंदु नाम्ना इस मशालची के मशाल भांजने की कुशल कला कह सकते हैं, जो हरचंद अंग्रेज़ी हुकूमत से ही मुखातिब होती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इनके हर नाटक में प्रायः एक राजा होता है, जो यूँ तो भारतीय सामंतों का प्रतिरूप होता है, पर उसकी वृत्तियाँ-प्रवृत्तियाँ बिलकुल अंग्रेज़ी सरकार जैसी होती हैं। यही कौशल है कलम का। वह राजा कभी बहुत मूर्ख होता है – कर्त्तव्यहीन, नाकारा, चौपट होता है – जैसे ‘अंधेर नगरी’ का चौपट राजा है – ध्यान रहे कि नगरी चौपट नहीं है – चौपट राजा के कारण नगरी बनी है – अंधेर नगरी…। कभी वह राजा बिलकुल अत्याचारी-अनाचारी होता है। रक्त-रंजित होता है उसका राजभवन – ‘वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति’ की तरह। क्या यह १८५७ का खूनी तांडव ही नहीं है? इस नाटक का सूत्रधार यहीं से शुरुआत ही करता है ‘जो लोग मांस लीला करते हैं, आज उनकी लीला करेंगे’…। और नाटक शुरू होता है, तो लीला होती है – भ्रष्ट राजा, मंत्री व पुरोहित की – याने इनकी बनायी बदमली से भरी व्यवस्था की। नेपथ्य से आवाज़ आती है – ‘बढ़ जाइयो…कोटिन लावा-बटेर के नाशक, वेद धर्म्म प्रकाशक, मंत्र से शुद्ध करके बकरा खाने वाले, दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाने वाले…सहित सकल समाज श्री गृधराज महाराजाधिराज…’ आदि। ऐसा साफ़ कहने वाली कलम भला किस तलवार से कम है? बल्कि तलवार तो सिर्फ़ मार ही करती है, कलम तो मारती है और बताती भी है कि क्यों मार रही है। क्या बताने की ज़रूरत है कि रक्त-लीला करके खून पीने वाले कौन हैं और जिनका रक्त पीते हैं, वे कौन हैं…?
मांस खाने का यदि एक सीधा अर्थ है – हिंसा, तो लक्ष्यार्थ है – धन खाना भी याने यहाँ की दौलत को वहाँ ले जाना, जिसके लिए भारतेंदुजी की सर्वाधिक मशहूर पंक्ति है – ‘पै धन बिदेस चलि जात, इहै अति ख़्वारी’। ध्यान दें कि कभी आगे चलकर दादाभाई नौरोज़ी तथा रजनी पामदत्त ने ‘ड्रेन ऑफ़ वेल्थ’ की बात कही, लेकिन भारतेंदुजी की दूरंदेशी देखें कि इस बात को वे तभी भाँप ही नहीं, अपने तेवर में कई-कई बार कई-कई तरह से कह भी गये थे…जैसे – ‘टके के वास्ते झूठ को सच करे’, चना हाकिम सब जो खाते, दूना टैक्स हज़म कर जाते…और ‘सबके ऊपर टिक्कस (टैक्स) की आफ़त आयी’। इस आर्थिक शोषण को भारतेंदुजी के रचनाकार की दूरदृष्टि वहाँ तक ले जाती है कि किस तरह यह सब कुछ देश की बदहाली का कारक बनता है। ‘भारत-दुर्दशा’ में तो वे अति वृष्टि-अनावृष्टि को भी अत्याचारी सेना का अंग बना देते हैं – गोया प्रतीक रूप में प्राकृतिक आपदाएं भी उन्हीं की करनी हों…।
भारतेंदुजी अपने रचनात्मक मोहरों (राजाओं) की कारस्तानियों के लिए विविध दृश्य भी सिरजते हैं…। ‘वैदिकी हिंसा…’ में एक यमपुरी का दृश्य है, जिसमें राजा की बही देखकर चित्रगुप्त बताता है – ‘महाराज, सुनिए – यह राजा जन्म से ही पाप में लिप्त रहा…। जो जी चाहा, वही किया। लाखों जीवों का इसने नाश किया और हज़ारों घड़े मदिरा के पी गया…। पर आड़ सदा धर्म की रखी। जो कुछ भी किया, एकदम वितंडा कर्मजाल किया’। ‘विषस्य विषमौषधम’ में तो कहते हैं राजा, पर बात खुलकर सीधे-सीधे अंग्रेजों की कर देते हैं – ‘धन्य है ईश्वर, १८९९ में जो लोग सौदागरी करने आये थे, वे आज स्वतंत्र राजाओं को दूध की मक्खी बना देते हैं…’। इस प्रकार १८५७ की क्रांति जिस अंग्रेज़ी सत्ता को तलवार के बल अपदस्थ करना चाह रही थी, उसका ऐसा पराभव करती है नाटककार भारतेंदुजी की कलम – गोया वह तनिक भी तलवार से कम नहीं, वरन ज्यादा है!!
अब एक अलहदा पक्ष की जानिब से देखें…१८५७ यदि सफल हो जाता, तो ऐसे प्रतीक राजाओं की व्यवस्था स्वयं ख़त्म हो जाती, पर इन नाटकों में उस व्यवस्था को भी इस तरह कटघरे में रखा गया है कि स्वयं व्यवस्था त्राहि-त्राहि कर रही है। इसका सबसे तेज व मारक रूप उभरा है – ‘भारत दुर्दशा’ में, जहां एक तरफ़ तो भारत और भारत-भाग्य हैं, तो दूसरी तरफ़ नाकारे शासन का पूरा तंत्र है…। मुखिया है -भारत-दुर्दशा; उसका फ़ौजदार है – सत्यानाशी; रोग, मदिरा, अंधकार, आलस्य,…सब उसके सहायक हैं – सहकर्मी। इन नामों से ही समझ में आ जाता है कि नाटक में क्या कुछ होगा…सब एकदम साफ़, सीधा, खुला। उधर ‘अंधेर नगरी’ का राजकीय महकमा पतन के गर्त में इतना गिर गया है कि बकरी के मरने और आदमी के मरने में कोई फ़र्क़ ही नहीं। प्रशासन से लेकर न्याय-व्यवस्था तक…सब कुछ इतना सड़ गया है कि जब अपराधी की गरदन के लिए फाँसी का फंदा छोटा पड़ गया है, तो ‘मौत के बदले फाँसी’ होनी चाहिए – चाहे जिसकी…के रूप में जड़ता का चरम सामने आता है – जैसे सब के सब काठ के पुतले हों…! और तब महंत की जागरूकता याने लेखकीय दृष्टि आती है – कथन बनकर – ‘ऐसी नगरिया ना रहना’…!!
जिस तरह ‘भारत दुर्दैव’ व उसके साथी मिलकर हर तरह की बदमली चलाते हैं, उसका नाटकीय व किंचित स्थूल आकलन ही पूरा नाटक है। पहले व दूसरे अंक में भारत के विलाप व निर्लज्जता द्वारा भारत की अवमानना होती है। तीसरे अंक में ‘भारत दुर्दैव’ नामक प्रमुख खल पात्र बनकर आता है। भारतेंदु बाबू ने उसका हुलिया बताया है – ‘क्रूर, आधा करिस्तानी, आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिये…फ़ौज के डेरों के सामने आकर नाचते हुए गाता है –
‘उपजा ईश्वर कोप से, आया भारत बीच। छार-खार सब हिंद करूँ, तो उत्तम – नहिं नीच!!
मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे इक राक्षस मानो जी!!
कौड़ी-कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्रान निकालूँ इनका तो मैं सच्चा राज!
मारी बुलाऊँ, देश उजाड़ूँ महँगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊँ दन्न हौ मुझको धन्न
मुझे तुम सहज न जानो जी…आदि-आदि…
यह सब पढ़ते हुए देख-सुन कर क्या नहीं लगता कि ये सब दृश्य १८५७ में हो चुके के नज़ारे के प्रतिरूप हैं? भारत की बर्बादी को लेकर अंग्रेजी राज में कितनी नृशंसता…कितनी बदनीयती भरी है, जिसे पढ़-सुनकर लोगों के आक्रोश फट पड़ें…की परिणति आपोआप निहित है इनमें…!!
उक्त गीतमय बर्बादी की नीयत से वह व्यंग्य करता है – ‘यह कैसे हो सकता है कि अंग्रेज़ी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरें…!! उस भयावह दौर में देश को सुधारने के लिए सचमुच तत्पर कुछ पढ़े-लिखे जागरूक हिंदुस्तानी लोगों के लिए अंग्रेज सरकार का इरादा यह कि – ‘ऐसों के दमन के लिए मैं ज़िले के हाकिमों को कह दूँगा…इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो…। जो जितना बड़ा मेरा मित्र (याने देश का ग़द्दार) हो, उसे उतना बड़ा ख़िताब दो। सत्यानाशी फ़ौजदार कहता है – धर के हम लाखों भेस, किया चौपट यह सारा देस…। वह सेना के अमलों को हुक्म देता है – ‘फ़ौज को आदेश दो कि चारो तरफ़ से हिंदुस्तान को घेर लो’… आदि!! और सारी फ़ौजों से घिरे भारत का वही होता है, जो १८५७ में हुआ था, जिसे सात-आठ सालों के भारतेंदु बाबू ने देखा था…। और जिस तरह फिर से अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई थी, उसी के प्रतीक रूप में चौथे अंक की शुरुआत में एक बड़ी मार्मिक फेंटेसी प्रस्तुत होती है…‘कमरा अंग्रेज़ी ढंग से सजा है। मेज़ कुर्सी लगी है। कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है। नाटक के अंतिम दृश्य में भारत एक पेड़ के रूप में नीचे गिरा है। भारत भाग्य आकर उसे जगाता है। न जगने पर विलाप करता है, जो एक लम्बी कविता में निबद्ध है। इसमें अतीत के भारत व उसके पौरुष का वह अंकन है, जिस पर आगे चलकर प्रसादजी का लगभग पूरा नाटय-संसार रचा गया…। फेंटेसी जारी है…आलाप जैसा लम्बा काव्य-संवाद पूरा होने पर वह पड़े हुए भारत को उठाने की कोशिश करता है। उसके न उठने पर वह जो कहता है, वह एक यथार्थ भी है और एक गम्भीर चेतावनी भी – ‘हाँ, भारतवर्ष को ऐसी मोह-निद्रा ने घेरा है…कि अब उसके उठने की आशा नहीं। और इस ग़म में भारतभाग्य आत्महत्या कर लेता है, पर उसके पहले हर जन्म में भारत जैसे भाई की कामना करता है…।
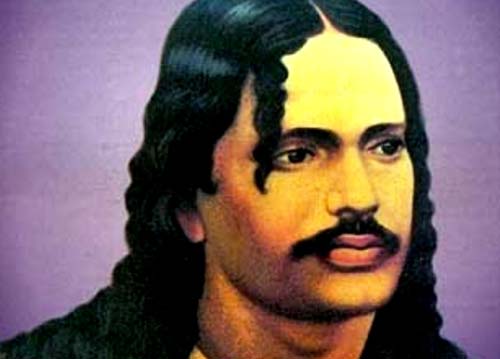
ऐसा ही दूसरे अंक के ‘श्मशान-दृश्य’ में भी आता है – ‘श्मशान…टूटे-फूटे मंदिर…कौए-स्यार-कुत्ते घूमते हुए…इधर-उधर पड़ी हुई अस्थियाँ…’ – गोया १८५७ के बाद का ही मंजर हो…। वहाँ इस हृदय-विदारक स्थिति को प्राप्त देश के प्रति भारतमाता का बेहद करुण व मर्मांतक विलाप नियोजित है –
कोउ नहिं पकरत मेरो हाथ
बीस कोटि सुत अछत, फिरत मैं हा-हा होय अनाथ…
तो यह है भारतेंदुजी की देश-चिंता, देश के प्रति उनकी अगाध संवेदना, सरोकार एवं देश-भक्ति…।
ख़ैर, यही दीन पुकार ‘भारत जननी’ में आकर हथियारबंद क्रांति का आवाहन बन जाती है –
उठौ उठौ सब कमरनि बाँधौ, सस्त्रन सान धरौ री। विजय निसान बजाइ बावरे आगेइ पाँव धरौ री…
कफ़न बांधु, कर में की सब रे चूरी डारहु तोरी…मचा बहु गहिरी होरी…।
फिर तो भारतेंदु बाबू इसी क्रांति को ‘नीलदेवी’ नाटक में ‘बीस कोटि सुत’ बना देते हैं और उक्त ‘शोक का उत्तर अश्रु-धारा से न देकर कृपाण-धारा से देंगे’ के रूप में सशस्त्र क्रांति की खुली चेतना जगाते हैं…। इतना ही नहीं, एक पागल के ज़रिए कुछ गुप्त दल बनाने का आइडिया भी देते हैं – ‘मार मार मार, मिल-मिल, छिप-छिप, खक-खुल…मार-मार…!
यह सब १८५७ का जवाब भी है, विस्तार भी है तथा उसके दमन का प्रतिकार भी है…।
और इन नाटकों के लिखे जाने तक कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी…। १८५७ में पराजित पराजित देश के पास कोई नेतृत्त्व नहीं था। जनता पूरी तरह से निराशा का शिकार तो नहीं हुई थी, पर स्वाभाविक ही था कि एक ग्लानि व अवसाद तथा किंकर्तव्यविमूढ़ता तारी हो गयी थी। ऐसे में भारतेंदुजी ने अपनी लेखनी के माध्यम से एक सक्षम नेतृत्त्व दिया। मैं पुनः कहूंगा कि तलवार का काम किया लेखनी से। विचार दिया कि एक हार के बावजूद अंग्रेजी सत्ता अपराजेय नहीं है। उससे लड़ा जा सकता है। उक्त सारे दृश्य ऐसी वैचारिकता के स्वर हैं। इन वीरताओं के साथ उस बौद्धिकता की ज़रूरत का भी भारतेंदुजी ने स्थापन किया, जो ‘अंधेर नगरी’ के महंतजी में है। असल में चौपट राजाओं की अंधेर नगरियों में अक्लमंदियों से ही कुछ कारगर किया जा सकता है। यहां मैं छूट लेकर कहूँ कि १८५७ की क्रांति में इस बौद्धिक कौशल, सधी रणनीति… आदि के किंचित् या काफ़ी अभाव भी उसकी असफलता के कारण थे। उसमें जितना जुनून था, उतनी योजनाबद्ध नीति न थी। वह आवेश में समय से पहले शुरू भी हो गया था और इसी के चलते सही संचालन के अभाव में काफ़ी बिखर भी गया था। शायद महंत के माध्यम से भारतेंदुजी इस कमी की भी पूर्ति का प्रयत्न कर रहे थे…।
तभी महंत ने ऐसी योजना बनायी कि चेले गोबर्धनदास को तो बचा ही लिया, चौपट राजा का अंत भी कर दिया। उसकी एक चाल के समक्ष अंधेर नगरी की पूरी अंधी व्यवस्था अपने खात्मे के लिए स्वतः तैयार गयी। और अंत में अपनी फांसी का वरण राजा खुद ही करता है। इस तरह उस व्यवस्था का अंत होता है, जो १८५७ के बाद देश में फिर से जम रही थी। ‘भारतजननी’ में लड़ाई के आह्वान, ‘नीलदेवी’ में उसके स्वीकार के साथ इस कूटनीतिक सोच को मिलाकर भारतेंदुजी के नाटकों में एक पूरी विचारसरणि बनती है, जिसका प्रेरक और नियामक भी १८५७ ही है। यहां लंबी चर्चा ‘भारतदुर्दशा’ की हुई, क्योंकि १८५७ के असर का सबसे सशक्त कच्चा चिट्ठा उसमें ही है। उसमें ऐसे सधे दृश्य व संवाद हैं, जिनका सूझबूझ के साथ रूपांतरण कर दिया जाये, तो वह आज के लिए भी प्रासंगिक हो जायेगा। उसमें लेखक का अंतस् पूरी संवेदना व कोफ्त के साथ फट पड़ा है।
भारतेंदुजी के सभी नाटकों में १८५७ के परिणामस्वरूप आते नवजागरण के विकासात्मक कार्यों का भी एक पहलू है, जो समानांतर रूप से नियोजित है। जिसमें थसमसायी जनता की काहिली, नशाखोरी, बेपरवाही, पुरोहितों के पाखंड, सामाजिक रूढ़ियों की जकडबंदी, अपने फायदे के लिए देश के साथ विश्वासघात, अंग्रेज सत्ता के सामने चापलूसी की वृति…आदि की आलोचना व मखौल भी बड़े सटीक ढंग से शामिल है। शिक्षा व स्त्री शिक्षा की जरूरत, विधवा-विवाह जैसी आधुनिक चेतना की आवश्यकता… आदि भी बड़े करीने से समाविष्ट हैं…। और ये सब १८५७ के परिणाम के तोड़ के रूप में नियोजित हैं। विस्तार-भय से इन सबका विस्तृत विवेचन यहां न हो पाने का खेद है, पर यह कहना चाहूंगा कि जिसे मात्र ३५ साल की कुल उम्र मिली, उस बाबू भारतेंदु के जाने के ६०-६५ सालों बाद जो आजादी हमें मिली, उसकी आकांक्षा भारतीय जनता की आंखों में भी उन्होंने ही जगायी थी – एक अदद राष्ट्र की आकांक्षा। ‘अपने मंडल व देश के एक स्वतंत्र सांस्कृतिक व्यक्तित्त्व की खोज’ की चेतना भी उन्हीं की ही जगायी हुई है और इन सबके लिए देश सदा उनका ऋणी रहेगा….!!



