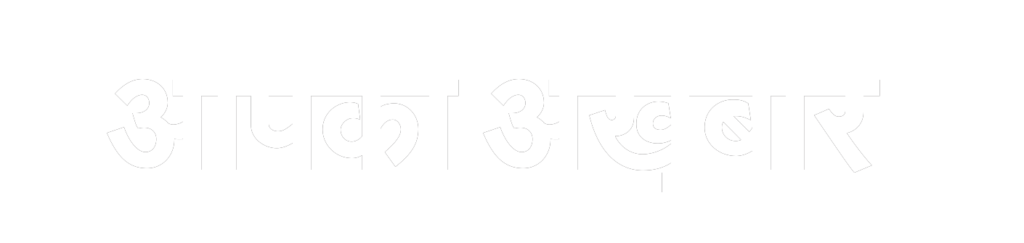पहाड़ पर आए दिन होने वाले हादसों को आपदा कहना बेमानी।
 व्योमेश चन्द्र जुगरान।
व्योमेश चन्द्र जुगरान।पहाड़ के एक दिवंगत कवि उमाशंकर बडूनी के काव्य ‘गंगावतरण’ की कुछ पंक्तियां पेश हैं। इनमें पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री गंगा को तपस्वी भगीरथ के साथ विदा करते हुए वियोग में व्याकुल है-
“सिंधु से मेघ जब-जब उठें, मानसूनी हवाएं चलें/ उनके द्वारा मेरी नंदिनी तेरे रैबार मुझको मिलें/ मेरे हिमनद पिघल जाएंगे, तुझसे मिलने चले आएंगे/ तेरा संदेश लेकर शुभे, मेघ अलका में छा जाएंगे।”
खास बात यह है कि कवि ने हिमालय के इस मर्म को मॉनसूनी चक्र की पूरी वैज्ञानिक व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया है। समु्द्र से बादलों के रूप में उमड़ती घटा को देख पर्वतराज हिमालय पृथ्वी पर अपनी पुत्री की सलामती के प्रति आश्वस्त है। साथ ही, ग्लेशियरों से बहकर पुत्री तक पहुंचने वाला नीर पुत्री को पिता की कुशलक्षेम का संदेश दे रहा है। समुद्र, हिम शिखर, हिमनद, आकाश, बादल, और जल के बीच कायम एक संतुलन को बड़े ही खूबसूरत अंतर्संबंध से जोड़कर कवि ने बेहतरीन संदेश दिया है। लेकिन प्रकारांतर से इसमें यह चेतावनी भी है कि इस प्राकृतिक संतुलन के गड़बड़ाने का अर्थ है, एक खतरनाक परिवर्तन जिसके संदेश मानव जाति के लिए भारी अनिष्टकारी हैं।
आफत बनकर बरसी बारिश
इन दिनों पहाड़ों, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर आफत बनकर बरसी बारिश और इसके कारण हुआ जानमाल का नुकसान आशंकित अनिष्टों की एक झलक मात्र है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में बीते रविवार से सोमवार के बीच 24 घंटे में ही 52.9 मिमी पानी बरसा जबकि इस मौसम में यहां आमतौर पर कुल 14.2 मिमी बारिश हुआ करती थी। इसी तरह हिमाचल के मामले में 24 घंटे का यह आंकड़ा 50.3 मिमी है जो कि सामान्य से पांच गुना अधिक है। हिमाचल और उत्तराखंड में अब तक 58 लोगों की मौत हुई है। इनमें अकेले हिमाचल में ही 52 जानें गई हैं और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई है। गढ़वाल में रुद्रप्रयाग के निकट भूस्खलन में एक वाहन के मलबे में दबने का समाचार है, जिसमें पांच सवारियों की मौत हो गई। पीपलकोटी में भी कई वाहनों के मलबे में दबने और बहने की सूचना है।
इसके अलावा इन राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनेक जगह भारी टूट-फूट हुई है। ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे का एक बड़ा हिस्सा तो तोताघाटी के निकट बिल्कुल सफाचट हो गया। दिल्ली-कोटद्वार-पौड़ी राजमार्ग दुगड्डा के पास और दिल्ली-देहरादून राजमार्ग डाटकाली मंदिर के निकट बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। निर्माणाधीन ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन की एक सुरंग में चार फीट तक पानी भर जाने से वहां काम रहे दर्जनों मजदूरों की जान पर बन आई। गनीमत है कि एनडीआरएफ और अन्य बचाव कर्मियों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। पहाड़ों में जगह-जगह इमारतें जमींदोज हुई हैं और बड़ी संख्या में वाहन बहे हैं।

अराजक निर्माण और प्राकृतिक असंतुलन
पर, सवाल वहीं का वहीं है। आखिर क्यों पहाड़ों पर अराजक निर्माण और प्राकृतिक असंतुलन की अनदेखी के खतरे हमें बार-बार आगाह कर रहे हैं ! नसीहतों को लेकर हमें लकवा क्यों मार गया है ! हम चेतते क्यों नहीं ! जून 2013 में केदारनाथ की विनाशलीला के बाद यदि हम अतिक्रमण से आक्रांत नदियों, नाजुक घाटियों, जंगलों और संवेदनशील धार्मिक स्थलों के लिए कारगर सुरक्षा कवच तैयार कर पाते तो शायद आठ साल बाद फरवरी 2021 में रैणी घाटी फिर से न कांपी होती। इन आपदाओं के बावजूद हम हिमालय के अवैध शोषण और लूट-खसोट के खिलाफ सख्ती का कोई माहौल नहीं बना सके। जबकि हिमालय की हिफाजत से संबंधित जिन सिफारिशों, निर्णयों और नीतियों को अमली जामा पहनाने से सरकारें किसी न किसी कारण से हिचकती रही हैं, आपदाएं हमें उन्हें लागू करने का अवसर देती आई हैं।
केदार की त्रासदी पर तो पूरा देश रोया था और हर कोई एकजुट होकर मदद को सामने आया था। आपदा में मारे गए दस हजार से अधिक लोग (सरकारी आंकड़ा छह हजार कुछ) देश के कोने-कोने से आए तीर्थयात्री थे, इसलिए भी उत्तराखंड के प्रति सहानुभूति का ज्वार संवेदना के स्वाभाविक प्रस्फुटन से कहीं अधिक था। सरकारें चाहतीं तो संवेदनशील चोटियों और हिमनदों के अध्ययन के हवाले से कई ऐसी स्थापनाओं को जन्म दे सकती थीं जो इस क्षेत्र की दीर्घकालीन हिफाजत के लिए कारगर सिद्ध होतीं। यह देशभर से मिली सहायता और सहानुभूति का संतोषप्रद विनिमय होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारें जल्द ही सब कुछ भुलाकर पुराने ढर्रे पर लौट आईं।
कथित बुद्धिजीवियों की खामोशी

पर, अकेले सरकारों को क्यों दोष दिया जाए! आज स्थिति यह है कि उत्तराखंड सरकार ने बदरीनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव जोशीमठ में कुछ समय पूर्व हुए भू-धंसाव के मद्देनजर यदि यात्रियों की संख्या को सीमित रूप से आगे भेजने की बातें कीं तो स्थानीय कारोबारियों सहित तीर्थस्थलों के पंडे-पुजारी ही विरोध में उतर आए और सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। जरा याद करें, जब दिसंबर-जनवरी माह में जोशीमठ के धंसने की खबरें आई थीं तो पूरे देश में कैसा हड़कंप मचा था। हमारा प्रश्न है कि जब से यात्रा सीजन शुरू हुआ है, तब से जोशीमठ के लोग और यहां चिल्लपौं मचाने वाले कथित बुद्धिजीवी क्यों खामोश हैं ! वे तो हेलंग बाईपास जो कि सुरक्षा और समय दोनों के लिहाज से आम तीर्थयात्री के हित में है, उसका भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जाहिर है, यात्रा सीजन के दौरान होने वाली कमाई से समझौता करने को कोई तैयार नहीं है, भले ही इलाके की भूगर्मीय स्थिति कितनी भी कमजोर क्यों न हो।
पहले भी तो खूब बरसते थे मेघ
बारिशें पहले भी हुआ करती थीं। कई दिनों तक अनवरत चला करती थीं। सावन के महीने सूरज के दर्शन मुश्किल हो पाते थे लेकिन बच्चे हंसी-खुशी स्कूल कॉलेज जाते थे। छाते और बरसातियों को ओढ़ना बहुत भाता था। भुट्टे, आम का स्वाद और रास्ते में पड़ने वाले सुनसान बागीचों में ढेला चलाकर पके-अधपके सेव-नाशपाती को जमीन पर गिराकर जेबे भर लेने वाली वे बरसातें तो कब की गुम हो गईं।

हां, तब दूर-दराज के इलाकों में कच्ची सड़कों का अवरुद्ध होना सामान्य बात थी। लेकिन चूंकि इनके आसपास मानवीय हस्तक्षेप/अतिक्रमण का ऐसा दस्तूर नहीं था, सो नुकसान नहीं होता था। अलबत्ता बादल फटने और अतिवृष्टि की इक्का-दुक्का घटनाओं में जान-माल के नुकसान को जनता और प्रशासन दोनों की ओर से बहुत गंभीरता से लिया जाता था। चारधाम यात्रा भी बरसात में स्वाभाविक रूप से मंद पड़ जाती थी। तब श्रद्धालुओं और सैलानियों का ऐसा रैला नहीं था और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा इत्यादि राज्यों से आए यात्रीगण अपने-अपने समूहों के साथ बरसात में आगे बढ़ने की बजाय धर्मशालाओं और बस स्टेशनों के शेड के नीचे रुककर अस्थायी डेरा बना लिया करते करते थे। तब नीतियों में तीर्थाटन को पर्यटन मानने की जिद शामिल नहीं थी और सरकारें इन संवेदनशील तीर्थस्थलों पर उमड़ रही भक्तों की भीड़ को पर्यटन क्रांति से जोड़कर देखने को लालायित नहीं थीं।
मलबे का डंपिंग जोन
यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि बड़े निर्माणों के कारण नदियों के जलागम क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं और नदी-घाटियां मलबे का डंपिंग जोन बनती जा रही है। इसे लेकर न तो सरकारें चिंतित दिखती हैं और न योजनाकारों के पास कोई ठोस डाटाबेस है। इकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि पहाड़ों में पनबिजली परियोजनाओं के कारण नदी तटों की ऊंचाई बढ़ी हैं। बड़ी-छोटी और बरसाती नदियों के मुहाने तो कब के गुम होकर बड़े-बड़े अतिक्रमणों में बदल गए है। देहरादून-टिहरी बार्डर पर रविवार को ताश के पत्तो की तरह ढही प्राइवेट इमारत नदी के कैचमेंट के ऊपर खड़ी थी। यहां बच्चे डिफेंस की कोचिंग लेते थे। खैर मनाइए कि 85 बच्चों को एक दिन पूर्व ही यहां से हटा दिया गया था।
हमने ऊपर उल्लिखित कविता के माध्यम से जिस संतुलन की बात की है, उसके गडबड़ाने के अंदेशा है। हिमालयी क्षेत्र को लेकर ऐसे शोध सामने आ रहे हैं जिनमें पहाड़ों में तापमान बढ़ने की गति को वैश्विक गति के बराबर आंका जा रहा है। इन शोधों में स्थिति को तब और गंभीर माना गया है, जब लोग ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के प्रति उदासीन हैं और अराजक मानवीय व मशीनी हस्तक्षेप के लिए गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं हैं। पिछले दिनों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) की रिपोर्ट में कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीसी तिवारी के शोधपत्र के हवाले से बताया गया था कि हिमालयी क्षेत्र का तापमान सन 2000 से 2010 तक यानी दस वर्षों में 0.2 डिग्री सेल्सियस और 2011 से 2020 तक 0.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। हिमालय के अधिकांश ग्लेशियर जो पहले ही पिघलकर पीछे हटते जा रहे हैं, उनके गलन में तेजी आएगी। शोध में कहा गया है कि जीवनदायिनी गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर सालाना 18 मीटर की दर से पिघलता जा रहा है।
खतरनाक संकेत
एक अन्य अध्ययन में गंगा की प्रमुख सहायक नदी अलकनंदा के सेटेलाइट चित्रों से यह खतरनाक संकेत मिले हैं कि अलकनंदा बेसिन ग्लोबल वार्मिंग की गहरी चपेट में है। अलकनंदा बदरीनाथ से आगे उच्च हिमालय के अलकापुरी क्षेत्र में सतोपथ और भगीरथ ग्लेशियरों से निकलती है। इस नदी बारे में अंतरराष्ट्रीय जर्नल ‘जियोकार्टो’ में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि पिछले 50 सालों के दौरान अलकनंदा के ग्लेशियरों का क्षेत्र 59 वर्ग किलोमीटर यानी आठ प्रतिशत तक सिकुड़ चुका है। अध्ययन कहता है कि संबंधित ग्लेशियरों के गलने की दर 11.7 मीटर प्रतिवर्ष है। मुख्य ग्लेशियर छोटे-छोटे हिस्सों में बंट चुका है। ये लघु ग्लेशियर गलन की गति में तो इजाफा कर रहे हैं मगर जल की मात्रा में योगदान करने में सक्षम नहीं हैं। अध्ययन कहता है कि अलकनंदा की इस हालत के कारण आने वाले समय में गंगा नदी को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा।

हिमनदों और इनसे निकल रही नदियों के जल क्षेत्र में हो रहे इन परिवर्तनों को वैज्ञानिक सीधे तौर पर स्थानीय स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तनों से जोड़कर देख रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में पहाड़ों को इकोलॉजी संबंधी अनेक समस्याओं जूझना होगा। नए मौसमी अध्ययन इशारा कर रहे हैं कि अनेकानेक कारणों से पहाड़ों की जलवायु में हो रही तब्दीलियां वैश्विक रुझान से जरा भी अलग नहीं हैं। अकेले अलकनंदा बेसिन में जाड़ों का तापमान 1968 से लेकर 2020 तक प्रतिवर्ष 0.03 सेल्सियस की गति से बढ़ा है।
हिमालय का विशाल क्षेत्र ग्लेशियरों ने थामा हुआ है। यहां की नदियों के प्रमुख स्रोत ये ग्लेशियर ही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के सिद्धांतकारों के अनुसार हिमालय के अधिकांश ग्लेशियर तेजी से पिघलते जा रहे हैं। गलन की यह प्रक्रिया जैसे-जैसे तेज होगी, उच्च हिमालय में हिमस्खलनों में भी तेजी आएगी। शिखरों पर टूटती बर्फ नीचे घाटियों में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ा देगी। शुरू में बाढ़ का कहर टूटेगा और बाद में पानी की कमी से अनेक नदियां पीली पड़ जाएंगी। इन सिद्धांतकारों के मुताबिक संसाधनों के दोहन की एवज में सरंक्षण के उपायों की गति बहुत धीमी है। हालांकि भूगर्भ वैज्ञानिकों का दूसरा तबका ग्लेशियरों के क्षरण को किसी बड़े खतरे से जोड़कर नहीं देखता। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वैज्ञानिक यह मानते आए हैं कि शिखरों पर समय-समय पर बर्फ गिरती रहती है जो गर्मियों में पिघलती है। लोडिंग-अनलोडिंग का यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है। कई मर्तबा कुछ कमजोर बिन्दु जरूर सक्रिय हो जाते हैं। इन वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग का असर ग्लेशियरों को किस हद तक प्रभावित कर पाया है या कर सकता है, इसके कोई ठोस आंकड़े उनके पास बेशक न हों, पर वे इसके लिए तैयार नहीं है कि हर परिवर्तन को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखा जाए। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि जो खतरे और चेतावनियां बताई जा रही हैं, वे मात्र दूर संवेदी आंकड़ों पर आधारित हैं। इस क्षेत्र के कुल 9575 ग्लेशियरों में से अब तक सिर्फ 25 से 30 का ही गहन अध्ययन हो पाया है।
हिमालय ग्लोबल एजेंसी में क्यों नहीं
ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर क्षरण को लेकर वैज्ञानिक समूहों के बीच मतभेदों के बावजूद मध्य हिमालय का सारा परिदृश्य हमारे सामने स्पष्ट है। हिमालय न सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, बल्कि मृदु जल का सबसे बड़ा स्रोत भी है। विश्व में सबसे ऊंची चोटियां में से 100 से अधिक अकेले हिमालय में हैं। एशिया के 130 करोड़ यानी वैश्विक आबादी के लगभग 17.8 प्रतिशत लोग जल के लिए हिमालय पर निर्भर हैं। बावजूद इसके हिमालय ग्लोबल एजेंडे में नजर नहीं आता। वर्ल्ड माउंटेन फोरम में भी हिमालय पर कोई बात नहीं होती। और तो और, भारतीय समाचारों तक में हिमालय की कवरेज चार फीसदी भी नहीं है।
भारत सरकार ने 2008 में जलवायु परिवर्तन ‘नेशनल मिशन फॉर सेस्टेनेबल डवलपमेंट ऑफ हिमालया’ नामक कार्यक्रम जारी किया। इसी कड़ी में जून 2014 में नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ‘नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज’ के लिए 108 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। लेकिन इन मिशनों के माध्यम से कितना कार्य हो पाया, यह कह पाना इसलिए भी कठिन है कि आज भी हमारे पास हिमालय को लेकर लंबी अवधि के ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिनके आधार पर हम जलवायु परितर्वन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरों के प्रतिरोध में हिमालय के लिए लंबी अवधि के कार्यक्रम तय कर सकें।
चारधाम यात्रा
उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को यहां की प्राणशक्ति माना जाता है। यहां का सारा वातावरण सदियों से ऋषियों, मनीषियों, अध्येताओं, तीर्थयात्रियों और सैलानियों को न सिर्फ आकर्षित करता रहा है, बल्कि उनके अनुभवों को दिव्यता व भव्यता भी प्रदान करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह अलौकिकता ही इस क्षेत्र के दोहन की सबसे प्रमुख वजह बन गई है। आज इस क्षेत्र का साबका विकास के नाम पर भारी-भरकम मशीनीकरण और अराजक मानवीय हस्तक्षेप से पड़ा है। सरकारों की छत्रछाया में पलते भू-भक्षियों और निजी निवेशकों को अपनी तिजोरी भरने के इरादे से इन पर्वतों, घाटियों और नदियों को साधने की जिद के आगे किसी चीज की परवाह नहीं है। पहाड़ों की छातियों पर भारी-भरकम मशीनों की सवारी जल, जंगल और जमीन से जुड़े संतुलन में खतरनाक बदलाव ला रही है। नदी-घाटियों और चोटियों के साथ लगातार बढ़ रही छेड़छाड़ उन्हें आपा खोने पर मजबूर कर रही है। जड़ से खोखला होने के कारण लगातार फिसल रही ढलानें यदि अपना रास्ता आप चुनने को मजबूर हुई हैं तो हिमालयी क्षेत्र में आए दिन होने वाले हादसों को ‘आपदा’ कहना बेमानी होगा।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)