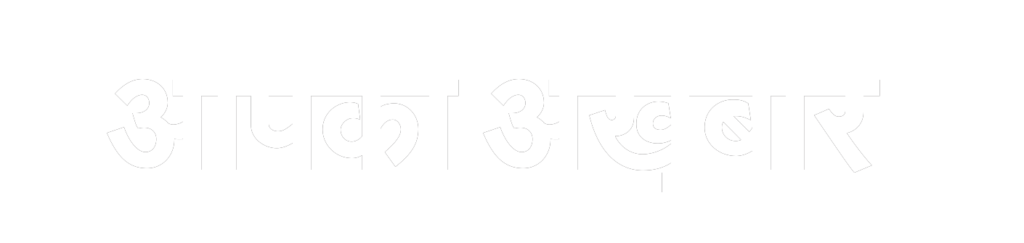बी.पी. श्रीवास्तव ।
बी.पी. श्रीवास्तव ।
भारतवर्ष में माइनॉरिटीज शब्द मुसलमान का पर्यायवाची बन गया है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को देखते हुए सवाल यह उठता है कि क्या अल्पसंख्यकवाद पर जोर, धर्मनिरपेक्षता का दुश्मन नहीं है क्योंकि वह समाज को बांटता है, जोड़ता नहीं।
भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला बहुधार्मिक देश है। इसने बहुत से धर्मों को जन्म दिया है। साथ ही बहुत से ऐसे धर्मों के लोगों को शरण भी दी है जो अपने देश में सताए गए थे। आज कई अन्य देश भी बहुधार्मिक हो गए हैं पर उनमें और भारत में एक अन्तर है। वहां के धार्मिक अल्पसंख्यक बाहरी देशों से आए विस्थापित लोग हैं, जबकि भारत के अधिकतर धार्मिक अल्पसंख्यक इसी मिट्टी के बेटे हैं क्योंकि इनका अतीत यहां के प्राचीन धर्म से ही जुड़ा है। इस लिहाज से भारत में दूसरे देशों के मुकाबले आत्मसात्करण आसान होना चाहिए था। पर दुर्भाग्य्वश ऐसा हुआ नहीं और देश अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक सिंड्रोम में फंस कर एक साम्प्रदायिक समाज बन कर रह गया, जिसकी राजनीति के मुख्य शब्द हैं- सेक्युलर, कम्युनल और माइनॉरिटीज यानी मुसलमान।
अल्पसंख्यकों के साथ दूसरे के बच्चों सरीखा व्यवहार
आजकल कई लोग बात बात पर 42वें संवैधानिक संशोधन का हवाला देते हैं और कहते हैं कि उसके तहत भारत एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है। ऐसा कहते समय वे भूल जाते हैं कि भारत इस संशोधन के पहले भी एक सेक्युलर देश ही था। भारत के हक में यह बात सराहनीय है कि उसने देश का धर्म के आधार पर विभाजन होने के बाद भी अपने को सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने का निर्णय लिया। इसी के चलते वह हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा और अवसर प्रदान करता है। इस बराबरी की बात को यदि परिवार के नजरिये से देखा जाय तो हर सदस्य का परिवार में बराबर का हक और बराबर का दर्जा होता है। साथ ही परिवार के मुखिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह परिवार के हर सदस्य को एक नजर से देखे और किसी के साथ भेदभाव न करे। इसी बात को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो देश, एक परिवार है और सरकार परिवार की मुखिया।
ऐसे में यह समझ के परे है कि आखिर क्यों देश की सरकारों ने कदम कदम पर ‘हम’ और ‘वह’ का नजरिया अपनाते हुए माइनॉरिटीज यानी मुसलामानों को बाहरी समझा। उनके साथ दूसरों के बच्चों सरीखा व्यवहार करते हुए न तो अपने ऊपर उनके भविष्य की जिम्मेदारी समझी और न ही उन्हें आग से खेलने पर तारणा दी- जैसा आप अपने बच्चों के साथ करते हैं। मिसाल के तौर पर- सरकार न तो उनके लिए कोई धर्म सुधारक बिल लाई जैसा उसने अपने लोगों (बहुसंख्यकों) के लिए किया और न ही उसने उनके पूजा स्थलों को उस एंडोवमेंट बिल में शामिल किया जैसा हिन्दू पूजा स्थलों के लिए किया। यही नहीं एक अतिथि का दर्जा देते हुए उनके लिए इफ्तार पार्टी करते रहे और हज पर जाने के लिए अनुदान भी देते रहे। इस दोहरे मापदंड का नतीजा यह हुआ कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के ही दिमागों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी। इस भ्रम की स्थिति का जो नतीजा हुआ, उसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वसंत साठे ने अपनी पुस्तक ‘इंडिया टु बी ए ग्लोबल पावर’ में इस प्रकार वर्णित किया, ‘इस भ्रम की स्थिति ने अनेक अनैतिक धार्मिक मांगों को जन्म दिया।’
बंटवारे के बाद मुसलामानों की मनोवैज्ञानिक स्थिति
मुसलमानों के लिए अलग देश बनाए जाने की मांग बड़े जोर पर थी और यह बात 1945-46 के चुनाव परिणामों से भी सही निकली थी। मुस्लिम लीग ने चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह पछाड़ते हुए देश के मुसलमानों के 86.6 फीसदी वोट प्राप्त किये थे। यही नहीं उसने कांग्रेस को इस हद तक हराया था कि कांग्रेस को केंद्रीय असेंबली की 30 मुसलमान सीटों में से एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। उन दिनों की एक विशेष बात और भी थी। वह यह कि पाकिस्तान बनने का उत्साह उन प्रांतों में अधिक था जहां मुसलमान अल्पसंख्या में थे और जो विभाजन के उपरान्त भारत में रहने वाले थे। यह उत्साह उन दिनों के वाइसराय लार्ड वैवेल की नजर से छुपा नहीं रह सका। उन्होंने 1945 में ही सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑफ़ इंडिया को लिख कर बता दिया था कि पाकिस्तान बनने का उत्साह मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतो में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतो से कहीं अधिक है। मजे की बात यह है कि अविभाज्य भारत के कुल 9 करोड़ मुसलमानों में से विभाजन के बाद जो 4.3 करोड़ विभाजन भारत में रुक गए थे, वे मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों के ही थे जिनका पाकिस्तान के प्रति उत्साह अधिक था। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए, भारत में रह गए मुसलमानों की मानसिक स्थिति को समझने में कठिनाई नहीं होना चाहिए। वे डरे हुए थे। प्रसिद्ध लेखक ए.जे. नूरानी ने अपनी पुस्तक, ‘द मुस्लिम्स ऑफ़ इंडिया’ में इस पहलू को दर्शाते हुए ‘भारतीय मुसलमानों की भय मनोविकृति की तुलना उनकी उस मानसिक स्थिति से की है जो 1857 के सिपाही गदर की असफलता के बाद हुई थी।’ और यही वह समय था जब भारत का संविधान बनना भी आरम्भ हो गया था।
‘मैं देख रहा हूं कि हमारे माननीय दोस्त जो अभी तक बोले हैं वे अल्पसंख्यक वर्ग से निवेदन कर रहे थे। मैं उनको बता देना चाहता हूं महोदय कि देश में कोई माइनॉरिटी नहीं है। मैं अपने को माइनॉरिटी नहीं मानता हूं। एक धर्मनिरपेक्ष देश में माइनॉरिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है। मुझे वे सब अधिकार और बराबरी का दर्जा प्राप्त हैं जो किसी और को हैं और मेरे वही दायित्व हैं जो किसी और के।’ (CAD VII 863)
सरकार को परिपक्वता से काम लेना था
भारत रह गए मुसलमानों की मानसिक दशा तो शायद स्वाभाविक थी पर दिल्ली की नई सरकार के राजनेताओं को परिपक्वता दिखाना आवश्यक था। उनको ऐसे कदम उठाने चाहिए थे जिससे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच की पुरानी बातें जड़ से मिट जातीं। पर क्या हुआ नहीं। उन्होंने उन समझदार आवाजों पर भी ध्यान नहीं दिया जो उस समय देश में मौजूद थीं और जो अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक वाली विचारधारा को समाप्त करने की सलाह दे रही थीं। इस संदर्भ में जो तजमुल हुसैन ने 1950 में कांस्टीट्यूएंट असेंबली में जो कहा था, वह जानने लायक है। उन्होंने कहा था, ‘मैं देख रहा हूं कि हमारे माननीय दोस्त जो अभी तक बोले हैं वे अल्पसंख्यक वर्ग से निवेदन कर रहे थे। मैं उनको बता देना चाहता हूं महोदय कि देश में कोई माइनॉरिटी नहीं है। मैं अपने को माइनॉरिटी नहीं मानता हूं। एक धर्मनिरपेक्ष देश में माइनॉरिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है। मुझे वे सब अधिकार और बराबरी का दर्जा प्राप्त हैं जो किसी और को हैं और मेरे वही दायित्व हैं जो किसी और के।’ (CAD VII 863)
इसी प्रकार की भावनाओं का प्रदर्शन करते हुए जी.बी. पंत ने भी कांस्टीट्यूएंट असेंबली में कहा था, ‘भारत उच्च नैतिकता और धर्मनिरपेक्षता के शिखर पर खड़ा है। हमारा लक्ष्य एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है जिसमें कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाला विचार सामने न आए और सभी लोग बराबर के नागरिक होकर साथ साथ रहें।’ तजमुल हुसैन ने तो एक कदम आगे जाते हुए कहा, ‘एक सेक्युलर देश में यह आवश्यक है कि हम अपनी पोशाक से न पहचाने जाएं। यदि आप एक विशेष तरह की पोशाक पहनते हैं, तो यह तुरंत विदित हो जाता है कि आप हिन्दू हैं या मुसलमान। इस चीज को समाप्त कर देना चाहिए।’ दुर्भाग्यवश इनमें से किसी भी समझदार आवाज पर ध्यान नहीं दिया गया और माइनॉरिटीज शब्द ने भारत के संविधान में एक ऊंचा स्थान ही नहीं प्राप्त किया बल्कि देश की पूरी राजनीति भी उसी के चारों और घूमती रही।
अभी भी गलती जारी
आज स्वतन्त्रता के 73 वर्ष बाद भी भारत में मुसलिम वर्ग का मुख्य धारा से अलग थलग रहना और उनमें पिछड़ेपन की अनुभूति किसी से छुपी नहीं है। और ऐसा तब है जब सभी सरकारें मुसलमानों के हित का दम भरती रही हैं। अभी बहुत दूर की बात नहीं है जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में डेवलपमेंट कॉउन्सिल की 52वीं बैठक में कहा था, ‘हमको ऐसी परिवर्तनात्मक योजनाएं तैयार करनी होंगी जो अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को, विकास के फल बराबरी से हासिल करने की ओर सशक्त कर सकें। उनका देश के साधन पर पहला दावा होना चाहिए।’ पर क्या इन सब बातों का मुसलमानों को कोई लाभ मिला? परिणाम सामने है। जहां देश में दूसरे छोटे धार्मिक समूह पनप रहे हैं, वहीं सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग अपने पिछड़ेपन को लेकर सिसक रहा है। ऐसा इसलिए कि उसने आज तक अपने को मुख्य धारा से अलग किया हुआ है। क्या यह सामाजिक विचारकों के सोचने का विषय नहीं है कि आखिर गलती किसकी है- मुसलमानों की, या उस राजनीतिक सोच की जो स्वतंत्रता के समय से ही देश में हावी रही है।
प्रसिद्धि विधिवेत्ता और लेखक एम.सी. छागला अपनी पुस्तक ‘रोजेज इन दिसंबर’ में मुसलमानों और सरकार दोनों से बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, ‘मुझे सदा से अनुभूति रही है कि मुसलमान या उनमें से अधिकतर लोग अपने अल्पसंख्यक दर्जे पर जोर देने की गलती करते रहे हैं। उनको चाहिए कि वे अपने को राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित कर लें।’ सरकार से उन्होंने कहा, ‘मैंने अक्सर सरकार की अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों का दर्जा और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर निरंतर जोर देने वाली बातों पर असहमति जताई है। यह राष्ट्रीय एकता के रास्ते में बाधा बनकर आती है और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाजों के बीच खाई पैदा करती है।’
क्यों न हम अपना रास्ता बदलें
कितना अच्छा होता यदि देश के नेताओं ने अतीत से सबक सीखा होता और देश के विभाजन के बाद एक धर्मनिरपेक्ष देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली विचारधारा को दफना दिया होता, जिससे देश में एक धार्मिक एकता वाला समाज जन्म लेता। इस सच्चाई का अहसास मोहम्मद अली जिन्ना को भी अंत में हो गया था जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह अहसास 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कांस्टीट्यूएंट असेंबली में पाकिस्तान बन जाने के बाद दिए उनके भाषण में झलकता है, ‘हमको चाहिए कि हम सबके साथ बराबरी के भाव से काम करना आरम्भ करें। हम देखेंगे कि समय के साथ साथ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली बातें गायब हो जाएंगी।’ तो फिर हम क्यों ना अपना रास्ता बदलें और इस बात पर सहमत हों कि अल्पसंख्यकवाद और धर्मनिरपेक्षता एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। वे साथ साथ नहीं चल सकते।
(लेखक ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया (बेसिल) के वरिष्ठ सलाहकार हैं)