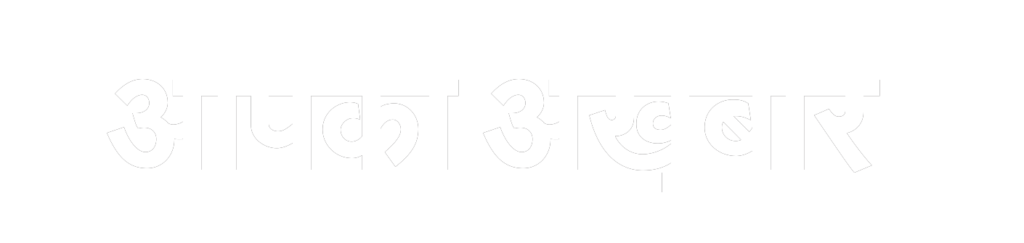नाट्य समीक्षा।
 सत्यदेव त्रिपाठी।
सत्यदेव त्रिपाठी।
प्रियवर योगेश त्रिपाठी लिखित एवं रानावि के स्नातक मुकुल नाग के निर्देशन में ‘पंख’ नाट्य समूह द्वारा आराम नगर (वरसोवा) स्थित ‘बेदा फ़ैक्टरी’ चौबारा में प्रस्तुत हुआ नाटक ‘नॉरवर्ग विला’ देखने का अवसर बना।
योगेशजी ‘मंजे हुए नाटककार हैं। इधर डेढ़ दशकों से उनके नाटकों को पढ़ते-देखते हुए जो सामाजिक सरोकारों से संचालित सीधे-सच्चे नाटक लिखने वाली उनकी छबि बनी थी, उसे तोड़ते हुए कुछ रहस्यों के साथ जीवन की पेचीदगियाँ लिये हुए आया है नाटक ‘नॉरवर्ग विला’। याने ‘आनंद भवन’, ‘कृष्ण कुंज’ में न रहकर हिंदी नाटकों के पात्र अब ‘नॉरवर्ग विला’ में रहेंगे!! और वह शीर्षक भी होगा। पूछना पड़ा कि हिंदी में इसे लिखें कैसे – ‘नो’ या ‘ना’, तो उन्होंने दोनो के बीच का ‘नॉ’ बताया। ठीक भी है – कृष्णकुंज में रहकर वे ढेरों आधुनिक काम नहीं होते, जो लेखक को इस चित्रकार पात्र से कराने हैं तभी तो बड़ा चित्रकार कहलाएगा!
 लेकिन नाटक में आनुवंशिकता भी इतनी तगड़ी है कि अपाहिज बाप नॉरवर्ग से जन्मी बेटी मार्था भी अपाहिज ही होती है। और वह चित्रकार बाप अरबपति की श्रेणी का अमीर होता है, तभी न इस बेटी को हाई-फ़ाई जगह पर रख पाता है और इतना अत्याधुनिक (अल्ट्रा मॉडर्न) भी बन पाता है कि अपने को उस बेटी के सामने कभी आने ही नहीं देता!! आने देता, तो शायद बड़ा पिछड़ा बाप हो जाता!! और आधुनिकता यहीं नहीं रुकती, वह जब अपनी प्रिया जिसेल (जो मंच पर नहीं, उल्लेखों में आती है) से शादी करता है, तो उसकी १२ साल की बेटी भी रहती है – एमिली, जिसे अपनाता है ‘मॉडर्न पेंटर’। फिर इस आधुनिकता की ऐसी उपयोगिता भी होती है कि बड़ी होकर यही पूरे तन-मन से सौतेले बाप की सेवा असली बेटी की तरह करती है – नाटक की नायिका बनती है। लेकिन अपने असली पिता के बारे में कभी नहीं पूछती!! तभी न बनता है उत्तर आधुनिक जीवन!! दर्शक उस स्त्री को देख नहीं सकता, जो बारह साल की बेटी के साथ चित्रकार नॉरवर्ग से शादी करती है!! इससे मंच पर एक पात्र कम का सुभीता होता है और ‘हम दो, हमारा एक’ वाला प्रगत जीवन भी नुमायाँ हो जाता है। फिर चित्रकार की अपनी बेटी मार्था बाप के रहने तक घर से दूर रहती है । उधर चित्रकार के पुराने दोस्त का लड़का आकर घर की तरह रहता है। हाय राम, कितनी आधुनिकताएँ, कितनी संगतियाँ-विसंगतियाँ!! लेकिन सबका चूर में चूर बिठाने वाले चुस्त-दुरुस्त लेखन के लिए भी योगेशजी बधाई के हक़दार हैं।
लेकिन नाटक में आनुवंशिकता भी इतनी तगड़ी है कि अपाहिज बाप नॉरवर्ग से जन्मी बेटी मार्था भी अपाहिज ही होती है। और वह चित्रकार बाप अरबपति की श्रेणी का अमीर होता है, तभी न इस बेटी को हाई-फ़ाई जगह पर रख पाता है और इतना अत्याधुनिक (अल्ट्रा मॉडर्न) भी बन पाता है कि अपने को उस बेटी के सामने कभी आने ही नहीं देता!! आने देता, तो शायद बड़ा पिछड़ा बाप हो जाता!! और आधुनिकता यहीं नहीं रुकती, वह जब अपनी प्रिया जिसेल (जो मंच पर नहीं, उल्लेखों में आती है) से शादी करता है, तो उसकी १२ साल की बेटी भी रहती है – एमिली, जिसे अपनाता है ‘मॉडर्न पेंटर’। फिर इस आधुनिकता की ऐसी उपयोगिता भी होती है कि बड़ी होकर यही पूरे तन-मन से सौतेले बाप की सेवा असली बेटी की तरह करती है – नाटक की नायिका बनती है। लेकिन अपने असली पिता के बारे में कभी नहीं पूछती!! तभी न बनता है उत्तर आधुनिक जीवन!! दर्शक उस स्त्री को देख नहीं सकता, जो बारह साल की बेटी के साथ चित्रकार नॉरवर्ग से शादी करती है!! इससे मंच पर एक पात्र कम का सुभीता होता है और ‘हम दो, हमारा एक’ वाला प्रगत जीवन भी नुमायाँ हो जाता है। फिर चित्रकार की अपनी बेटी मार्था बाप के रहने तक घर से दूर रहती है । उधर चित्रकार के पुराने दोस्त का लड़का आकर घर की तरह रहता है। हाय राम, कितनी आधुनिकताएँ, कितनी संगतियाँ-विसंगतियाँ!! लेकिन सबका चूर में चूर बिठाने वाले चुस्त-दुरुस्त लेखन के लिए भी योगेशजी बधाई के हक़दार हैं।
मूल नाटक तो कहानी के उस मोड़ के साथ ही शुरू होता है, जब चित्रकार के जिगरी दोस्त का लड़का सूरज चित्रकला सीखने आ जाता है। यह आना-रहना एक तरफ़ उक्त प्रगत जीवन को तोड़ता है, दूसरी तरफ़ उस पुराने भारतीय जीवन को सार्थक करता है जब दोस्तों-नातेदारों के बच्चे परिवारों में घर की तरह पलते थे और यहाँ तो नाटक को बेहद ज़रूरत थी – इसी को नायक बनना है। वरना बाप-बेटी ही रहते, तो ऐसा नाटक कैसे होता!! अब साथ रहते हुए सूरज-एमिली का प्रेम होना ही था – आख़िर तो ‘आग-भूसे की तरह ही होते हैं लड़का-लड़की’ (‘ब्वायज ऐंड गर्ल्स आर लाइक फ़ायर एंड स्ट्रा’)। और प्रेम-प्रसंगों के लिए भी बाप का अपंग होना बड़ा मुफ़ीद सिद्ध होता है। किंतु उन्हें देखते हुए मुझे पता नहीं क्यों डर लगा रहता था कि कहीं कभी बाप देख न ले। वैसे तो वह पहिए वाली कुर्सी से भी अकेले कहीं आ-जा नहीं सकता, लेकिन मेरी छठीं इंद्रिय वाला शक़ सच हो गया, जब एक दिन सूरज-एमिली समुद्र किनारे (लोकेशन की कल्पना भी ध्यातव्य है) से घूम के आते हैं, तो बाप बैठक में मिलता है। कैसे आया, यह प्रस्तोता नहीं बताता। किताब पढ़ी, तो उसमें किसी-किसी तरह जद्दो-जहद करके आने का उल्लेख है। तो क्या निर्देशक ने यह बेज़ा छूट ले ली या अभिनेता संजय गांधी ऐसा करने को तैयार नहीं हुए या समर्थ नहीं थे जबकि बाक़ी सारे दृश्य तो उन्हें ठीकठाक व संतुलित अभिनेता साबित करते हैं। अभिनय बहुत प्रभावी नहीं, तो निपटाऊ तो क़तई नहीं। जो भी हो, यह रंगकर्म की हानि है और तब तो और बढ़ गयी, जब ठीक उसी वक्त उधर नादान प्रकाश-संचालन से दर्शक देख लेते हैं कि कुर्सी धकेल के कोई ला रहा है। ख़ैर, अब हम तो समझ रहे थे कि प्रेम के लिए दोनो को डाँट-वाट पड़ेगी, किंतु कलाकार नॉरवर्ग तो मॉडर्न है न!! सो, बेटी ही चौंक कर पूछती है – कैसे आये? पर बाप अलग ही प्रसंग शुरू कर देता है – ‘आज मैने हिम्मत की – एक पेंटिंग बनायी’। फिर एमिली को हटाके पिता अपनी बेटी के साथ शादी करने का कौल ले लेता है सूरज से। फिर सूरज और दर्शक को तो क्या चाहिए – अंधे को दो आँखें। सो, मोग़म्बो लोग (सूरज व दर्शक) खुश हुए!!
लेकिन इन सबके बाद ही आकस्मिक रूप से बाप हार्ट अटैक से मर जाता है – बीच में सूरज को सिखाने आदि की पूरक बातें यथोचित आयी हैं। ख़ैर, मरने के बाद उसका वकील जॉन आता है, जो पहले भी दो-तीन बार आने-जाने से दर्शकों के लिए अजबवी नहीं है। वह अपनी सादी व निरपेक्ष, ‘काम से काम’ वाली निठुरी गतिमान अदा में विरल भी है और स्मरणीय भी। उसका चलना-बोलना सब मशीन जैसा निर्देशक ने ही बनाया होगा, जिसे शुभांकर विश्वास ने उसी तरह निभाया भी है, जो अलग प्रभाव भी छोड़ता है। उसके द्वारा अपने उसी मशीनी अंदाज में वसीयत सुनाने के दौरान असली नाटक सामने आता है, जब रहस्य खुलता है कि मृत चित्रकार की एक और बेटी भी है, जो उसकी औरस संतान है – मार्था। और बाप ने एमिली से नहीं, इसी दूसरी बेटी मार्था से सूरज की शादी की बात कही है, जिसकी शर्त यह भी है कि शादी से और शादी तक ही वह सारी सम्पत्ति का मालिक होगा, वरना नहीं – याने ज़िंदगी भर उस अपाहिज लड़की के साथ बँध के रहने का पुख़्ता इंतज़ाम, जो कि व्यावहारिक तो है ही, भुक्तभोगी बाप के लिए सर्वथा जायज़ भी है और उसके अमीर व कलाकार के अंह-तुष्टि के पूर्णतः लायक़ तो है ही।
 अब वह वारिस बेटी मार्था भी पहिए वाली कुर्सी पर नमूदार होती है। इस प्रकार यह कुर्सी भी नाटक की एक पात्र के रूप में हमेशा मंच पर मौजूद रहती है, जो इस निर्देशक के इससे पहले वाले नाटक में भी थी। इससे कयास होता है कि पाँव से अपाहिजों से और इसीलिए कुर्सी के साथ भी निर्देशक का कुछ ख़ास-सा लगाव ज़रूर है। या फिर मंच-सम्पत्ति के रूप में कुर्सी ख़रीद ली गयी है, तो अपाहिजों पर नाटक करके उसे सधाना है। लेकिन पिछले नाटक में कुर्सी ही कुर्सी थी छह फ़ोनों के बीच इतना चक्कर मारती रही कि हमे रात को भी चक्कर आते रहे। ख़ैर,
अब वह वारिस बेटी मार्था भी पहिए वाली कुर्सी पर नमूदार होती है। इस प्रकार यह कुर्सी भी नाटक की एक पात्र के रूप में हमेशा मंच पर मौजूद रहती है, जो इस निर्देशक के इससे पहले वाले नाटक में भी थी। इससे कयास होता है कि पाँव से अपाहिजों से और इसीलिए कुर्सी के साथ भी निर्देशक का कुछ ख़ास-सा लगाव ज़रूर है। या फिर मंच-सम्पत्ति के रूप में कुर्सी ख़रीद ली गयी है, तो अपाहिजों पर नाटक करके उसे सधाना है। लेकिन पिछले नाटक में कुर्सी ही कुर्सी थी छह फ़ोनों के बीच इतना चक्कर मारती रही कि हमे रात को भी चक्कर आते रहे। ख़ैर,
जैसा कि ऊपर संकेत हुआ कि यह विकलांग चित्रकार इतना पक्का बाप रहा है कि उसने अपनी जन्मायी बेटी को अपना चेहरा क्या, फोटो तक कभी नहीं देखने दिया है, तो अब वह फ़ोटो में पूछकर बाप को पहचानती है। किंतु यह चित्रकार अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त (ओब्सेस्ड) पति भी रहा कि अपने हर चित्र में एक ही चेहरा बनाता रहा, और अब चेले सूरज से भी एक ही चेहरा बनवाता है, जो उसकी कला की अवधारणा का एक मानदंड बनता है कि दुनिया दृष्टिगत सत्य है। और वह अवधारणा सिद्ध होती है – ‘हर सूरत साक़ी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, आँखों के आगे कुछ भी हो, आँखों में है मधुशाला’।
लेकिन वही कलाकार बाप उस ग़ैर की जन्मी बेटी एमिली के प्रति इतना क्रूर भी सिद्ध होता है कि दिन-रात सारी सेवाएँ लेकर उसे अपनी वसीयत में कुछ नहीं देता!! एमिली के साथ इस अत्याचार की बावत लेखक से पूछा जाना चाहिए, लेकिन हमें लगा कि ऐसा कर देता, तो नाटक में बचता क्या? फिर तो जैसे सबके दिन फिरते हैं – नाटक के भी फिर जाते। लेकिन इस कुकृत्य पर एमिली के प्रेमी सूरज का चिढ़ता-झल्लाना जायज़ ढंग से क्षतिपूर्त्ति करता है, जो साहज स्वाभाविक है, लेकिन उस एमिली की आदर्शवादी रचना हमारी समझ से बाहर है, जो उस सौतेले व अब कृतघ्न हो गये पिता के प्रति अब भी उतनी ही समर्पित-उदार रहती है। वह देवी हो सकती है, मानवी नहीं। लेकिन प्रेमी सूरज इतना ज़मीनी व खाँटी आदमी अवश्य सिद्ध होता है कि सारी सम्पत्ति के बदले भी वह अपनी प्रेमिका एमिली को छोड़ कर मार्था से शादी नहीं करना चाहता। वाह रे भौतिक विरक्ति व हार्दिक अनुरक्ति!! बड़ी भूमिका के अलावा इस बात के लिए भी सूरज का पात्र सही नायक सिद्ध होता है। इतने पारिवारिक झोल-झाल से अब पता लगता है कि शुरू में चित्रकार ने सूरज से घर के राज़ छिपाने की शर्त क्यों रखी थ।
अपनी तन-जाया बेटी के प्रति इतने स्वार्थी सौतेले बाप के लिए भी एमिली इतनी उदारमना है, तो इस सगी बेटी मार्था को को भी उदारमना होना ही था। सो, वह सारी संपत्ति इन दोनो को दे देती है। और सारा राज-पाट पाकर राजा-रानी (सूरज-एमिली) सुख से रहने लगते हैं तो मैं भी क्यों न कह दूँ – जैसे इनके दिन फिरे, सबके फिरें!!
और मार्था? तो उसके लिए वह पहले वाली जगह है ही, पर अब वह भाड़ा कहाँ से देगी? जीवन-यापन का आधार क्या होगा आदि को लेकर नाटक कुछ नहीं कहता। शायद आप कहेंगे कि इतनी सारी जटिलताओं-उदारताओं वाली प्रेममयी-कलामयी-नाट्यमयी कथा में मैं जीवन-यापन जैसी इतनी मामूली बात कैसे पूछ सकता हूँ!! लेकिन बाप के रहते अनाथ की तरह रहने वाली इस लड़की की चिंता जब किसी ने न की, तो मैं भी कैसे न करूँ – आख़िर इस नाटय-जगत में रहकर भी इसका सबसे उपेक्षित प्राणी -नाट्यालौचक जो ठहरा!! बहरहाल।
 इतने तिलिस्मी रहस्यों वाला नाटक भी योगेशजी लिख पाएँगे, जानकर अच्छा लगा – कम से कम इस विविधता के लिए तो लगा ही। अब इतने भावात्मक आलोड़न-विलोड़न के बाद इसे जीवन के प्रति प्रतिबद्धता वाला नाटक भी क्यों न कहें? और परत-दर-परत इतने रहस्यों, मनुष्य की इतनी सारी वृत्तियों से भरी कथा तो नाटय-विधा के लिए एकदम फिट है ही, रहस्य-जिज्ञासा,रूमान-कलाप्रेम, गहरे दोस्ताने, शातिराने जज़्बात आदि से भरपूर यह कथा मंच-विधा के लिए बेहद सही-सटीक!! मुकुल नाग ने अपने लगभग पूरे परिवार को शामिल करके इतने मन से बनाया है कि उसमें चार चाँद लगने की सम्भावनाएँ दिख रही हैं। बाप तो अभिनय में भी बाप है – रहस्यों के लिए रहस्यमय है, जो आगे के शोज़ में अच्छी रियाज़ के बाद अपनी रहस्यमयता में और खुलेगा, तो शायद चमके भी। असली बेटी मार्था बनी पाखी नाग को छोटी भूमिका मिली है – वह भी कुर्सी में क़ैद, पर अभिनय की चौचक रिहाई उसकी शख़्सियत से ही हो जाती है। पाखी का व्यक्तित्व जो काम कर देता है, उसे एमिली बनी शिवानी झा अपने तन्वी (स्लिम) व्यक्तिव में हाव-भावों, अभिव्यक्तियों-अदाओं से धीरे-धीरे पकाती है। भूमिका लम्बी है, तो अभ्यास ज्यादा हुआ होगा, जिससे लगता है कि शुरुआती १५-२० मिनटों के बाद शिवानी झा सम पर आती है, तो खूब आती है – एकाकार भी हो जाती है। उसके परिधान-परिवर्तन भी समझ में आते हैं और उसकी अदा में अच्छा सहाय करते हैं। इसी से अब उसमें ज्यादा लहकने की उर्वरता बची नहीं, तो ज़रूरत भी नहीं। सूरज की भूमिका भी बड़ी है, विविधताओं भरी है। इसे अंजाम देने वाले राघव राजपूत के सामने पहली चुनौती परायों के बीच अपनों की तरह रहने की है, जिसे वे मंच पर आने के चंद मिनटों बाद ही वाचिक-कायिक दोनो स्तरों पर बखूबी पकड़ लेते हैं। हाँ, उसके पास अपने पिता के साथ नायक की गाढ़ी यारी की नौका है, तो प्रभावी देहयष्टि की सबल पतवार भी है, जिसके संचालन में वह विविध रूपी भावों व बोलने के उतार-चढ़ावों तथा आंगिकता का अनुकूल उपयोग करके भूमिका के साथ न्याय के स्तर को छूने लगता है – आगे के शोज़ में समरस होते हुए खेलने की भी संभावनाएँ प्रबल हैं। पर प्रस्तुति का नायक तो पिता ही है, जो किरदार के क़द के मुताबिक़ बंद (गम्भीर) रहने के साथ अच्छा खुला है और आगे चलके और खिलने के आसार हैं।
इतने तिलिस्मी रहस्यों वाला नाटक भी योगेशजी लिख पाएँगे, जानकर अच्छा लगा – कम से कम इस विविधता के लिए तो लगा ही। अब इतने भावात्मक आलोड़न-विलोड़न के बाद इसे जीवन के प्रति प्रतिबद्धता वाला नाटक भी क्यों न कहें? और परत-दर-परत इतने रहस्यों, मनुष्य की इतनी सारी वृत्तियों से भरी कथा तो नाटय-विधा के लिए एकदम फिट है ही, रहस्य-जिज्ञासा,रूमान-कलाप्रेम, गहरे दोस्ताने, शातिराने जज़्बात आदि से भरपूर यह कथा मंच-विधा के लिए बेहद सही-सटीक!! मुकुल नाग ने अपने लगभग पूरे परिवार को शामिल करके इतने मन से बनाया है कि उसमें चार चाँद लगने की सम्भावनाएँ दिख रही हैं। बाप तो अभिनय में भी बाप है – रहस्यों के लिए रहस्यमय है, जो आगे के शोज़ में अच्छी रियाज़ के बाद अपनी रहस्यमयता में और खुलेगा, तो शायद चमके भी। असली बेटी मार्था बनी पाखी नाग को छोटी भूमिका मिली है – वह भी कुर्सी में क़ैद, पर अभिनय की चौचक रिहाई उसकी शख़्सियत से ही हो जाती है। पाखी का व्यक्तित्व जो काम कर देता है, उसे एमिली बनी शिवानी झा अपने तन्वी (स्लिम) व्यक्तिव में हाव-भावों, अभिव्यक्तियों-अदाओं से धीरे-धीरे पकाती है। भूमिका लम्बी है, तो अभ्यास ज्यादा हुआ होगा, जिससे लगता है कि शुरुआती १५-२० मिनटों के बाद शिवानी झा सम पर आती है, तो खूब आती है – एकाकार भी हो जाती है। उसके परिधान-परिवर्तन भी समझ में आते हैं और उसकी अदा में अच्छा सहाय करते हैं। इसी से अब उसमें ज्यादा लहकने की उर्वरता बची नहीं, तो ज़रूरत भी नहीं। सूरज की भूमिका भी बड़ी है, विविधताओं भरी है। इसे अंजाम देने वाले राघव राजपूत के सामने पहली चुनौती परायों के बीच अपनों की तरह रहने की है, जिसे वे मंच पर आने के चंद मिनटों बाद ही वाचिक-कायिक दोनो स्तरों पर बखूबी पकड़ लेते हैं। हाँ, उसके पास अपने पिता के साथ नायक की गाढ़ी यारी की नौका है, तो प्रभावी देहयष्टि की सबल पतवार भी है, जिसके संचालन में वह विविध रूपी भावों व बोलने के उतार-चढ़ावों तथा आंगिकता का अनुकूल उपयोग करके भूमिका के साथ न्याय के स्तर को छूने लगता है – आगे के शोज़ में समरस होते हुए खेलने की भी संभावनाएँ प्रबल हैं। पर प्रस्तुति का नायक तो पिता ही है, जो किरदार के क़द के मुताबिक़ बंद (गम्भीर) रहने के साथ अच्छा खुला है और आगे चलके और खिलने के आसार हैं।
निर्देशक मुकुल नाग पक्खड़ रंगकर्मी हैं। निर्देशन के साथ मंच-नियोजन एवं रंगदीपन का ज़िम्मा भी उन्हीं का है। निर्देशन तो खूब सधा है, जो आगे के शोज़ में मँजा हुआ भी सिद्ध होगा। अपेक्षाकृत छोटे से मंच को समृद्ध दिखाने के लिए उस पर काफ़ी कुछ रखने के बावजूद उन्होंने कलाकारों की गतिमानता व खेलने-खेलाने के लिए पर्याप्त अवकाश भी सुलभ कर लिया है। याने प्रतीकात्मक न होकर सब कुछ वास्तविक है, तो उसी तरह सब कुछ सही राहों पर ऐसा रवाँ भी है कि कुछ क़िया गया हो, ऐसा दिखता नहीं और सब कुछ बखूबी हो भी गया है। लेकिन पहले शो में जाने हुए रास्तों को पहचानने की प्रक्रिया में कुछ अटकने-भटकने होती हैं, जो राह पकड़ लेंगी और कुछ कुछ ढिलाइयाँ भी दिखीं, जो धीरे-धीरे कसाव पा लेंगी।
इस नाटक की सफलता से हुलसे योगेशजी भी रहस्य-रोमांच की धारा के और भी नाटक लिखें, तो ‘शो मस्ट गो ऑन’ भी सार्थक होगा, जिसके लिए मैं भी क्यों न कहूँ – आमीन!!