 कमल जयंत।
कमल जयंत।
देश की 85 फीसदी शोषित-वंचित आबादी को संविधान में प्रदत्त अधिकार दिलाने के लिए वजूद में आये सियासी दल इन दिनों बहुजन समाज के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाले दल के खिलाफ लड़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बल्कि स्थिति यह है कि ये जिस दल को बहुजन विरोधी और मनुवादी बताकर हमेशा उसका विरोध करते रहते थे, इन दिनों वे उसी भाजपा की सरकार के समर्थन में अपनी आस्था जताते नजर आ रहे हैं। मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने व इन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए यूपी में दो प्रयास हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही बार ये गठबंधन लम्बा नहीं चल सका। अब स्थिति ये है कि विपक्षी दल अपने आपसी द्वंद के चलते अपने विरोधी दल को शिकस्त देने के लिए भाजपा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं।
लड़ाई भी, समर्थन भी
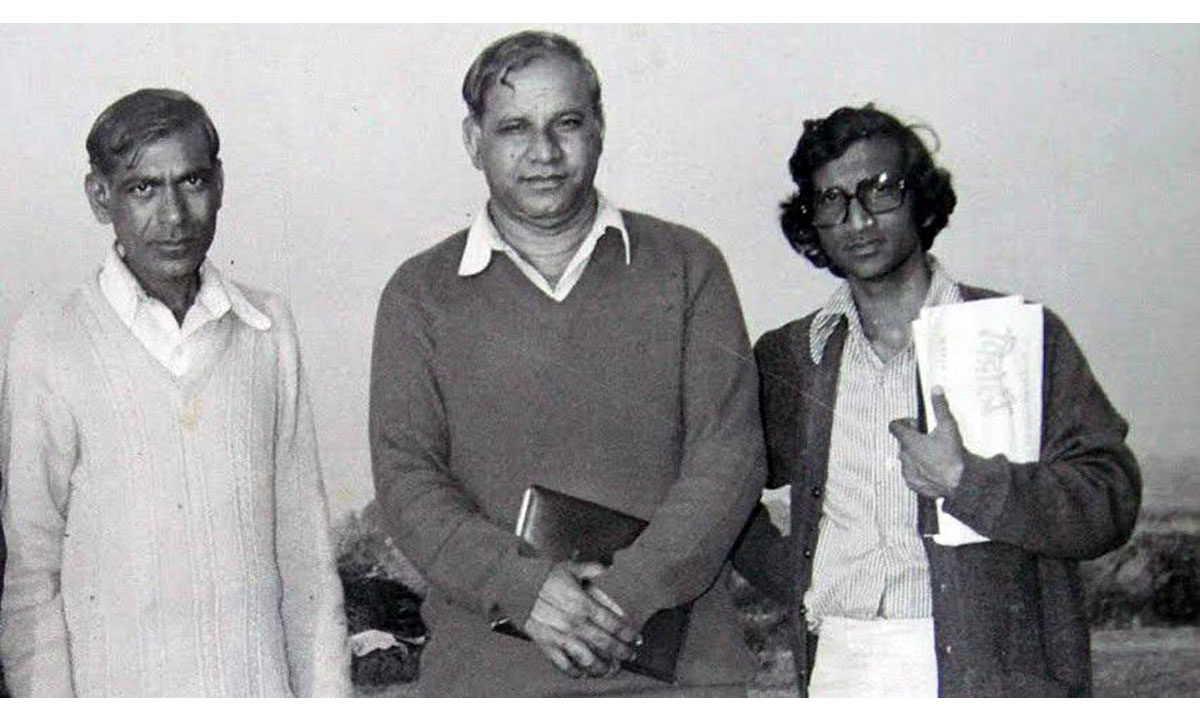
वैसे जिस विचारधारा को आगे बढाने के लिए बहुजन नायक कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, पार्टी अपनी उस मूल विचारधारा से विरत होती दिख रही है। कांशीराम ने मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कांग्रेस के साथ ही भाजपा को भी मनुवादी व्यवस्था का पोषक बताया। कांशीराम ने भाजपा के साथ मिलकर अपनी शर्तों पर तीन बार सरकार बनायीं और इस दौरान बहुजन समाज के हितों से कोई समझौता नहीं किया। बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए कांशीराम जी ने भाजपा से नाता तोड़ लिया, जिसकी वजह से बसपा की सरकार गिर गयी, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी कोई समझौता नहीं किया। मौजूदा हालात में अब बसपा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में खुलकर भाजपा के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हालाँकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भाजपा के खिलाफ बसपा चुनाव मैदान में होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बसपा प्रमुख मायावती राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाजपा का समर्थन क्यों कर रही है? बसपा प्रमुख ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की वजह भाजपा प्रत्याशी का आदिवासी होना बताया था। अब जबकि कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से मार्गेट अल्वा को प्रत्याशी बनाया है, जो दलित से ईसाई बनीं हैं। बावजूद इसके बसपा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर रही है और इसके पीछे समाज और मूवमेंट का व्यापक जनहित बता रही है।
विपक्षी एकजुटता का प्रयास नाकाम

एकजुट विपक्ष ही भाजपा को शिकस्त दे सकता है। बावजूद इसके छोटे-छोटे फायदे और अपने अहंकार को लेकर विपक्ष बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने को अलग रखा है। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक व सांसद इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसा करके वह अपनी कट्टर विरोधी भाजपा का ही सहयोग करेंगी। इसका जो कारण ममता बनर्जी ने बताया है वह है- उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी चयन में कांग्रेस ने उनसे सलाह नहीं ली। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ टीएमसी प्रत्याशी का खुलकर समर्थन किया था। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल भाजपा के खिलाफ लड़ने के साथ ही अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा की भी मदद कर रहे हैं। साथ ही भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का प्रयास भी नाकाम होता दिख रहा है।
सपा-बसपा का मिलना-बिछड़ना

देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर बहुजन नायक कांशीराम ने यूपी में ही भाजपा को रोकने के लिए वर्ष 1993 में सपा के साथ गठबंधन किया और विधानसभा के चुनाव में मंदिर आन्दोलन के उभार के बाद भी भाजपा को सत्ता में आने से रोक दिया। देश की सत्ता में भाजपा की वापसी को रोकने के लिए वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में एकबार फिर सपा-बसपा के बीच गठबंधन हुआ। हालाँकि ये गठबंधन भाजपा को रोक पाने सफल नहीं हुआ और चुनाव बाद बसपा ने ये गठबंधन तोड़ लिया। इस गठबंधन का एक फायदा ये हुआ कि कांशीराम ने जिस शोषित-वंचित बहुजन समाज- जिसमें दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज शामिल हैं- वे करीब आए। अगर ये गठबंधन लम्बा चलता तो बहुजन समाज के बीच स्थापित हो रही एकता और मजबूत हो सकती थी। यह बहुजन समाज के लोगों की विड़म्बना ही है कि मनुवादी विचारधारा के खिलाफ आंदोलित दल निजी स्वार्थों की खातिर कहीं ना कहीं अपने कट्टर विरोधी विचारधारा वाले दल का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं।
“मोदी विरोध” से राष्ट्रवाद विरोधी खेमे में खड़ी होती कांग्रेस
कार्यकर्ताओं, समर्थकों में भ्रम
इस सम्बन्ध में सामाजिक संस्था बहुजन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस कुंवर फ़तेह बहादुर का कहना है कि विपक्षी दलों की अपनी विचारधारा है। यदि ये दल अपनी विचारधारा के विपरीत सत्ताधारी दल को सहयोग करते हैं तो इससे उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उनका कहना है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग के नेता जिस दल से जुड़े हैं, वे उसकी विचारधारा के मुताबिक काम करेंगे। यह सोचना बेमानी होगा कि वे बहुजन विचारधारा के पक्ष में काम करेंगे। केवल प्रतीकों के सहारे दलित और आदिवासी समाज का वोट पाने की खातिर इन वर्गों का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार देने से समाज जुड़ने वाला नहीं है। भाजपा भी प्रतीकों की राजनीति करती है, लेकिन साथ ही उनका काडर लम्बे समय से केवल चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि सामान्य दिनों में भी जमीनी स्तर पर उस समाज के बीच जाता रहता है। लेकिन सपा-बसपा इस दिशा में कोई ठोस काम करती नहीं दिख रहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूपी में सपा ही भाजपा के खिलाफ मजबूती से लडती दिख रही है। लेकिन आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के लिए हुए उप चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रचार से दूरी बनाये रखने व प्रत्याशी चयन में देरी की वजह से सपा को अपनी जीती हुई दोनों सीटें गंवानी पड़ीं। विधान परिषद के लिए 28 वर्षीय कीर्ति कोल का नामांकन करा दिया, जिसकी वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह आजम खां के बेटे के उम्र को लेकर चल रहे विवाद से भी सपा नेतृत्व को बचना चाहिए था। ऐसे मामलों से पार्टी को स्थिति हास्यास्पद हो जाती है।
(लेखक लखनऊ स्थित वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं)




