 सत्यदेव त्रिपाठी।
सत्यदेव त्रिपाठी।
पिछले दिनों पटना के ‘प्रवीण सांस्कृतिक मंच’ द्वारा आयोजित चार दिवसीय नाट्योत्सव देखने का अवसर बना, जो अपनी निर्मिति व प्रस्तुति में खाँटी एवं विविधरंगी रंगकर्म का जीता-जागता रूप बनकर दिल-दिमाँग पर छाया हुआ है, लेकिन यह कसक साल भी रही है कि यदि थोड़ी-सी सोच व सक्रियता और जुड़ जाती, तो यह अपने ढंग के नाट्योत्सवी रंगकर्म की मिसाल बन जाता…!!
इस नाट्योत्सव में प्रस्तुत चारो नाटकों के निर्देशक एवं पूरे उत्सव के संचालक पटना-निवासी श्री विज्येद्र कुमार टाँक से मेरी देखा-देखी, नमस्ते-आदाब तो ढाई दशक पुराना है, जब वे मुम्बई आये थे और सूत्र बने थे पटना के ही प्रसिद्ध रंगकर्मी विजय कुमार। तब टाँकजी कमसिन थे और बेहद चुप्पा हुआ करते थे, लेकिन चुप्पी टूटना और सहज बातचीत वाला मिलना भोपाल में हुए भी डेढ़ दशक से कम न हुआ होगा… तब सूत्र बने देश के शीर्ष नाट्य संगीतकार व पुन: पटना निवासी और टाँकजी के सार्वकालिक ग़ुरु संजय उपाध्याय, जो इस उत्सव में भी चारो शाम साथ रहे और इन नाटकों में संगीत तो उन्हीं का था ही, जिनमे एक तो लगभग पूरी तरह संगीत-आधारित ही था। उसके दो-चार साल बाद (कोरोना-काल के ठीक पहले) ही हमारे बुलावे पर ‘रंगशीर्ष’ नामक नये नाट्य समूह के उद्घाटन में उसी संजयजी और पटना के ही अपने ढंग के ज़हीन चिंतक व रंगकर्मी पुंज प्रकाश जी के साथ रात भर के लिए बनारस के मेरे निवास पर मिलना हुआ, तो फिर बातचीत फ़ोनों पर भी होने लगी – कभी-कभार व काम जितनी ही सही, होने लगी थी…, जिसके सहज परिणाम में इधर कई सालों से ‘प्रवीण स्मृति नाट्योत्सव’ देखने का बुलावा आता रहा…, पर मुम्बई की लम्बी दूरी व रंग़ समूह के नाहक बड़े खर्च की व्यावहारिक दिक़्क़तों के मद्देनज़र मैं टालता रहा, लेकिन इस बार बनारस में रहने के संयोग ने विज्येंद्र के बुलावों के तक़ादे की भरपाई कर देने का सुयोग बना दिया…।

नाटक के शुभारम्भ की दोपहर पहुँच गये पटने…। मुम्बई में बस गयी पटना की अभिनेत्री बच्ची शाइस्ता ही मेरे बनारस होने की सूचना का सूत्र बनी थी और वही मिलने भी आयी तथा शाम को सभागार ले जाने भी। गाड़ी में बैठते ही मिले – दूसरे विशेषज्ञ मेहमान अभिराम भड़कमकर, जिनसे फिर चार दिनों खूब छनी – जमके गप्पें हुईं…, क्योंकि हम दोनो के कमरे बगलगीर थे और नाटकों एवं फ़िल्मों की रुचियाँ भी काफ़ी समान निकल गयीं। तात्पर्य यह कि उत्सव-संचालक व आयोजक विज्येंद्र टाँक आयोजन-स्थल पर पहुँचने के बाद ही मिले…। ऐसे अनौपचारिक आचार के नये चलनों के अनुभव भी मुम्बई विराट नगर की यांत्रिक व्यावहारिकता में पिजे होने के चलते भले तो लगते हैं, पर पिछले चार दशकों के दौरान दर्जनों उत्सवों के अहसासों के बरक्स अनकुस (अनइजी)-सा अहसास भी कराते हैं, क्योंकि उस दौरान चाहे इप्टा, रायगढ़ के अजय आठले रहे हों या जबलपुर के अरुण पांडेय या हिमांशु राय हों या फिर सीधी के रोशनी मिश्र-नीरज कुंदेर…आदि (बहुतेरे) हों…, सभी समूह-संचालक आधी रात हो या तीन-चार बजे भोरहरे का वक्त…स्टेशन ही आते…। अगवानी की यह एक भावात्मक संस्कृति तो थी ही, वहीं से आग़ोश-अंकवार वाले भेंट-मिलन से जो हालचाल शुरू होते, नाटक के साथ जीवन के रस में भी सराबोर कर जाते…। यह अनुभव तीसरे दिन होटेल में मिलने आकर हमारी पीढ़ी के ऋषिकेश सुलभ दे गये…। और भाई संजय उपाध्याय तो एक दिन घुमाने ही आ गये – मशहूर गुरुद्वारे के सुशांत-दिव्य दर्शन व गुरूबानी-श्रवण के साथ पटने के नव-निर्मित सरिता-सेतु पर मैरीन ड्राइव का लुत्फ़ और गन्ने के मौसमांत पर उसके रसपान का अविस्मरणीय आनंद लिया गया…। कुल का तात्पर्य यह कि अब नयी पीढ़ी की यही संस्कृति है, जिसकी पहली झलक प्रवीण गुंजन और फिर रींवा के अपने शिष्य अंकित मिश्र में मिली थी…। लेकिन मिस्टर टाँक ने दो शामों को अपने घर पे सुस्वादु भोजन व मर्यादित आचमन से उस संस्कृति को भी गाढ़े अपनेपन की गहरी मसर्रत से लहका दिया…और चलने के दिन होटेल आये भी। याने संस्कृति ने अपना रूप बदल लिया है…और कुछ क्षीण भी अवश्य हुई है। पर सबके अपने-अपने मज़े हैं – ‘अपने अपने युग में सबको भायी अपनी-अपनी हाला’…। बहरहाल,

अब आयोजन-स्थल से जारी करें…। ‘प्रेमचंद रंगशाला’ पहली बार देखा। इसके पहले इस शहर में रंगकर्म से ही बावस्ता दो अवाइयों में ‘कालिदास रंगालय’ तक ही रह गया था। पटना शहर के एक मुख्य भाग में स्थित ‘प्रेमचंद रंगशाला’ का परिसर काफ़ी बड़ा है। थिएटर-कर्म के सभी आयामों – मंचन, नेपथ्य, नाट्याभ्यास, नुक्कड़-आयोजनों, बैठकों, व्यायाम…आदि के लिए पर्याप्ताधिक जगह है। लोग यहाँ-वहाँ बैठे-खड़े गपिया रहे थे, विचर रहे थे। इस जमाव की कोई अर्गला न थी, फिर भी बड़ा संयम था – लोग संयत थे…। न कोई गहमाग़मी, न अफ़रा-तफ़री, न भागमभाग, न शोर-शराबा…सबक़ुछ शांत-स्थिर… गोया व्यवस्थित हो! और जब समय हुआ, तो बिना किसी घोषणा या घंटी के यहाँ-वहाँ बिखरे लोग आपोआप…फिर एक दूसरे की देखा-देखी भी नुक्कड़ नाट्य-स्थल की तरफ़ बढ़ चले…जैसे कोई प्रशिक्षित समूह हो…। यह शांत-सहज नाट्य-संस्कृति भी मुझे लुभा गयी…।

चारो दिन नाटक के पहले के नुक्कड़ नाट्य इस उत्सव का बड़ा ही खूबसूरत आयाम रहा – गोया किसी शीशमहल में प्रवेश के पहले का श्रिंगाररूपी भव्य सिंहदवार हो…! पहले दिन की नुक्कड़ प्रस्तुति जहांगीर खान के निर्देशन में ‘आशा रिपर्टरी’ की थी…(जाने क्या मोह या मतलब है कि हिंदी में रंगमंडल, नाट्यसमूह…आदि जैसे अच्छे शब्दों के रहते ‘रिपर्टरी’ लिखा जाता है!! ख़ैर,)। प्रस्तुति थी – हरिशंकर परसाई की सदाबहार मशहूर रचना ‘भोलाराम का जीव’, जिसमें कहानी बिलकुल सही व सटीक यूँ व्यक्त हुई – गोया शीशे में उतार ली गयी हो…। नुक्कड़ विधा की सारी सम्भावनाओं का उपयोग करती हुई जितनी मनोरंजक, उतनी ही व्यंजक भी। सर्वाधिक मज़ा आया मूल के साथ जुड़े परिष्कारों (इम्प्रोवाइजेशंस) का। कहानी में सरकारी कार्यपद्धति की भ्रष्ट-आलसी-कामचोर क़ुसंस्कृति के साथ फ़ाइलों-कुर्सियों-बाबुओं एवं उनकी कारस्तानियों के ज़रिए प्रशासन की बहुरूपी कीमियागीरियों का तीखा व मज़ेदार निदर्शन है, जिसे आधुनिक तकनीक में कम्प्यूटर, ईमेल, व्हाटसअप…आदि से जोड़ देना अपने समय का साक्ष्य तो बना ही…, सोने में सुहागा-सा खूब फबा भी…। अभिनेता सब बड़े जोश व स्फूर्ति से लबरेज़ थे – पूरी प्रस्तुति के साथ खेलते हुए रमे थे…। दूसरे दिन प्रेमचंद की कहानी ‘खुच्चड़’ खेली गयी और तीसरे दिन ‘पालकी पालना’, जो हम एक दिन आयोजकों की भूल तथा एक दिन अपनी व्यस्तता के चलते देख न सके। चौथे दिन ‘नाट्य शिक्षक की बहाली’ वाले टिपिकल विषय में नाटक वालों के रोज़गार को अपना सामयिक व जरूरी दर्द रहा। ऐसे विषयों में ही नुक्कड़ विधा सार्थक होती है। ये प्रस्तुतियाँ कलाकारों के बाहुल्य और उनकी आपसी संगति, जो महानगरों से अलग छोटे शहरों-क़स्बों (गाँवों में थिएटर ही नहीं) की नेमत है, के रूप में बहुत प्रीतिकर लगा…। यूँ इस उत्सव के सभी नाटक भी बहुपात्रों वाले ही रहे, बल्कि कहीं-कहीं कलाकारों की सहज सुलभता के चलते जहां पात्रों को कम किया जा सकता था, वहाँ भी जोड़कर प्रस्तुति को अतिरिक्त समृद्ध कर लेना दिखा…और इसी बहुलता के कारण इस आकलन में सभी कलाकरों के अभिनय की चर्चा न हो पा रही है। और इससे अच्छी बात यह कि बच्चों के अफाट उत्साह में नाट्य-विधा के उज्ज्वल भविष्य की सम्भावनाएँ साकार होती दिखीं…। बहरहाल‘भोलाराम का जीव’ नुक्कड़ समाप्त होते ही मुख्य सभागार में पहुँचे, जिसका मंच तो सचमुच विशाल है – शायद नाट्य-शास्त्र के मानकों को पूरा करता हुआ…शायद उसके पार भी जाता हुआ…!! अपने मंच के अनुपात में और मुम्बई के टाटा थिएटर, नेहरू सेंटर जैसे बड़े सभागारों की अपेक्षा दर्शक-दीर्घा छोटी है, किंतु चारो दिनों की दर्शकता को देखते हुए शहर के सहृदय समाज के लिए काफ़ी है – याने पटना के लिए बहुत अनुकूल व योग्य। कुल मिलाकर वही कि सबसे सुंदरतर न सही, विविध दृष्टियों से उपयुक्त व बहुविध उपयोगी है प्रेमचंद सभागृह…।
यूँ तो इस समारोह में औपचारिकताएँ बहुत कम ही निभायी गयीं – सीधे नाटक हुए और नाटक के सिवा का सब कुछ बस अनिवार्य-जितना ही हुआ…, जो इस नाट्योत्सव का सबसे अच्छा पहलू रहा – मेरा मन-विचारों के अनुकूल, वरना कहीं-कहीं तो घोषणाएँ व नेता-परेताओं, अपने खासमखासों की ढेरों औपचारिकताएँ नाटक पर भारी होकर पका देती हैं…। लेकिन पहले दिन तो उद्घाटन होना ही था, जो नुक्कड़ नाटक होने के बाद हुआ…याने विधानत: उत्सव शुरू हो चुका था। लेकिन नुक्कड़ और मुख्य शो की प्रकृति के अनुसार दूसरा क्रम हो नहीं सकता था। ख़ैर,
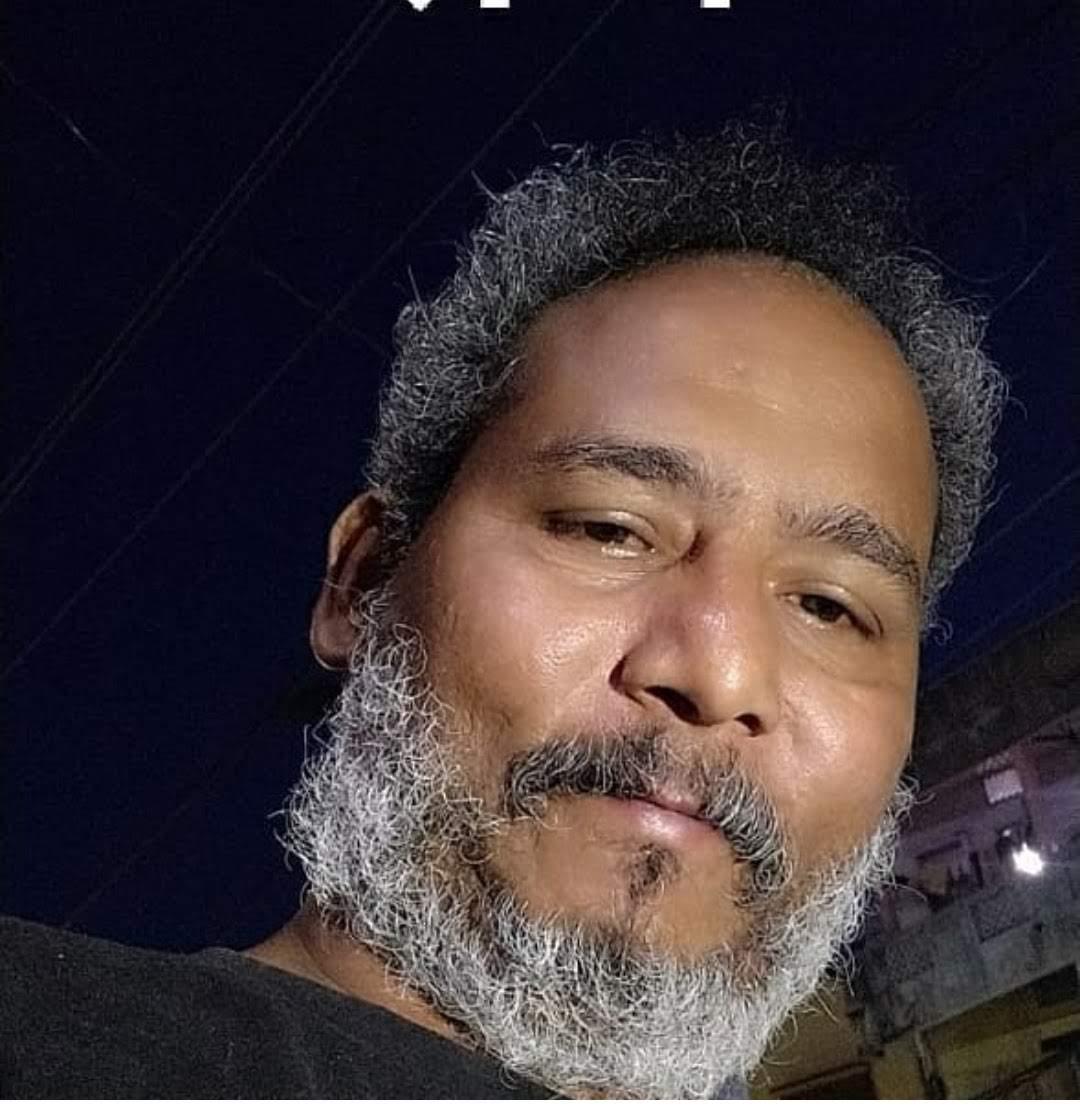
उद्घाटन की ख़ास बात यह थी कि वह औपचारिक न होकर सप्रयोजन था – ‘प्रवीण स्मृति सम्मान’ जो देना था। अब यही स्थल है इस आलेख में कि इस सम्मान व इसके ‘प्रवीण’ नाम का खुलासा कर दिया जाये…, जो नाटक के बड़े ज़हीन सरोकार से बावस्ता है। नाटक की एक धारणा यह भी है कि यह शूद्रों की विधा है, जो वेद-पुराणादि के ज्ञान एवं जीवन की अनिवार्य ज़रूरतों से भी वंचित अनपढ़ लोगों के लिए बनी, ताकि अक्षर-ज्ञान से भी विधानत: (स्त्री-शुद्रौ नाधीयताम्) महरूम वे लोग देख-सुन कर ही कुछ जान-समझ सकें। लेकिन प्रभाव ऐसा बना कि इसे चारो वेदों के बाद पाँचवाँ वेद कहा गया, फिर भी ब्राह्मण-कुल में पैदा होने के नाते बचपन में हमे नौटंकियाँ चोरी-चोरी देखनी पड़ती थीं। लेकिन हर नौटंकी कम्पनी के मैनेजर (संयोजक) अक्सर ब्राह्मण होते थे, जो या तो पहले से ही किसी आरोप वश जाति-बाहर होते थे या नौटंकी करने के नाते बहिष्कृत कर दिये गये होते थे। बहरहाल, सार यह कि जिस ख़ास वर्ग के लिए बनी नाट्य-विधा, उसी पिछड़ी जमात के मेधावी व क्रांतिकारी युवक थे प्रवीण, जो अपनी जमात को इन साँसतों से मुक्ति दिलाने की प्रगतिशील गतिविधियों की रहनुमाई करते हुए सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्ष में जुट गये थे, लेकिन प्रतिरोधी शक्तियों के हाथों क़त्ल कर दिये गये। परंतु उनकी मुहिम रुकी नहीं…आज तक चल रही है, जिसका सांस्कृतिक रूप है उनके भाई अपने विज्येंद्र टाँक के नेतृत्त्व में उन्हीं के नाम पर ‘प्रवीण सांस्कृतिक मंच’ अभिधान से चल रहा यह नाट्यकर्म। इस प्रकार मूलत: पिछड़े वर्गों का विकास-चेता होकर टाँकजी का यह थिएटर-कर्म सच्चे अर्थों में रंगकर्म को सार्थक कर रहा है। इसके सालाना नाट्योत्सव का नाम तो प्रवीण के नाम पर है ही, इसमें हर साल एक मेधावी कलाकर को ‘प्रवीण स्मृति सम्मान’ से नवाज़ा भी जाता है। और यह उद्घाटन-सत्र यूँ तो समारोह-सत्र ही था, लेकिन अधिक ताम-झाम व औपचारिकताओं के बिना ‘काम से काम’ का संक्षिप्त एवं मधुर आयोजन रहा यह…।
मंच पर प्रकाश होते ही माइक के साथ जो सज्जन नुमायाँ हुए, मेरे लिए पूरे आयोजन के सबसे चुनमुनवां शख़्स वही सिद्ध हुए – पूरे उत्सव के स्थायी संचालक अशोक तिवारी। न उनकी बुनावट में कोई बनावट थी, न प्रस्तुति में अदा-ओ-अंदाज या शेर-ओ-शायरी…आदि की कोई मिलावट। सबक़ुछ निराबानी था – सीधा-सहज, लेकिन सादगी का सौंदर्य शब्द-शब्द में झरता रहा था। सबसे ख़ास थी उनकी सिधाई, जिसमें उनकी सीमा भी कलाकारिता बन गयी। उदाहरण दूँगा ज़रूर…मंच पर आमंत्रित करते हुए अभिरामजी के श्रीनाम ‘भड़कमकर’ का उच्चारण न कर पाये, तो न शरमाये, न छिपाया…, सरे आम ग़लत बोल-बोल के सीखते हुए समापन के दिन तक सही बोल के दिखा दिया, जो कार्यक्रम की एक उपकथा बन गया। यह निछद्दम वृत्ति हमारे लोक की निधि रही है – गोया ‘ये बेबाक़ी नज़र की, ये मुहब्बत की ढिठाई है’, जो अब नष्ट हो गयी…सब कुछ औपचारिक-नीरस-बनावटी रह गया है।

उद्घाटन-समारोह की सबसे महत्त्वपूर्ण घोषणा हुई – यह नाट्योत्सव थोड़े ही दिनों पहले दिवंगत हुई, पटना की विदुषी साहित्यकार, ‘साहित्य अकादमी’ से सम्मानित और सबकी आदरणीय व प्रिय उषा किरण खान की स्मृति को समर्पित है’। उनके साहित्यिक अवदान की संक्षिप्त, पर सारगर्भित चर्चा भी हुई। उषाजी पिछले २५ वर्षों से मेरी भी प्यारी दीदी रहीं…। दीदी-विहीन पटना में पहली बार होना साल रहा था। उनकी तस्वीर पर हम सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की, जिससे मेरी बेचैनी को काफ़ी राहत मिली। यह सम्मान-कार्यक्रम संजय उपाध्याय के नेतृत्त्व में हो रहा था। वहाँ मौजूद लगभग सभी उनके शिष्य ही थे। सौमनस्य के माहौल में संजयजी ने सम्मान मूर्त्ति अपने प्रिय-पटु शिष्य मो॰ ज़फ़र आलम का बड़े सुमन से संक्षिप्त परिचय दिया – शेष परिचय तो चारो दिन के नाटकों में उनके अभिनय में साक्षात तस्दीक़ हुआ ही। मंचस्थों के हाथों सम्मान-ग्रहण के उपरांत ज़फ़र की अत्यंत संक्षिप्त व भावभीनी प्रतिक्रिया भी सुनी गयी…। कुल ४०-४५ मिनटों का यह कार्यक्रम जितना ज़रूरी था, उतना ही सधा हुआ भी सिद्ध हुआ।
लेकिन उद्घाटन-सत्र का सबसे कारगर प्रयोजन सिद्ध हुआ – बिहार सरकार में ‘संस्कृति एवं युवा’ विभाग की मुख्य सचिव मादाम हरजोत कौर की अध्यक्षीय उपस्थिति से। यूँ तो यह देश का दुर्भाग्य है कि जनता को ऐसे ज़हीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अपने ही (दिये कर के) पैसों को पाने में जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं… और कला-संस्कृति के पुराधाओं को मिलने वाले सम्मानों पर प्रशासनिक अधिकारियों व बालिश मंत्रियों को स्थापित करना पड़ता है, जिसे अब सबने ‘मजबूरी का नाम महात्मा गांधी’ की तरह मान लिया है। लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ कौरजी योग्य भी निकलीं और पर्याप्त विनम्र भी, जो उनकी ईमानदारी भरी बातों व सलीकों तथा उनकी ज़ुबानी निकले संस्कृतिक विकास व उत्थान की योजनाओं में साफ़-साफ़ दिख पड़ा…। यदि उनका कहा हुआ सब नियमित रूप से कार्य में उतरे, तो कम से कम उनके रहते प्रदेश के संस्कृति-कर्म आबाद रहेंगे, जिसका काफ़ी श्रेय इन आयोजकों की समझी-सुथरी दृष्टि व सत्प्रयत्नों को भी जायेगा…। बस, मंचन के बाद नाटक पर भी बोलने के लिए फिर से उन्हें मंच पर बुलाना ज़रा ज्यादा हो गया, जिससे बचा जा सकता था – गोकि हरजोतजी ने फिर सिद्ध किया कि कला-संस्कृति में उनकी अच्छी रुचि व पैठ है, जो किताबी न होकर ज़ेहनी और जेनुइन है…।
यहीं लगे हाथों कह दूँ कि मुम्बई से आने वाले हम टिकिट लेकर नाटक देखने की पद्धति से सुपरिचित हैं, लेकिन अपने उत्तर भारत में इसका नामों-निशान तक नहीं और नामोनिशान क़ायम करने की कोशिश तक नहीं। इसका एक बड़ा कारण सरकारी अनुदान भी है, जो मिल जाता है। मेरे गाँव में एक कहावत है – ‘गया पूत, जो मांगन पावा’ – याने वह सुपुत्र ‘देश से गया’, जिसे उधार मिल जाता है। इस प्रक्रिया में कौर मैडम जैसे उदारों के रहते रंगकर्म का स्वावलंबी होना और मुश्किल होता जायेगा…। मैं जानता हूँ कि यह पढ़कर उत्तर भारत के लोग मेरी कमतर बुद्धि पर हँसेगे, लेकिन रंगमंच की भलाई का अंतिम सत्य (अल्टीमेट रीयलिटी) इस मंगन-वृत्ति को रोकने में ही है।
अब उत्सव के मुख्य भाग – नाटकों पर आयें…। पहले दिन का नाटक था – ‘गुंडा’। प्रसादजी की सरनाम कहानी पर आधारित यह नाटक दिल्ली के कामपटाऊ निर्देशक के ‘कहानी का रंगमंच’ वाला कामचलाऊ काम न था – सम्पूर्ण मंचीय संभार (मंच-सामग्री, वेशभूषा, पात्रवत आहार्य, गीत-संगीत-नृत्य…आदि) के साथ मुकम्मल नाटक था। यह ठीक है कि कहानी इतनी मशहूर है कि मैं मंच पर इस गुंडे में प्रसादीय वर्णन की छबियाँ खोज रहा था, लेकिन लिखित विधा की यह ताक़त है कि ‘वह जब चलता था, उसकी नसें चट-चट बोलती थीं, वह गुंडा था’ को नाट्य में दिखा पाना दूभर है। लेकिन जब प्रसादजी का गुंडा नन्हकू सिंह बना टाँक का मृत्युँजय प्रसाद अपनी बलिष्ठ देहयष्टि और मंथर गति की सलोनी अदा में स्थिर नज़रों से इत-उत देखते चलता है, तो दृश्य विधा की इस ताकत के सामने प्रसादजी का गुंडा हमारी धारणा में तिरोहित और नाटक का यह गुंडा विधिवत स्थापित हो जाता है। यह गुंडा आज का ‘भाई’ नही हैं, जो ग़रीबों-कमज़ोरों को सता कर ऐश करे…। यह ग़रीबों की बस्तियाँ उजाड़कर कोठियाँ नहीं बनाता, बल्कि बिना कुछ कहे अपनी कोठियाँ बेचकर ग़रीबों की मदद करता है। वह आज के गुंडों जैसा अय्याश बलात्कारी नहीं है, दुलारी के प्रति उसका प्रेम शुक्लजी के शब्दों में कहें, तो कनखियों में ‘शालीनता से झांकता है, निर्लज्जता से कराहता नहीं’। तभी तो जिससे प्रेम करता है, उसके घर के बाहर बैठ के संगीत सुनता है और आधी रात को चुपचाप उठकर घर चला जाता है। बड़ा तबका उसका निंदक है, पर वह अवाम का हीरो है। और प्रसादजी का समय आज़ादी-प्राप्ति के निर्णायक प्रयत्नों की ओर बढ़ती लड़ाई का था। सो, उनका गुंडा समय आने पर अंग्रेजों से मिल गये देशद्रोही मौलवी कुबरा को सरेआम बेइज्जत करके ललकार देता है और इसके चलते कुबरा इस पर अंग्रेज सेना से धावा बोल देता है…फिर तो वह गुंडा नन्हकू ‘न दैन्यम्, न पलायनम्’ के महनीय मूल्यों पर चलने की मुहिम में अकेले दम लड़ते एवं दुश्मनों का पसीना छुड़ाते हुए प्राणोत्सर्ग कर देता है। कहना होगा कि यदि यह कहानी आज भी हमे खींचकर अपने को पढ़ाती है, विज्येंद्र को इतना समृद्ध नाटक बनाने के लिए आमंत्रित करती है, तो ऐसे हज़ारों हज़ार गुंडों की ज़रूरत आज भी है, क्योंकि अंग्रेज गये नहीं हैं, लोक कवि के शब्दों में प्रतीक रूप से कहूँ तो ‘कांग्रेसिया बिदेसिया समान सजनी’ बनकर फिर से यहीं बस गये हैं…!! इस तरह प्रसाद-काल के माध्यम से नाटक हमारे आज को ललकारता ही नहीं, जीवन के मूल्यों पर चलकर उसे पाने का रास्ता भी दिखाता है…।

बस, बलिदान हो जाने के बाद के विस्तार में गुंडे के बहुरूपिया होने (बचे रहने के लिए वेश बदलने) को संकेतित करने के लिए मंच को चार-पाँच मिनट थामके उसे नर्तकी के रूप में पेश किया जाना… न आम दर्शक के पल्ले पड़ता, न अंत में ठहरे हुए रंग़-प्रयोग में जँचता। यह संकेत ‘गुंडा’ के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन कहीं ऐसे बिठाना होगा कि अंत समय के बेज़ा इंतज़ार से बचा जा सके तथा इस बात को ज्यादा अच्छे से कहा भी जा सके…। कहने की बात नहीं कि बड़े नाट्य-दल के बावजूद सबका अभिनय अपने में सही और आपसी संगति में लहकता हुआ रहा तथा गीत-संगीत प्राणवायु बनकर दर्शकों को जीवंत व मस्त करता रहा…। ऐसी पूर्ण प्रस्तुतियाँ आजकल दुर्लभ हैं, जिसे ‘प्रवीण नाट्योत्सव’ द्वारा कर पाने का यह श्रेय अभिनंदनीय है।
उत्सव की दूसरी शाम का नाटक ‘कुच्ची का क़ानून’ देखकर तो पटना आना अपनी रज-ग़ज़ से सार्थक हो गया…। यह शिवमूर्त्तिजी की इसी नाम की कहानी है, जो पुनः विज्येंद्र के करने में ‘कहानी का रंगमंच’ के ‘अंकुर’ को तो कहीं ऊसर में गाड़ ही देती है, बड़े से बड़े सरनाम नाटक के कान काटने जैसी बात बन गयी है। ग्रामीण जीवन में नारी- उत्पीड़न के तेज रचनाकार हैं शिवमूर्त्ति। उनकी कहानी ‘तिरिया चरित्तर’ और उस पर इसी नाम से बनी बासु चटर्जी की फ़िल्म आपको याद होगी। ससुर द्वारा सुनियोजित रूप से बहू के बलात्कारी यौन शोषण पर पंचायत वहाँ भी जुटी थी और स्त्री के जननांग़ को जलती सलाख़ों से दागने का फ़ैसला हुआ था। पंचायत यहाँ भी जुटती है, लेकिन गोया ‘तिरिया चरित्तर’ के नाजायज़ फ़ैसले को निरस्त करने और नारी-पक्ष को स्थापित करने के लिए। वैसे यह कहानी आज भी अपने देश के गाँवों के लिए समय से काफ़ी आगे की बात है। वहाँ आज भी इसे दिखाने जायें, तो शायद लोग मार के भगा दें…। वहाँ कौन बर्दाश्त करेगा कि कोई विधवा बहू (कुच्ची) बिना दूसरी शादी के गर्भ धारण करे…पिता का नाम भी न बताये और बच्चा पैदा करके शान से रहना चाहे…? यह अलग बात है कि अब गाँवों में पंचायतें होती नहीं – काग़ज़ पर प्रावधान भले हो। और कोर्ट में यह केस पाँच मिनट में हल हो जायेगा…कुच्ची के कृत्य को बहाल कर दिया जायेगा…। बहाल यह पंचायत भी करती है, क्योंकि कुच्ची तर्क देती है कि यदि अपने हाथ-पाँव…आदि सारे अंगों पर स्त्री का अधिकार है, तो उसकी कोख पर उसका अधिकार क्यों नहीं है? भले अभी बात ठेंठ (इंटीरियर) जनमानस में पचे न, लेकिन इसीलिए ऐसे नाटकों को सुदूर गाँवों में दिखाने की व्यवस्था सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं को करानी चाहिए, ताकि स्त्री-अधिकार व अस्मिता के ये बोल्ड व सही सलूक सद्विचार के रूप में आम लोगों तक पहुँचें…। बात यह भी है कि ऐसा सब कुछ मान्य होकर जब समाज के बीच खुलकर चलन में आने लग जाएगा, तब समाज का रूप क्या होगा? तो, तब जो होगा, देखा जाये गा – पहले यह तो हो…।
टाँकजी ने ‘गुंडा’ में मंच पर काफ़ी कुछ स्थायी रूप में बिठाया था, जो ज़रूरी भी था और कारगर भी, लेकिन यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। काफ़ी बार तो ख़ाली स्थान पर बात होती है। फिर ज़रूरत के मुताबिक़ कभी खाट, कभी लम्बा पटरा॰॰आदि जैसा कुछ-कुछ आता है, फिर हटत्ता है। इस आवाजाही में बिखराव तो होता है – कथागति व घटना-प्रवाह किंचित बाधित भी होता है। फिर भी कह सकते हैं कि सीमित व निश्चित मंचोपकरणों में मंच मुक्त भी है, पर पात्रों को पौंड़ने की खुली छूट भी नहीं है। ‘उन्मुक्त कसाव’ कह सकते हैं इसे। हाँ, कुच्ची और उसके देवर या जेठ के परिवार के निवास के संकेत आमने-सामने निश्चित हैं, पर हैं सांकेतिक ही। जिस तबके की कथा है, उसमें परिधान वग़ैरह के हाइ-फ़ाइ होने की स्थिति ही नहीं है। सो, अति सामान्य पहनावे ही अनुकूल हैं। पर कुच्ची की साड़ियाँ अवसरानुकूल बदलती अवश्य हैं…। कुच्ची की इस मुख्य व लम्बी भूमिका का नेपथ्य मुझे पता है…। मुम्बई से आने पर अचानक इस ज़िम्मेदारी को पाकर दस दिनों में तैयार करके इतना सही निर्वाह कर देने के लिए शाइस्ता रशीद की लगन-जुनून-मेहनत व मेधा को दाद देनी पड़ेगी – वैसे इसका यह दाय बचपन से ही पटना के थिएटर-कर्म की ही देन है। लेकिन इसमें मंजने, रवानगी लाने के लिए और शोज़ की दरकार है, जिसका व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव न हो पाना रंगकर्म का दुर्भाग्य है। मृत छोटे भाई की जायदाद…आदि हड़पने के साथ उसकी पत्नी कुच्ची पर भी बुरी नज़र रखने वाले बनवारी की टोटल खल भूमिका में मृत्यंजय प्रसाद के ऐक्शन-आवाज़ के जलवे ऐसे निखरे हैं कि पूरे सभागार के गोया दुश्मन बन गये हों …। नाम का उल्लेख न हो, तो आप नहीं समझ सकते कि यही गुंडा के नन्हकू हैं। बलिहारी वेश-श्रिंगार की भी और अभिनय की भी।
दृश्य तो सभी कमोबेस ठीक व अच्छे बने हैं, पर उत्कर्ष (क्लाइमेक्स) के रूप में पंचायत वाला निर्णायक दृश्य वैचारिक बहसों पर आधारित है। लिहाज़ा बहस के विषय व तर्कों की रोचकता तथा कलाकरों की वाजिब सन्न्द्धता के चलते यह अपनी बनावट में बेजोड़ बन पड़ा है। लेकिन बुनावट से उसे लहकाने में पुनः और प्रयोगों (शोज़) की दरकार है। टाँकजी को कोशिश करके इसके अधिकाधिक प्रदर्शन कराने चाहिए, तो यह इनकी ‘पहचान’ (सिग्नेचर वर्क) हो सकता है। वैसे चारो नाटकों के निर्देशन का उनका कौशल अपनी उसी ख़ासियत से बावस्ता है कि कहीं से निर्देशन के गुर जहिराते नहीं, पर हर गति व मोड़ में, हर पहल व उपराम में…कुल मिलाकर समूचे विधान में सारा सरंजाम इतना हस्तामलक है, ऐसे कौशल से संचालित है कि नाटक बन जाता है – बनने का पता नहीं देता…!! और टाँकजी रहते भी इतने निरपेक्ष हैं कि जैसे कुछ कर न रहे हों – और करते हैं भी नहीं, पर सब होता है…। यह एक जादू ही है। शायद इसमें समूह के कलाकरों का भी बहुत कारगर योग है, जो एक समूह से बंधे न होकर शहर के कई समूहों से जुड़े हैं। तो सबकी समझते हैं, जिससे पूरे शहर का रंगकर्म अपने अंजाम तक पहुँच रहा है।
उत्सब का तीसरा नाटक ‘नागर दोला’ अंतरजातीय प्रेम की त्रासदी पर है। लोकनायकों पर आधारित कथा लिखी है रवींद्र भारती ने और अभिकल्पना है – अभिषेक राज की। बड़ी जाति की लड़की रेशमा और पिछड़ी जाति का लड़का खुच्चड़। दंगल मारने वाले खुच्चड पर रीझने वाली रेशमा कुश्ती ही इसलिए खुच्चड़ से छुड़वा देती है कि इसमें एक दूसरे को पटकने की क्रूरता व जोखम है। किंतु यह मेल जमाने को भाता नहीं। रेशम को जान से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन यह प्रेम व दोनो प्रेमी अमर हो जाते हैं। प्रवीण सम्मान से नवाज़े गये मुहम्मद ज़फ़र आलम व पटना की सुपरिचित अभिनेत्री अपराजिता मिश्र मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह इसका शायद दूसरा ही प्रदर्शन था, लेकिन अच्छे अभिनय व सही नाट्य सरंजामों तथा तदनुकूल संगीत से सजी यह दुखांत प्रस्तुति भी दर्शकों को रंजित कर जाती है। इस तरह बारम्बार दर्शनीय बन गये ‘नागर दोला’ का मंचीय भविष्य उज्ज्वल है…।

उत्सव का अंतिम नाटक उत्तर भारत -खासकर पूर्वी उत्तरप्रदेश व बिहार- की नाट्य-परम्परा के नटसम्राट भिखारी ठाकुर लिखित ‘गबर घिचोर’ का मंचन रहा…। नाटक वहाँ के लोकजीवन की उस समस्या पर आधारित है, जिसमें गाँव से कमाने गया युवक शहर में शादी कर लेता है और गाँव में बैठी उसकी परिणीता पत्नी को तरह-तरह की मुसीबतें-ज़िल्लतें झेलनी पड़ती हैं। उधर गावों के नये विकास में बढ़ती नशाखोरी…आदि के चलते नैतिक मूल्यों के पतन की स्थिति में उसको अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ती है और किसी से जुड़ाव के तहत वह एक बेटे की मां भी बन जाती है। इससे मां-बेटे दोनो के प्रति गाँव की हिकारतें बढ़ जाती हैं। बेटे का गबरघिचोर नाम उसी का नतीजा है। किंतु सब कुछ झेलते हुए दोनो का जीवन प्रायः ठीकठाक ही चलता है कि शहर में कायदन पति-पिता और जड़ व्यवस्था में उस मर्द… को बेटे का पता लग जाता है। फिर उसकी स्वार्थी निर्लज्जता उस तथाकथित बेटे को लेने आ जाती है, ताकि उससे भी कमवा के अधिक सुखी हो सके…। उसके लिए इसमें वह स्त्री तो कहीं है ही नहीं। नाटक का बेटे वाला यह पूरा व महत्वपूर्ण कथांश जीवन-यथार्थ के विपरीत भिखारीजी की उद्भावना है, जिससे वे उस १५ साल के बच्चे से उस मर्द-पति को जवाब दिला पाते हैं – वह उस लापता-अनजान मर्द-पिता के साथ जाने से इनकार कर देता है। उसकी करनी के समक्ष आज यह बहुत मामूली कदम भले लगता हो, पर तब यह बहुत था। इसे भिखारी ठाकुर की उसी चेतना व उनके नाट्य के सभी कौशलों के साथ खेलना इस अंचल की अच्छी नाट्य-परम्परा रही है, जो अब कई कारणों से उतना आसान नहीं रह गया है, फिर भी टाँक जी ने उसे सम्भव कर दिखाया है। यह भिखारीत्व की अपनी विरासत के प्रति उसके युवा वारिस (विज्येंद्र) की जानिब से सम्मान-समर्पण का द्योतक तो है ही, उस नाट्य-परम्परा को संजोने-सहेजने व आगे बढ़ाने का कृतज्ञता भाव भी है। ऐसी भाव-चेतना के साथ हुआ यह रंगकर्म और इसी से उत्सव का समापन अपनी सोद्देश्यता के साथ यादगार व सम्मान्य बन गया है, जिसके लिए टाँकजी सलाम के हक़दार हैं…।
इस नाटक के बाद उसी शाम एक कार्यक्रम रखा गया, जिसे समापन कहा जा सकता है। कहीं से गूंज आयी थी कि दो मेहमान बुलाये गये थे, पर इन्हें सुना न जा सका…। सो, समापन में यह भी हो जाये…। और हुआ। मंच पर स्थानीय नाटककर-कथाकर हृषीकेश सुलभ व संजय उपाध्याय भी थे, जिन्होंने एक-एक वाक्य बोलके समय को संतुलित किया और हमें समय दिया। कार्यक्रम औपचारिक था, तो वैसा ही बोलना था, जिसका अच्छा पालन अभिरामजी ने किया। उत्सव के सारे पहलुओं को संक्षेप, पर समग्रता में सटीक ढंग से समेट देने वाले अभिरामजी मेरे लिए मंजे हुए समाहारी वक्ता तो सिद्ध हुए ही, अंग्रेज़ी में पढ़े मराठीभाषी व्यक्ति का मंच से इतनी सुंदर हिंदी में बोलना तो ५४ साल से महाराष्ट्र (मुम्बई) में रहने के बावजूद मराठी न बोल पाने वाले मेरे लिए आश्चर्य, ख़ुशी व अनुकरण का सबब सिद्ध हुआ…। मैंने आयोजन की खूबियों के उल्लेखों और अपने को बुलाये जाने के प्रति आचारवत आभार…आदि के साथ अवश्य मास्टराना सुझाव भी दे दिया कि आज के युग में ‘विमर्शहीनता सबसे बड़ा ख़तरा है’। थियेटर-जगत में इतने अच्छे काम हो रहे हैं, जिसका अच्छा उदाहरण यह उत्सव भी है, पर आज कहीं भी इन पर बातचीत नहीं होती, ताकि सुधार-बदलाव-विकास के मंजर बनें…, जो चिंतनीय है। याद भी दिलाया कि दशक भर पहले तक ऐसे उत्सवों में हर नाटक के बाद तुरत हॉल में ही या फिर पर दूसरे दिन निर्देशक व टीम के बीच संवाद होते थे। कई बातें साफ़ होती थीं…। उदाहरण के तौर पर बता भी दिया कि ‘नाट्याध्यापक की बहाली’ वाली नुक्कड़-प्रस्तुति की बावत कहूँ, तो बहाली तब होगी, जब नियुक्ति हुई हो। लड़ाई तो विद्यालयों में संगीत-शिक्षक आदि की तरह नाट्याध्यापन के लिए शिक्षक-पद की शुरुआत की है। बहरहाल,

बाहर निकलते ही विमर्श-हीनता के कुफ़ल का प्रमाण सुन पड़ा, जब भाई सुलभजी ने बताया कि वह नुक्कड़ वाला मुझसे बोलबाज़ी करने उठ रहा था, उन्होंने रोका। मैंने कहा – ‘भाई, क्यों रोका? आने दिया होता – गरमा-गरमी ही सही, ‘नियुक्ति’ व ‘बहाली’ का फ़र्क़ तो समझ में आ जाता…सौदा घाटे का न था’!! गरज ये कि विमर्श की संस्कृति ख़त्म न हुई होती, तो वह सुनता-समझता-सीखता, वरना बोलबाज़ी करना चाह रहा है…!!
और सचमुच मन में यह टीस कुरेदती रहेगी…, लेकिन सबसे ऊपर, पर सबसे गहरे… मन में बसी रहेगी – ‘कुच्ची के क़ानून’ की याद और इंतज़ार रहेगा उस दिन का, जब नाटक की कुच्ची की तरह हमारे समाज की हर कुच्ची ख़म ठोंक कर कह सकेगी – ‘मेरा बालकिशन पैदा होकर रहेगा’…आमीन!!
————————————————




