 अनिल भास्कर।
अनिल भास्कर।
सरकार विरोध की यह परंपरा भी बड़े कमाल की है, जिसमें सरकार तो तटस्थ रहती है, विरोध प्रदर्शक उत्पीड़क और आम जनता उत्पीड़ित हो जाती है। यह हम सबको समझने की जरूरत है कि रेल-सड़क जाम, व्यापार और दूसरे काम-धंधों पर जबरन रोक वास्तव में सरकार विरोध का जरिया है या आम जनता की सांसत का?
तोड़फोड़ से नुकसान किसका

सरकारी सम्पत्तियों में तोड़फोड़ या आगजनी से वाकई सरकार का नुकसान होता है या आम जनता का? किसान आंदोलन के ताप में भी सरकार की बजाय आम जनता ही अकुला रही है। सरकार और आंदोलन के सरगनाओं की हठधर्मिता की चक्की में आम आदमी पिसा जा रहा है। सोमवार के भारत बंद में बंद कुछ भी नहीं। पश्चिम यूपी, पंजाब और हरियाणा के कुछेक शहर-कस्बों को छोड़ दें तो कहीं भी व्यावसायिक, सामाजिक या अन्य गतिविधियों पर अब तक कोई असर नहीं दिख रहा। लेकिन सड़कों को जाम कर आम मुसाफिरों के लिए मुसीबत जरूर पैदा की जा रही है। एनसीआर के लोगों को दिल्ली की सीमा में घुसने से पहले घंटों जाम का दर्द सहना पड़ रहा है। वक्त के साथ-साथ उनके वाहनों का वह ईंधन भी इस जाम में स्वाहा हो रहा है, जिसकी लगातार बढ़ती कीमतों को आंदोलन के मुद्दों में शामिल बताया जाने लगा है।
शक्ति प्रदर्शन या सिर्फ हताशा
पिछले एक साल में बंद का हर आह्वान नाकाम होने के बाद एक बार फिर वही दांव शक्तिप्रदर्शन का जरिया है या सिर्फ हताशा का द्योतक, हमें यह भी समझना चाहिए। यह कब का साफ हो चुका है कि देश भर के किसानों के नाम पर चल रहे संघर्ष से कुछ खास जिलों के अलावा बाकी किसानों का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं। सरकार यह भली-भांति जानती है। इसलिए शुरू में वह सक्रिय हुई, आंदोलन खत्म कराने की कोशिशें भी की, लेकिन अब आंदोलन को कोई भाव नहीं दे रही। वह मानकर चल रही है कि इस आंदोलन के कर्ताधर्ता एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी सियासी हसरतों की गंध रिस चुकी है। बंगाल चुनाव में डुगडुगी बजाने और राष्ट्रीय आंदोलन की महापंचायत दिल्ली से भागकर मुज़फ्फरनगर में करने के फैसले ने तो इसे उजागर किया ही, लखनऊ घेरने और स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में झंडा फहराने के ऐलान के बाद पीछे हटने के पीछे की राजनीतिक पैंतरेबाजी भी राज न रह सकी।
बौद्धिक परिचर्चा
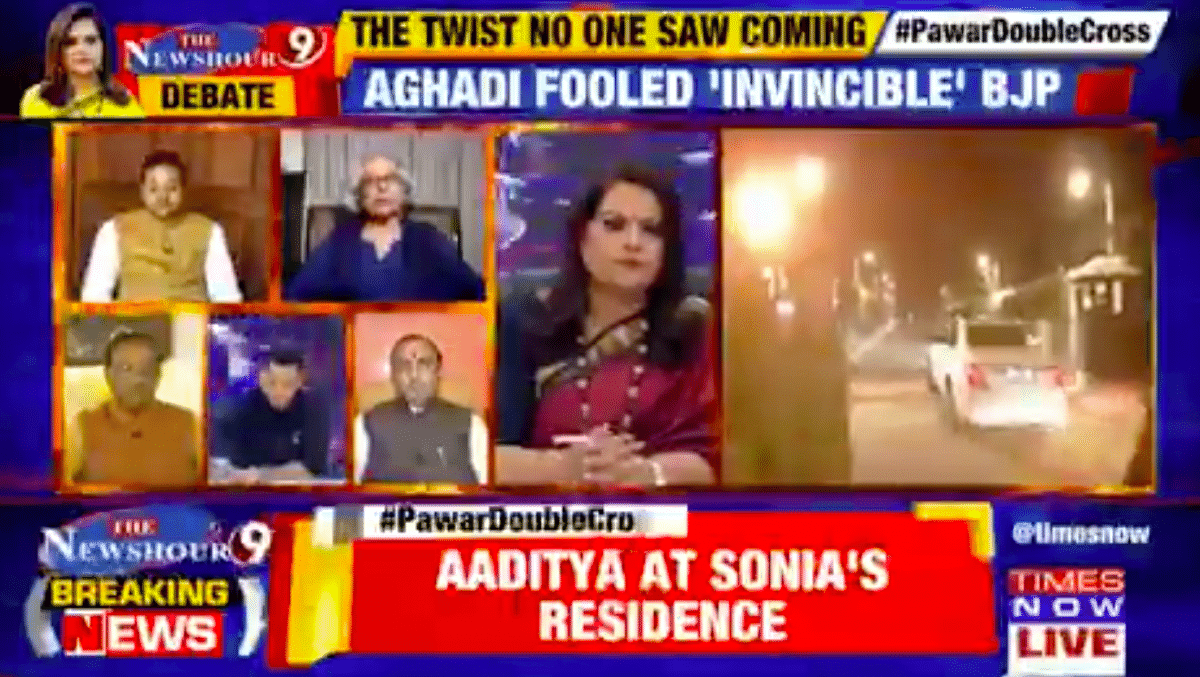
अब तो आलम यह है कि टीवी स्टूडियो से लेकर ड्राइंगरूम तक जब भी इस किसान आंदोलन पर बौद्धिक परिचर्चा होती है, इसके खेती-किसानी पर पड़ने वाले प्रभाव के बजाय आसन्न चुनावों पर संभावित असर का आकलन शुरू हो जाता है। इस आंदोलन के समर्थक और विरोधी किसानों के नफ़ा-नुकसान की बजाय भाजपा समर्थन और विरोध की नीति के आधार पर लामबंद दिखते हैं।
सौदेबाजी का होमवर्क
हमारे एक परम मित्र ने तो मुज़फ्फरनगर महापंचायत के बाद यहां तक लिखा कि यह आंदोलन यूपी में विपक्षी दलों के लिए संजीवनी बन सकता है बशर्ते ये दल इसपर बेरोजगारी, महंगाई जैसे बुनियादी और पारंपरिक मुद्दों का लेप चढ़ाने में सफल हों। लेकिन वे शायद यह आंकने में चूक गए कि महापंचायत मुज़फ्फरनगर में करने की असली वजह अपनी गिरती साख बचाने की थी। दरअसल राकेश टिकैत और उनके सिपहसालार जानते थे कि आंदोलन के मुख्यस्थल (गाजीपुर बॉर्डर) पर महापंचायत रखी तो शायद अपेक्षित भीड़ न जुट पाए और ऐसा हुआ तो आंदोलन की साख और घट जाएगी। दूसरे, मुज़फ्फरनगर में महापंचायत कर राकेश टिकैत अपने लिए राजनीतिक समर्थन का आकलन और इस आधार पर आसन्न चुनाव से पहले सियासी दलों के साथ सौदेबाजी का होमवर्क कर पाएंगे। लिहाज़ा इनसे यह अपेक्षा कि उनका आंदोलन चुनाव में विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ अस्त्र देगा, बेमानी ही रहेगी।
खूंटी पर टंगा मौलिक अधिकार

उधर, विकास के भारी-भरकम सरकारी दावे और 8346 करोड़ की लागत से तैयार दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सालभर से किसान मल-मूत्र त्याग कर रहे हैं। सरकार बेशक इस आंदोलन को चुका हुआ मानकर शाहीनबाग जैसी परिणति की आस में निस्पंद बैठ जाए, लेकिन जिस तरह दिल्ली को अन्य राज्यों से जोड़ने वाले राजमार्ग पिछले एक साल से बंधक हैं और सुगम यात्रा के आम जनता के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसे साफ़तौर पर सरकार की नाकामी ही मानी जाएगी। माना कि किसान और सरकार के बीच चल रहे शह-मात के खेल में आम जनता का हित सुरक्षित रहे, यह जिम्मेदारी उभयक्षीय है, मगर गुरुतर जिम्मेदारी सरकार की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या यह मान लिया जाए कि शासन-प्रशासन ने उन लाखों लोगों के सुगम यात्रा के मौलिक अधिकार को आंदोलन की खूंटी पर हमेशा के लिए टांग दिया है? जब तक किसान आंदोलनरत रहेंगे, क्या हम संकटग्रस्त रहेंगे? क्या इस मुआमले का हल निकलने में सरकार की नाकामी की सजा आम जनता भुगतती रहेगी?
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)




