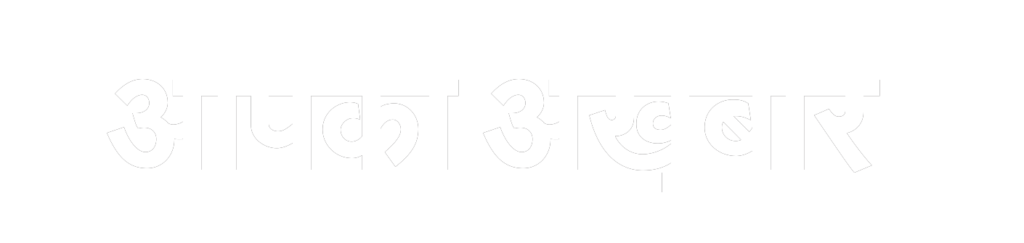प्रमोद जोशी।
प्रमोद जोशी।राम के चरित्र ने जितना हमारे समाज को प्रेरित और प्रभावित किया है, उतना शायद ही किसी दूसरे ने किया होगा। उत्तर भारत में अभिवादन का तरीका ही ‘राम-राम’ है। मैथिलीशरण गुप्त ने अपने ग्रंथ ‘साकेत’ में लिखा है, ‘राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है।’ राम के साथ भारत का रिश्ता बहुत गहरा है। भगवान राम व्यापक रूप से पूजनीय देवता हैं, पर जन संस्कृति के क्षेत्र में, उनकी भूमिका और भी व्यापक है।
जवाहरलाल नेहरू ने ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ में रामायण और महाभारत के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा है, मेरे बचपन की सबसे पहली यादों में इन महाकाव्यों की वे कहानियाँ हैं, जिन्हें मैंने अपनी माँ से और घर की बड़ी-बूढ़ी महिलाओं से उसी तरह सुना था, जिस तरह कि यूरोप या अमेरिका में बच्चे परियों और साहस की दूसरी कहानियों को सुनते हैं। फिर हर साल खुले मैदान में होने वाली रामलीला का अभिनय होता था।
नेहरू ने राम के महत्व को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक-संदर्भों में देखा, पर गांधी ने उसका आध्यात्मिक संदर्भों में इस्तेमाल किया। उनपर राम का बचपन से ही प्रभाव था, जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है। जन्मना वैष्णव विश्वास के होने के कारण, राम और कृष्ण के मंदिरों में जाना उनकी आदत थी, लेकिन मंदिरों ने बालक गांधी में आस्था नहीं जगाई। उन्होंने लिखा, वह मुझे मेरी पुरानी परिचारिका रंभा से मिला। उसने भय के इलाज के रूप में राम-नाम का जप करने का सुझाव दिया। यह उनके लिए जीवन भर के लिए एक अचूक उपाय बन गया। पर गांधी का जीवन व्यावहारिक राजनीति से जुड़ा था। उन्हें पता था कि उन्हें काफी बड़े समाज को अपने साथ लेकर चलना है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू हैं, पर सभी हिंदू नहीं है।
सांस्कृतिक-भूमिका
हर साल रामलीलाओं में वही पात्र वही कहानियाँ, वही संवाद होते हैं, जो दर्शकों को प्रेरित और प्रभावित करते हैं। यह रामकथा की विशेषता है। इस्लाम के भारतीयकरण की लंबी प्रक्रिया में मुसलमान कवियों और लेखकों ने भी राम के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया है। अकबर के ‘नवरत्नों’ में से एक अब्दुर्रहीम खान-ए-खाना ने, जो रहीम (1556-1627) के नाम से प्रसिद्ध है, राम की प्रशंसा में लिखा: ‘गहि सरनागति राम की, भवसागर की नाव/रहिमन जगत उधार को, और न कछु उपाय’ (राम की शरण में जाना ही भवसागर (संसार) से पार ले जाने वाली नाव है, और संसार से उद्धार पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है)। इकबाल ने भगवान राम को ‘इमाम-ए-हिंद’ (भारत का आध्यात्मिक नेता या मार्गदर्शक) कहा, जो उनकी नज़्म ‘है राम के वज़ूद पे हिन्दोस्तां को नाज़’ में व्यक्त हुआ है। लोगों को सही राह दिखाते और अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं, राम।
लोहिया के राम
भारत के आध्यात्मिक महापुरुषों के वर्तमान संदर्भों पर समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने काफी विस्तार से और सार्थक-दृष्टि से लिखा है। उन्होंने 1955 में प्रकाशित ‘राम, कृष्ण और शिव’ शीर्षक से अपने लेख में लिखा, ‘राम, कृष्ण और शिव हिंदुस्तान की उन तीन चीजों में हैं, जिनका असर हिंदुस्तान के दिमाग पर अनेक ऐतिहासिक चरित्रों से भी ज्यादा है। गौतम बुद्ध या अशोक ऐतिहासिक लोग थे, लेकिन उनके काम के किस्से इतने ज्यादा और इतने विस्तार में आपको नहीं मालूम हैं, जितने राम, कृष्ण और शिव के क़िस्से। कोई आदमी वास्तव में हुआ या नहीं, यह इतना बड़ा सवाल नहीं है, जितना यह कि उस आदमी के काम किस हद तक, कितने लोगों को मालूम हैं और कितने लोगों के दिमाग पर उनका असर है।’
लोहिया ने लिखा, लोगों के दिमाग पर उनका असर सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। असर इसलिए है कि वे लोगों के दिमाग में एक मिसाल की तरह आते हैं और ज़िंदगी के हरेक पहलू और हरेक कामकाज के सिलसिले में वे मिसालें, आँखों के सामने खड़ी हो जाती हैं।…सिर्फ मिसाल ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे किस्से भी, जैसे राम ने परशुराम को क्या कहा, कब कहा और कितना कहा, यह एक-एक किस्सा सबको मालूम है। या जब शूर्पणखा आई, तो राम-लक्ष्मण और शूर्पणखा में क्या-क्या बातचीत हुई, या जब राम को वापस ले जाने के लिए भरत आए, तब उनकी आपस में क्या-क्या बातें हुईं, इन सबकी एक-एक तफ़सील, इसने यह कहा, उसने वह कहा, सबको मालूम है।